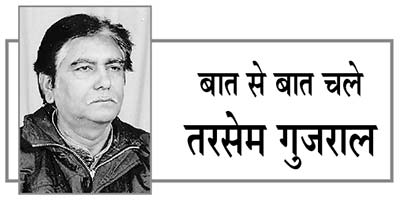लोकतंत्र में जन-हित ही प्राथमिक होता है
हम में से कोई भी वक्त को थाम नहीं सकता। समय का चक्र घूमता रहता है, इसे घूमता रहना चाहिए। 2018 साल या तो डायरियों में रहेगा या स्मृतियों में। 2019 साल का आरम्भ हो चुका है। भारतीय लोकतंत्र की बड़ी घटना 2019 में ही घटने वाली है। यह घटना है देश के आम चुनाव। राजनीति का सिक्का किस करवट गिरेगा, अभी से कह पाना, कुशल राजनीतिज्ञों के लिए भी सम्भव नहीं, परन्तु जो सूरते हाल दिख रहा है, उससे आंखें भी नहीं चुराई जा सकतीं। क्योंकि यह 2014 नहीं है, जो एक इतिहास होने जा रहा है। नरेन्द्र मोदी सामने हैं परन्तु वह पहले की तरह पूर्ण बहुमत से पार्टी को विजय दिलवाने वाले रूप में नज़र नहीं आ रहे। तब भारत की जनता को लगता था कि वह बदलाव लेकर आने वाले हैं। कांग्रेस नीत शासन पर भ्रष्टाचार को लेकर गम्भीर आरोप जो लग रहे थे। बदलाव अवाम की पुकार थी और बदलाव आया परन्तु इन लगभग साढ़े चार साल के शासन में बदलाव की सकारात्मकता सन्देह के घेरे में आयी है। वे क्षेत्र जो बदलाव दिखा रहे हैं, वे भयभीत करने वाले हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू की नीतियां, जो समाजवादी ढांचे से प्रभावित थीं, उनके दिवंगत हो जाने के दशकों बाद भी सरकार के खून में थीं। लिहाजा दूध, सीमेंट, चीनी पर पहला अधिकार सरकारी प्रतिनिधियों का बना रहा परन्तु वे सरकारी अफसर होने के अभिमान से ही ज़मीन से डेढ़ इंच ऊपर थे, ज़मीनी हकीकत से आर्थिक परिवर्तनों से दूर ही रहे। बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत ज़रूरतों पर भी कोई यथार्थपरक सोच वह थी नहीं। समाजोपयोगी प्राथमिकताओं पर कोई विशेष तवज्जो व्यवहारिक एप्रोच में नज़र आई नहीं। नरेन्द्र मोदी ने सरकार को व्यापार चलाने से मुक्त रखने का विकल्प बता कर लोगों को आकर्षित किया। जब भूमंडलीकरण का तीसरा चरण खुल चुका था, मोदी का समय इसकी क्रूरता में अपवाद कैसे रह सकता था? सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक मंच पर विघटनकारी चरित्र दिखने लग गया था। हिन्दी क्षेत्र की दशा और भी ध्यान देने लायक बनी रही, जहां लव जिहाद, गौ-रक्षा के नाम पर विध्वंस ने दिल दहला देने वाली घटनाएं प्रस्तुत कीं। राजनीति का सकारात्मक परिवर्तन यह होता है कि जन प्रतिनिधि तथा लालफीताशाही के सरकारी अफसर तहे दिल से अपना अहंकार त्याग अवाम की खिदमत में हाजिर रहें। गांधी ने जिसे देश के अंतिन जन की तकलीफों को लेकर सावधान किया था, उसी सावधानी के साथ अवाम की मुसीबतें कम करने का लक्ष्य बनायें। परन्तु व्यवहारिक स्तर पर यह जज्बा सामने आ न सका। यहां यह आश्वासन नहीं दिया जा सकता कि यू.पी.ए. के कार्यकाल में लोकतंत्र अपनी आदर्श स्थितियों को पा चुका था, जबकि आज पी. चदिम्बरम लोकतंत्र के संतुलन पक्ष पर जोर दे रहे हैं। कहते हैं कि जब संतुलन खतरे में पड़ जाता है, या प्रभावित होता है तो लोकतंत्र के अस्तित्व पर सवाल खड़ा हो जाता है। भारत के सामने तो यह सवाल है कि क्या भारत में अब लोकतंत्र जीवित रह पायेगा, गहराता जा रहा है। उन्हें लग रहा है कि अगर समाधान नहीं निकला तो एक मुद्दा भी लोकतंत्र की पटरी से उतर सकता है। उन्हें लैंगिक असमानता की स्थिति गम्भीर लगी और कहा कि लगता है कि लैंगिक समानता वाला समाज बनाने को लेकर कोई भी गम्भीर नहीं। यह ठीक है कि इस किस्म की असमानता देश कौम को प्रगतिशील नहीं बनातीं। परन्तु नवम्बर’84 के घटनाक्रम को हम भला कैसे भूल सकते हैं, जब देश में प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी की हत्या के उपरांत सिख भाईयों पर अमानवीय अत्याचार हुए थे। परन्तु भाजपा के शासन के वर्तमान दौर में जो गौरक्षा के नाम पर एक प्रकार का आतंक उभरा है, वह भी भारतीय जन-मानस को स्वीकार्य नहीं है। इससे डर और हिंसा के माहौल में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भाजपा के चुनाव में पराजित होने पर राहुल गांधी अभी से 2019 का आम चुनाव बीत जाने की कल्पना करते नज़र आते हैं। परिवारवाद का विस्तार जितना अधिक फैल चुका है, उसने देश के नेताओं से जन-चेतना, जनता की खिदमत जैसे मुहावरों को प्रश्नांकित कर दिया है, फिर महागठबंधन जनहित की पैरवी की जगह नरेन्द्र मोदी को पराजित करने का दावेदार ज्यादा है। आने वाले दिन अच्छे होंगे या नहीं इसकी निर्भरता अब जन-चेतना पर ही है। उनका विवेक वही मदद कर सकता है।