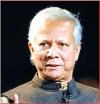विपक्ष की एकता से क्यों झिझक रही है कांग्रेस ?
किसी ज़माने में विपक्ष की एकता का मतलब होता था ़गैर-कांग्रेसवाद की थीसिस के इर्दगिर्द चर्चा होना। 1967 में 10 राज्यों में बनी संविद सरकारों से इस प्रयोग की शुरुआत हुई थी, और 1977 में जनता पार्टी के केंद्र में सत्तारूढ़ होने के साथ यह प्रयोग शिखर पर पहुँचा। नब्बे के दशक में जब भाजपा की साम्प्रदायिक राजनीति ने जोर पकड़ा तो यह बहस ़गैर-भाजपावाद की संभावनाओं के तहत होने लगी। उत्तर प्रदेश में बनी सपा-बसपा सरकार इस तरह की राजनीति की प्रमुख अभिव्यक्ति थी। उसके बाद 2004 और 2009 ने गठजोड़ बनाकर दो बार पहले अटल बिहारी के नेतृत्व वाली भाजपा और फिर लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व वाली भाजपा को हराया। यह एक नयी घटना थी। इससे पहले कांग्रेस गठजोड़ राजनीति से दूर ही रहती थी। गठजोड़ तो उसके खिलाफ बनते थे। आज परिस्थिति पूरी तरह से बदल गई है। भाजपा के दबदबे के खिलाफ राष्ट्रीय गठजोड़ बनाने की गेंद कांग्रेस के पाले में ही है। दिक्कत यह है कि कांग्रेस उसे खेलने से हिचक रही है।
यह नहीं कहा जा सकता कि विपक्ष की एकता एक ऐसा विषय है जो 60 के दशक से ही हमारी राजनीति को चिंतित करता रहा है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस के बोलबाले के तहत भारत की पार्टी-प्रणाली ‘एक दल-महाप्रबल’ की तज़र् पर चल रही थी। हमेशा लगता था कि अगर विपक्ष में एकता न हुई तो लोकतंत्र पूरी तरह से कांग्रेसमय होकर कमज़ोर हो जाएगा। बीच में जब गठजोड़ सरकारों का दौर आया तो यह चिंता काफी-कुछ कम सुनायी देने लगी। 1989 से 2014 तक करीब 35 वर्ष ऐसे गुज़रे कि हर पार्टी किसी न किसी गठजोड़ में रह कर सत्ता की नज़दीकियों का सुख उठा रही थी। लेकिन, जैसे ही भाजपा ने 2014 के चुनाव के बाद कांग्रेस के ही पैटर्न पर ‘एक दल-महाप्रबल’ के रूप में उभरना शुरू किया, वैसे ही विपक्षी एकता की चिंताएं एक बार फिर ज़ोर पकड़ने लगीं।
2024 के चुनाव से पहले ‘इंडिया गठबंधन’ बनाने की कोशिशों ने संकेत दिया कि अब भाजपा को भी कड़ी लोकतांत्रिक प्रतियोगिता से गुज़रना पड़ सकता है। खास बात यह है कि विपक्ष का यह राष्ट्रीय गठजोड़ कभी संगठनात्मक दृष्टि से औपचारिक रूप नहीं ग्रहण कर पाया, लेकिन इसकी चर्चा और इसका विचार ही अपने-आप में इतना पर्याप्त निकला कि भाजपा लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार नहीं बना पायी। ज़ाहिर है कि भाजपा को दस साल की एंटीइनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा था, पर विपक्ष को उसका लाभ पहुंचाने के लिए ‘इंडिया गठबंधन’ की दावेदारियों (भले ही वे कितनी भी बिखरी हुई क्यों न रही हों) की ज़रूरत तो थी ही। आज भाजपा के पास अगर 240 सीटें हैं, तो ‘इंडिया गठबंधन’ के पास सबको मिला कर उससे केवल छह कम यानी 234 सीटें हैं। लेकिन भाजपा एकजुट है और उत्तरोत्तर चुनावी सफलताएं प्राप्त कर रही है। ‘इंडिया गठबंधन’ पहले से भी ज्यादा बिखरा हुआ है। एक तरह से वह एक ऐसा बेचारगी से भरा जमावड़ा बन गया है जिसका न तो कोई केंद्र है और न ही जिसके पास कोई राजनीतिक दिशा है। इस समय वह ज्यादा से ज्यादा संसद में ़गैर-एनडीए शक्तियों के समन्वय का नाम बन कर रह गया है। अदानी के मसले पर देखा गया कि यह समन्वय भी बीच-बीच में टूटता रहता है। विपक्ष की राजनीति इस समय एक दोहरे सवाल का सामना कर रही है: क्या ‘इंडिया गठबंधन’ का भविष्य अंधकारमय है, और लोकसभा चुनाव से पहले उसे औपचारिक रूप न मिल पाने का ज़िम्मेदार कौन है?
मोटे तौर पर देखा जाए तो ‘इंडिया गंठबंधन’ अपने-अपने प्रदेशों में बेहद शक्तिशाली क्षेत्रीय शक्तियों का एक ऐसा गठजोड़ है जो एक राष्ट्रीय पार्टी (कांग्रेस) के ज़रिये दिल्ली की सत्ता में हिस्सेदारी का दावा कर सकती हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो कांग्रेस इन क्षेत्रीय शक्तियों की मदद से दिल्ली में भाजपा को अपदस्थ करने का मंसूबा रखती है। जब दोनों के स्वार्थ मिलते हैं तो फिर यह गठबंधन औपचारिक संरचना क्यों ग्रहण नहीं कर पाया? मेरे पास इसका सीधा जवाब है। कांग्रेस अगर चाहती तो पिछले साल की शुरुआत में ही इस गठबंधन का ढांचा खड़ा हो जाता। दरअसल, जिस दिन कांग्रेस चाहेगी, उसके हफ्ते-दस दिन के भीतर-भीतर इंडिया का एक दफ्तर होगा, एक संयोजक बन जाएगा, एक सचिवालय गठित हो चुकेगा, उसके प्रवक्ताओं की टोली नियुक्त हो जाएगी और उसका न्यूनतम साझा कार्यक्रम कागज़ पर तैयार हो जाएगा।
तो, कांग्रेस ने पहले क्यों नहीं होने दिया, और वह अब क्यों इस तरह की पहल़कदमी से परहेज़ कर रही है? यहां एक बड़े अंतर्विरोध की शिनाख्त ज़रूरी है। जिस समय नितीश कुमार सारे देश में घूम-घूम कर विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर आने के लिए गोलबंद कर रहे थे, उस समय उनकी पीठ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का खामोश हाथ था। स्पष्ट रूप से उस समय कांग्रेस का आलाकमान इस तरह का मोर्चा बनाना चाहता था, और नितीश उसके अघोषित राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। नितीश ने बिहार में तेज़स्वी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और उन्हें केंद्रीय राजनीति में अपनी भूमिका की तलाश थी। इसलिए वे कांग्रेस के साथ मिल कर यह ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे ही कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में करारी शिकस्त हुई, कांग्रेस के आलाकमान का मन बदलना शुरू हो गया। उसे लगने लगा होगा कि अब वह क्षेत्रीय शक्तियों के इस गठजोड़ को अपने हिसाब से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। उसके ़कदम पीछे खींचने का पहला बड़ा संकेत तब मिला जब स्वयं राहुल गांधी ने नितीश कुमार को संयोजक बनाने के प्रस्ताव में इस बहाने से टांग अड़ाई कि इसके लिए ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की सहमति अभी नहीं मिली है। इस घटना ने एक तरह से नितीश का दिल तोड़ दिया, और वे एक बार फिर पलटी मारने की तरफ चले गये। कांग्रेस के इस असहयोग की स्थिति में उनके लिए राष्ट्रीय राजनीति में कदम जमाना नामुमकिन सा था।
चूंकि विधानसभा चुनाव बार-बार हारने के कारण कांग्रेस की क्षेत्रीय शक्तियों का नेतृत्व करने की क्षमता अब पहले से भी कमज़ोर हो गई है, इसलिए वह विपक्ष का कोई भी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने के लिए फिलहाल तैयार होने की स्थिति में नहीं है। कहावत है कि न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगीं। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव बताते हैं कि कांग्रेस शुरुआती बढ़त के बावजूद चुनावों में हार रही है। लोकसभा में उसे सफलता का जो हल्का सा स्वाद मिला था, वह अब तक खत्म हो चुका है। एक तरह से वह राहुल गांधी की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से पहले वाली स्थिति में पहुँच गई है। ऐसी स्थिति में विपक्ष की एकता का नेतृत्व कर पाना फिलहाल उसके लिए संभव नहीं रह गया है।
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।