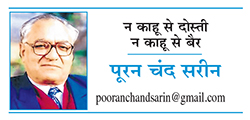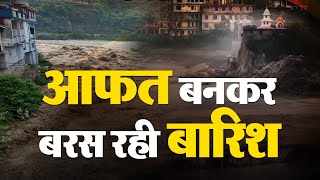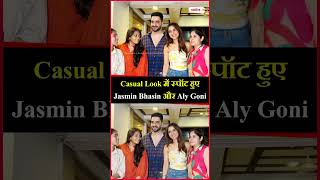प्रकृति की सुरक्षा के लिए कवच की तरह हैं जंगल
अक्सर कहते सुनते और देखते पढ़ते यह बात सामने आती है कि मौसम के तेवर बदल रहे हैं। भयंकर गर्मी, भयानक सर्दी, विनाशकारी बाढ़, बेमौसम बरसात और बर्फबारी तथा ज़मीन खिसकने जैसी घटनाएं अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चिंता और बहस का विषय बन रही हैं। इस सब के मूल में केवल एक बात प्रमुख है, और वह है बड़े पैमाने पर और अंधाधुंध ढंग से वन-विनाश होना। ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तपिश) का कारण यही है।
वर्षा वन दिवस
आज हम विश्व वर्षा वन दिवस मना रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को यह अजीब लगे लेकिन जब इसे मनाये जाने की परम्परा शुरू हुई थी, तब तक संसार के आधे से अधिक वन साम्राज्य पर अपना मतलब साधने के लिए तैयार लोगों का कब्ज़ा हो चुका था। यह सौ से अधिक वर्ष पहले आरंभ हुआ और अब इस सदी में कुछेक साल पहले अचानक ध्यान आया कि मानव जाति उस प्रकृति का कितना नाश कर चुकी है जो हमारा संरक्षण करती है।
अमरीका, यूरोप, एशियाई देश इसकी चपेट में सबसे अधिक आये हैं, जहां सड़कों, भव्य इमारतों के निर्माण, विशाल क्षेत्र का खेतीबाड़ी और बड़े-बड़े उद्योग लगाने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाया गया। यह था कि जहां भी रुकावट हो, उसे जड़ से समाप्त कर दो। अवरोध करने वाले और कोई नहीं, हमारे जंगल थे, वनीय उपज थी और उनमें रहने वाले वनवासी या आदिवासी थे। विरोध के स्वर उठे, बहुत हाहाकार हुआ, आंदोलन हुए, अत्याचार सहे लेकिन सब व्यर्थ क्योंकि अपने पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारने वाले को कौन रोक सकता है? आज सभी देशों से जलवायु परिवर्तन के संदेश आ रहे हैं। भारत इससे अछूता नहीं है और हमारी पूरी आबादी इसे महसूस कर रही है।
सामान्य जंगल तो सब ने जीवन में कभी न कभी देखे होंगे। आजकल जंगल सफारी का चलन है और वहां पाये जाने वाले पशु पक्षियों को निकट से देखने का मोह बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों से निकलकर वन प्रदेशों में घूमना फिरना, झरनों का सौंदर्य निहारने और नदियों तथा तालाबों में जलीय जीवों की अठखेलियां देखना कभी न भूल सकने वाला अनुभव है। बहुत-से संरक्षित यानी जिन जीवों का शिकार नहीं किया जा सकता, उन्हें हाथ से छूना रोमांचक हो जाता है। उनकी सिहरन और हाथ से फिसलने का कौतुक बहुत समय तक महसूस होता रहता है। इन जंगलों में आधुनिक सुविधाओं, इंटरनेट और रहने तथा मौज-मस्ती करने के साधनों का विस्तार हो रहा है। ‘ईको टूरिज़्म’ के नाम पर दूरवर्ती बस्तियों में आराम और खानपान के प्रबंध धन कमाने का ज़रिया बन चुके हैं।
इसके विपरीत वर्षा वन वे होते हैं, जो लगातार वर्षा से भीगते रहते हैं। अमेज़न के जंगल प्रमुख हैं। यह भारत जैसे दो से भी अधिक देशों के आकार के हैं। यहां दुर्लभ वृक्ष, उनकी प्रजातियां और असंख्य जीव जंतु पलते और बढ़ते रहते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कहीं और नहीं मिल सकते। हमारे देश में असम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिमी घाट और अंडमान निकोबार में वर्षा वन देखे जा सकते हैं। इन्हें सुरक्षित और सामान्य आवाजाही से मुक्त रखने के लिए कानून हैं और इनमें प्रवेश के कड़े नियम हैं।
उल्लेखनीय है कि मेघालय में पवित्र गुफाओं (सेक्रेड ग्रोव) के रूप में विशाल वनस्थली है। वहां की ख़ासी जाति इसका संरक्षण करती है। अनेक सदियों पहले यहां के लोगों ने अनुमान लगा लिया होगा कि क्या होने वाला है, इसलिए वन संरक्षण के ऐसे उपाय किए कि वन सुरक्षित रहें। एक बहुत बड़े क्षेत्र का चुनाव किया जहां हर समय वर्षा होती रहती थी और इसे पवित्र गुफा का नाम दिया ताकि यहां से कोई एक पत्ता तक न ले जा सके।
वर्षा वन की तीन परतें होती है। सबसे पहले घना प्रदेश जहां घना अंधेरा रहता है। यहां जलवायु में उमस और गर्मी रहती है जिससे विभिन्न वनस्पतियां पनपती हैं। एक बहुत बड़ी कैनोपी (छतरी) बन जाती है। घास, पात और पेड़ों से लिपटी लताएं झुंडों में बढ़ती हैं। पूजा स्थल भी है, जहां स्थानीय देवता की पूजा होती है। लोग ऊपर से झांक रही सूर्य की किरणों के प्रकाश में विधि विधान से पूजा-अर्चना करते हैं। वनस्पति विज्ञान के शोधार्थी अध्ययन करते हैं।
यहां रेंगने वाले जीव हैं, सरसराहट करते बिलों में घुस जाने वाले सांप की प्रजातियां हैं। बहुत-से ऐसे जीव हैं जो भयावह वातावरण बनाने के लिए पर्याप्त हैं। न जाने कब कौन कहां से प्रकट हो जाये, कुछ नहीं कहा जा सकता। यहां जो हाथी जैसे विशाल जानवर हैं, मानिए वे किसान हैं। वे जो कुछ खाते हैं, उसे पचाने के बाद जगह-जगह अपना मल त्यागने से उन स्थानों पर बीज भी बिखेरने का काम करते हैं। नये पेड़ उगते हैं, वर्षा वन मालामाल होते रहते हैं। हिंसक पशुओं की दहाड़ गलत इरादे से आये व्यक्ति की रूह फाख्ता करने के लिए काफी है। वर्षा वनों में अनेक किंवदंतियां भी प्रचलित हैं, जैसे कि किसी ने किसी पेड़ की टहनी ले जाने की कोशिश की तो शेर सामने आ गया और जब तक चोरी छिपे ले जा रही वस्तु छोड़ नहीं दी, यह साथ चलता रहा। इसी तरह की कहानियां यहां विद्यमान देवता के बारे में कही जाती हैं। देवता का अपना न्यायतंत्र है और उसी के अनुसार दण्ड का विधान है।
उपयोगिता और वास्तविकता
वर्षा वन और इनमें बसे जीवों की उपयोगिता के बारे में इतना ही कहना काफी होगा कि विश्व की लगभग आधी औषधियां इन्हीं की बदौलत प्राप्त हुई हैं। यहां की हर्बल सम्पदा अनेक गम्भीर रोगों के उपचार में काम आती है। दुर्भाग्य से इस प्राकृतिक खज़ाने पर डाका पड़ रहा है। तस्करी के धंधे में लगे लोग चोरी कर रहे हैं और अमीर देशों को बेच रहे हैं। वर्षा वन की दूसरी परत एक विशाल छतरी की तरह है और तीसरी में साठ से अस्सी मीटर तक के ऊंचे वृक्ष हैं। पेड़ों का अद्भुत संसार दिखाते ये वर्षा वन अपने-आप में अनमोल ही नहीं, पीढ़ियों की धरोहर है, आगामी पीढ़ी के रक्षक हैं। इको सिस्टम इन्हीं पर सबसे अधिक आधारित है। अर्थव्यवस्था के प्रमुख घटक होने के बावजूद इन वनों के विनाश की प्रक्रिया जारी है। विडम्बना यह है कि हम वनों से लेना तो सब कुछ चाहते हैं लेकिन उसे देना तो बहुत दूर, उसका मूल्य भी नहीं चुकाते। यदि वनों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया जाये और अपनी प्रकृति के अनुसार स्वयं बढ़ने दिया जाये तो यही बहुत बड़ा उपकार होगा।
आज पेड़ काट कर और फिर उनके स्थान पर नये लगाने का नाटक बहुत हो गया। केवल इतना ही कर लें कि जंगलों की बहुत कम कटाई करते हुए सड़कें बनायें। इस तरह भी वन विनाश पर रोक लग सकती है। विकास का कोई विरोध नहीं है। उद्योग-धंधे ज़रूरी हैं, आवागमन और यातायात के साधन आवश्यक हैं। विशाल इमारतों का निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र तथा रिहायशी बस्तियां बनानी हैं। कृषि और पशु पालन तथा चारागाह के लिए ज़मीन चाहिए ही, आर्थिक मज़बूती के उपायए रोज़गार के साधन विकसित करने ही होंगे। इनके बिना देश विकसित नहीं होगा। कहना यह है कि ऐसे कानून बनें और कड़ाई से पालन करते हुए वन विनाश को मनुष्य की हत्या के बराबर माना जाये। तब ही पर्यावरण बच सकता है। प्रतिकूल मौसम से बचाव हो सकता है और प्रकृति के साथ कदम ताल करने का सुख मिल सकता है।
आज अमरीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप ऐसी जीवन शैली अपना रहे हैं जो अफरीका जैसी है, जहां जंगलों को साथी मान कर उन्हें अपनाया जाता है, उनके अनुसार स्वयं को ढाला जाता है। प्रकृति को असंतुलित होने से रोकना है तो भविष्य की ऐसी भयावह कल्पना करनी होगी जिसमें चारों ओर मरुस्थल, बंजर भूमि, अधिक या कम वर्षा से बाढ़ और सूखाग्रस्त धरती और आसमान से बरसती आग तथा पृथ्वी पर जल पलायन के दृश्य होंगे। यदि इसे सच में घटित होने से रोकना है तो आज ही कदम उठाने होंगे वरना कौन जाने, कल क्या होगा?