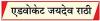बेझिझक रूस से मित्रता निभा रहा भारत
ठीक ऐसे समय जब अमरीका की राजधानी वाशिंगटन में नाटो शिखर सम्मेलन चल रहा था, प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा, न तो कोई रणनीतिक चूक थी और न ही अमरीका और रूस में से सिर्फ रूस को चुनने का रणनीतिक संदेश। वास्तव में यह भारत द्वारा पश्चिम के कूटनीतिक दबाव का बहुत स्पष्टता से दिया गया जवाब था। इसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के सालों में भारत और अमरीका के रिश्ते बहुत मज़बूत हुए हैं। सार्वजनिक मंचों पर जिस तरह से अमरीकी राष्ट्रपति ने भारत को अपना मज़बूत दोस्त कहना और जताना शुरु किया है, वह भी इसका ठोस सबूत है। साथ ही यह बात भी सच है कि आज के आधुनिक और आर्थिक विश्व में अमरीका से बेमतलब की दूरी अपनी आर्थिक और राजनीतिक संभावनाओं पर कुल्हाड़ी मारना है, लेकिन इस सबके बीच भारत यह कैसे भूल जाए कि इतिहास में जब जब हमारे अस्तित्व पर संकट मंडराया है, यह रूस (जो कि एक समय तक सोवियत संघ था) ही है, जो सीना तानकर हमारे साथ खड़ा रहा है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर समस्या को लेकर दर्जनों बार रूस द्वारा किया गया वीटो हो या 1971 की भारत-पाक जंग के दौरान अमरीका और ब्रिटेन द्वारा भारत को अप्रत्यक्ष रूप से घेरने की साज़िश के विरूद्ध अरब सागर में अपने जंगी बेड़े के साथ आ डटना रहा हो।
तब का सोवियत संघ ऐसे हर मौके पर भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े होने में ज़रा भी हिचक नहीं दर्शायी, तो भला भारत ऐसे परीक्षा के वक्त पर रूस को अकेला कैसे छोड़ दे, जब अमरीका के नेतृत्व में समूचा पश्चिमी जगत उसे गैर-ज़रूरी दबाव में लाकर दुनिया में अपना एकछत्र वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा हो। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बाहरी तौर पर देखने में भले लग रहा हो कि रूस और यूक्रेन युद्ध इसलिए नहीं खत्म हो पा रहा, क्योंकि पुतिन बहुत ज़िद्दी और घमंडी राजनेता हैं, वह किसी भी कीमत पर रूस की विजय की स्वीकार्यता के युद्ध बंद नहीं करना चाहते। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू है। हकीकत यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदोमीर ज़ेलेंस्की किसी षड़यंत्र के चलते या बेवकूफी में अमरीकी नेतृत्व वाली पश्चिमी ताकत का मोहरा बने हुए हैं। ध्यान से देखें तो रूस और यूक्रेन के बीच मुकाबले का कोई जोड़ नहीं है और अगर नाटो के डेढ़ दर्जन देश पहले दिन से ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ इस तरह जबरदस्ती पकड़कर खड़े न होते तो कब की यह जंग खत्म हो गई होती।
लेकिन अमरीका के मन में तो चोर है, गोर्वाच्यौव और रोनाल्ड रीगन की आपसी दोस्ती के कारण दुनिया को शीतयुद्ध से मुक्ति दिलाने के लिए जो राह हमवार हुई थी, जिसके चलते बाद में गोर्वाच्यौव और रीगन 11-12 अक्तूबर, 1986 को आईसलैंड के रेक्जाविक में शिखर सम्मलेन के लिए मिले, उस बैठक से लेकर सोवियत संघ के पतन तक जितनी भी बैठकें हुई थीं, उन सब में यह तय हुआ था कि शीतयुद्ध को धार देने वाले अलग-अलग खेमों के दो सैन्य गुटों—वार्सा पैक्ट और नाटो को खत्म कर दिया जायेगा, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद वायदे के मुताबिक रूस ने वार्सा पैक्ट तो खत्म कर दिया, लेकिन अमरीका ने इधर-उधर की बातें करके नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) को न सिर्फ बनाये रखा, बल्कि जैसे-जैसे सोवियत संघ के खात्मे के बाद रूस कमज़ोर होने लगा, वैसे-वैसे अमरीका पुरानी बातों और वायदों को भूल कर नाटो को न सिर्फ बरकरार रखा बल्कि धीरे-धीरे उसकी ताकत और आक्रामकता भी बढ़ाने लगा। यह सीधे-सीधे रूस के पूर्व रूप सोवियत संघ की पीठ में अमरीका द्वारा घोंपा गया विश्वासघात का छुरा था।
लेकिन इस सब पर अमरीका किसी तरह का अपराबोध पालने की बजाय उल्टा इसे अपनी रणनीतिक चातुरी और विजय की तरह प्रस्तुत करने लगा। जब घोषित रूप से अब दुनिया में दो प्रतिद्वंदी कैंप या धड़े नहीं रहे, तो फिर आखिर नाटो की उपयोगिता क्या है? जबकि उसकी स्थापना ही रूस और उसके साथी कम्युनिस्ट देशों की भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती को ध्वस्त करने के लिए और दुनिया में पूंजीवाद का विस्तार करने के लिए हुई थी। ऐसे में सिद्धांतत: यह ज़रूरी था कि जब वार्सा पैक्ट को खत्म कर दिया गया, जिसमें सोवियत संघ का नेतृत्व स्वीकार करने वाले देशों की सेनाएं और सैन्य ताकत एकजुट थीं। रूस भला इस विश्वासघात को कब तक अनदेखी करता, खास तौर पर तब जब सोवियत संघ के पतन के बाद अमरीका लगातार अपने नेतृत्व में नाटो को आधुनिक रूप से सैन्य-सज्जित कर रहा था। साथ ही बिना किसी तरह के संकोच या लिहाज के वह नाटो का विस्तार करते हुए इसे रूस के दरवाज़े तक लेकर जा रहा था। एक तरह से अमरीका की योजना रूस में ही रूस को छोटे-छोटे यूरोपीय देशों के कंधों पर उनकी सुरक्षा के नाम पर बंदूक रखकर घेरने की कोशिश थी जबकि रूस लगातार अमरीका को इसके विरूद्ध चेतावनी दे रहा था।
पिछले दो सालों से ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों की कठपुतली बनकर अपने देश को नेस्तनाबूद करा लिया है। पिछले दो सालाें में रूस ने यूक्रेन के दो-तिहाई हिस्से को तहस-नहस कर दिया है, लेकिन अभी भी ज़ेलेंस्की के दिमाग में यह बात नहीं चढ़ रही कि पश्चिमी देश उसे उकसाकर उसका कबाड़ा करवा रहे हैं। जिस पश्चिमी सहायता के नाम पर ज़ेलेंस्की उछल-कूद रहे हैं, उस संबंध में उन्हें जानना चाहिए कि ब्रिटेन से लेकर अमरीका तक और फ्रांस से लेकर जर्मनी तक किसी भी देश ने यूक्रेन को सहायता के नाम पर अपनी सैनाएं नहीं दीं, सिर्फ हथियार दिए हैं, जिनका इस लड़ाई में और सही से परीक्षण हो जाए। साथ ही इसकी कीमत भी आगे पीछे यूक्रेन को ही किसी भी रूप में चुकानी है। पश्चिमी देशों और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के इस महत्वाकांक्षा के दबाव में भारत अपने हितों के साथ समझौता क्यों करे? इसलिए तीसरी बार सरकार बनाने के बाद अगर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की पहली यात्रा पर जाना तय किया है, तो यह दुनिया को संदेश है कि भारत फैसले के वक्त पर अपनी सोच और समझ का फैसला करता है, किसी के दबाव में नहीं आता।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर