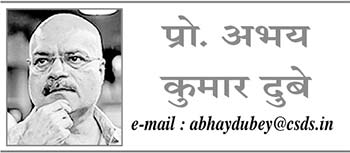क्या भारतीय लोकतंत्र में गिरावट आ रही है ?
कहते हैं कि दुनिया उम्मीद पर कायम है। यही बात लोकतंत्र के बारे में भी कही जा सकती है। बस अंतर यह है कि उम्मीद रखने वाले लोकतंत्र के किसी एक पक्ष से आशान्वित रहते हैं, और इस चक्कर में दूसरे पक्ष की उपेक्षा हो जाती है। मसलन, एग्ज़िट पोल के अड़तालीस घंटे पहले स्टॉक एक्सचेंज में एक प्रतिशत यानी 537 अंकों का उछाल आया। जानकारों ने कहा कि अगर एग्ज़िट पोल में मोदी के नेतृत्व वाला मोर्चा (राजग) तीन सौ के करीब सीटें जीतता नज़र आया तो बाज़ार कम से कम एक से डेढ़ फीसदी ऊंचा खुलेगा, और अगर यह मोर्चा ढाई सौ से कम सीटें जीतता नज़र आया तो शेयर नीचे चले जाएंगे। हम जानते हैं कि सट्टा बाज़ार संभावनाओं और अंदेशों का खेल है। वह राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता चाहता है। मुझे याद है कि 2009 में जैसे-जैसे चुनाव नतीजे कांग्रेस के नेतृत्व वाले मोर्चे (संप्रग) के पक्ष में आते गए, सट्टा बाज़ार नई ऊंचाइयां छूता चला गया था। जो उम्मीद तब उसे सोनिया और मनमोहन की जोड़ी से थी, आज वही उम्मीद उसे मोदी और शाह की जोड़ी से है। कभी यही उम्मीद अडवानी-अटल की जोड़ी से थी। ज़ाहिर है कि पार्टियां और जोड़ियां व़क्त के साथ बदलती रहती हैं, इसलिए यह हमारे लिए चिंता का सबब नहीं होना चाहिए। खास बात यह है कि भारतीय लोकतंत्र से निकलने वाली उम्मीदों के आसरे केवल स्टॉक एक्सचेंज ही नहीं, दुनिया के दूसरे देश भी हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत दुनिया भर में लोकतंत्र का विस्तार करने के लिए क़ाफी संसाधन खर्च करता है। पूर्व राजदूत विष्णु प्रकाश द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2015 के बाद से भारत संयुक्त राष्ट्र के लोकतंत्र कोष में तीन करोड़ बीस लाख डॉलर का योगदान कर चुका है। और तो और, दुनिया में एक कम्युनिटी ऑ़फ डेमोक्रैसीज़ नामक संगठन भी है जिसके संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है। यहीं प्रश्न उठता है कि क्या स्टॉक एक्सचेंज और दुनिया के अन्य देश भारतीय लोकतंत्र से जो उम्मीदें रखते, क्या यह लोकतंत्र वास्तव में उस पर खरा उतर पा रहा है? चुनाव नतीजे आने से पहले यह सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी है कि चुनाव प्रचार खत्म होने की घंटी बजने से पहले बंगाल में जो कुछ हुआ है, वह उन आशाओं पर एक तरह का तुषारापात कर देता है जिनकी ऊपर चर्चा की गई है। ममता बनर्जी संयम और मर्यादा छोड़ कर खुलेआम मोदी-शाह को ‘दो गुंडों’ की संज्ञा देती नज़र आईं। हम सबने देखा है कि ममता की राजनीतिक प्रौद्योगिकी किस किस्म की है। पहले उनकी पार्टी आतंक बरपा करती है, और फिर भी अगर विपक्षी उम्मीदवार जीत जाता है तो उसको धमका कर या फुसला कर अपने पक्ष में दल-बदल करवा लिया जाता है। पंचायत से विधानसभा के स्तर तक वे ऐसा कई बार करके चुनाव-प्रक्रिया को बेमानी बना चुकी हैं। लेकिन इस बार उनका म़ुकाबला भाजपा से है जिसके जीते हुए उम्मीदवार उनके साथ किसी कीमत पर नहीं जाने वाले। उधर अमित शाह के रोड शो को देख कर ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी हिंदू त्यौहार का जुलूस हो। एकदम रामलीला का समां था। वही पोशाक, वही रंगे हुए चेहरे और धार्मिक नारेबाज़ी। सीधे-सीधे साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश दिखाई दे रही थी। यानी लोकतांत्रिक प्रतियोगिता में यह नौबत आ चुकी है कि चुनाव जीतने और सत्ता की निरंतरता के लिए नेताओं और पार्टियों ने हर अलोकतांत्रिक हथकंडे को अपनाने की छूट ले रखी है। एक तऱफ हमारे लोकतंत्र का यह काला पक्ष हमारी आंखों में घूर रहा है। दूसरी तऱफ उसके उज्जवल पक्षों पर भी निगाह डाली जानी चाहिए। इन्हीं ममता बनर्जी, जो भाजपा के हमले से अपनी सत्ता बचाने के लिए दीवानी हुई जा रही हैं, को अपने 33 ़फीसदी टिकट स्त्रियों को देने का श्रेय जाता है। यही काम ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के सर्वेसर्वा नवीन पटनायक ने भी किया है। जिस देश की विधायिकाएं स्त्रियों को माकूल नमुइंदगी देने में नाकाम रही हैं और जहां स्त्री-आरक्षण विधेयक लम्बे अरसे से लटका हुआ है, वहां अगर दो बड़े क्षेत्रीय नेता यह पहलकदमी लेते हैं तो उसे एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। इससे स्त्री-आरक्षण विधेयक के पक्ष में एक मज़बूत तर्क विकसित होगा। इसी तऱीके से इस चुनाव में कौन पिछड़ा है, और कौन नहीं, इस विषय में हुई बहस भी स्वागत-योग्य प्रतीत होती है। यह विवाद प्रधानमंत्री की जाति को मिली पिछड़े वर्ग की हैसियत से शुरू हुआ, और इस बौद्धिक बहस के मुकाम पर पहुँचा कि अगर किसी को पिछड़े वर्ग का होने के बावजूद सामाजिक और अन्य तरह के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है तो उसके पिछड़े वर्ग के होने के दावे को गम्भीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। सोचने की बात है कि अगर यह तर्क और आगे बढ़ता है तो केवल जन्मना पिछड़े और दलित होने की सामाजिक वैधता पर सवालिया निशान लग जाएगा। ऐसे न जाने कितने पिछड़े, दलित और आदिवासी हैं जिन्होंने जीवन के एक दौर में या परिस्थितियों वश शुरू से ही भेदभाव का सामना नहीं किया है। यानी वे केवल तकनीकी रूप से पिछड़े या दलित हैं। ऐसे लोगों को देखने की निगाह अगर बदलेगी, तो सामाजिक न्याय की राजनीति में आ गई विकृतियां दूर होने की परिस्थितियां बनेंगी। मुझे याद पड़ता है कि चुनावी मुहिम शुरू होते समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सड़क यात्रा के दौरान मैंने अपने तीन समाज वैज्ञानिक सहयोगियों (तीनों ही राजनीतिक शास्त्री) से पूछा था कि उनकी निगाह में भारतीय लोकतंत्र इस समय किस स्थिति में है? सोच-विचार के बाद तीनों विद्वानों का जवाब था कि लोकतंत्र का हुलिया तो ठीक-ठाक लग रहा है, पर उसकी क्वालिटी में गिरावट आई है। संभवत: उन तीनों का कहना यह था कि लोकतंत्र की क्वालिटी मूल्यवान समृद्ध होने के बजाय क्षय की तऱफ जाती हुई दिख रही है। इस माऩीखेज़ प्रेक्षण पर भी लोकसभा चुनाव की मुहिम की रोशनी में गौर किया जाना चाहिए। लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि वह सभी तरह की राजनीतिक शक्तियों को प्रतियोगिता का समान धरातल मुहैया करायेगा। लेकिन इस बार ऐसा होता हुआ नहीं दिखा। मसलन, बंगाल में झगड़ा तृणमूल और भाजपा में था लेकिन चुनाव आयोग ने दस घंटे पहले ही प्रचार बंद करवा दिया और इस तरह उन पार्टियों (कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी) को भी सज़ा दे दी जिनकी उस हिंसा या झगड़े में कोई भूमिका नहीं थी। तुर्की के प्रधानमंत्री एरडोगन का एक कथन यहां याद आता है कि लोकतंत्र एक ऐसी ट्रेन है जिससे आप मंज़िल पर पहुंचने के बाद उतर जाते हैं। यानी उनके लिए लोकतंत्र अपने-आप में एक मंज़िल न होकर किसी (?) मंज़िल तक पहुंचने का एक ज़रिया भर है। अगर इस प्रेक्षण में दम है, तो फिर हमें लोकतांत्रिक प्रतियोगिता में भिड़े हुए किरदारों और पार्टियों की लोकतांत्रिक निष्ठाओं के बजाय उन मंज़िलों को समझने की कोशिश करनी होगी जो उन कथित निष्ठाओं की आड़ में कहीं छिपी हुई है।