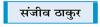दूसरे दौर में दाखिल हो चुका है संघ का प्रोजैक्ट
देश के एक अत्यंत प्रतिष्ठित राजनीतिक सिद्धांतकार सुहास पलशीकर ने हिन्दुत्ववादियों द्वारा लोकतंत्र के साथ निकट भविष्य में किये जा सकने वाले सुलूक के बारे में लिखा है, ‘एक समय आएगा जब लोकतंत्र को पश्चिमी विचार बताने की दलील दे कर कहा जाएगा कि यह सच्चे और आध्यात्मिक मोक्ष के लिए अनावश्यक है। यह दावा किया जाएगा कि लोकतंत्र का एक देशज तात्पर्य भी है। उदारपंथी विचार और व्यक्ति के अधिकार तो पश्चिमी फैशन हैं, संस्थाओं की स्वायत्तता का विचार पत्थर की पूजा के अलावा कुछ नहीं है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बेकार की विलासिता है .....। दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर ज़ोर और एम.एस. गोलवलकर के विचारों की फिर से बेहिचक दावेदारी उस पहले कदम का लक्षण है जिसके तहत लोकतंत्र के भारतीय-हिन्दू संस्करण होने की दलील दी जाने वाली है। संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत के हाल के भाषणों का सावधानीपूर्वक अर्थ ग्रहण करने से इसका प्रमाण मिल जाएगा। यह दावा सीधा-सरल है कि पश्चिमी बौद्धिक परम्परा से स्वतंत्र और उससे बहुत पहले हिन्दू परम्परा और शास्त्रों में लोकतंत्र का आविष्कार, अभ्यास और सिद्धांतीकरण किया जा चुका था। यह कहते हुए उन दो केंद्रीय स्रोतों को नकार दिया जाता है जिन पर भारत की लोकतांत्रिक राजनीति आधारित है। ये हैं राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान।’
पलशीकर ने बहुसंख्यकवादी राजनीति के उभार के कई ओझल पक्षों को पहले भी हमारे सामने रखा है। इस क्षेत्र में उनका योगदान प्रशंसनीय है। दरअसल, पलशीकर ने ही अपने आंकड़ागत विश्लेषण के ज़रिये बताया था कि 2004 से 2014 तक भाजपा सत्ता से बाहर ज़रूर रही, लेकिन वोटों के स्तर पर हिन्दू एकता लगातार मज़बूत होती रही। लेकिन, इस ़खूबी के बावजूद उनका यह अवलोकन दो समस्याओं का शिकार है। पहला, उनके लहज़े से यह प्रतीत होता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य के ऊपर पश्चिम का कॉपीराइट है, और उस मॉडल से किसी तरह का विचलन स्वाभाविक रूप से शक के दायरे में समझा जाना चाहिए। किसी भी विद्वान का ऐसा रवैया हमें अंग्रेज़ों के भारत आने से पहले की राजनीति को समझने और अध्ययन करने से रोक देता है। 18वीं सदी में पश्चिम के उदय से पहले भी दुनिया में राज्य-व्यवस्थाओं के विभिन्न रूप प्रचलित थे। पश्चिमी लोकतंत्र को ही राज्य का एकमात्र श्रेयस्कर रूप मानने का नतीजा अतीत के ज्ञान की उपयोगिता को बिना सोचे-समझे नकारते रहने में निकलता है। हो सकता है कि पलशीकर का यह कथन हिन्दुत्ववादियों द्वारा लोकतंत्र को विकृत कर डालने के डर की उपज हो लेकिन इसमें भारतीय समाज-विज्ञान में घर कर चुकी युरोपपरस्ती भी देखी जा सकती है।
दूसरा, यह कथन हिन्दुत्वादियों द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन और संविधान को अपने विचारधारात्मक प्रोजेक्ट में खींच लेने की उस प्रक्रिया को नज़रअंदाज़ करता है जो बालासाहब देवरस के ज़माने से ही सतत जारी है। देवरस ने 1974 में पूना में दिये गये अपने एक भाषण में इसका सिद्धांतीकरण किया था। ़गलतियां करने और सुधारने की धीरे चलने वाली लेकिन लम्बी प्रक्रिया के ज़रिये संघ और भाजपा ने इसे व्यवहार में उतार दिया है। आज़ादी के पहले और बाद से चल रही विभिन्न बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता में कई अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठा कर और बिना थके प्रयास करते रहने के कारण हिन्दू बहुसंख्यकवाद अन्य बहुसंख्यकवादों (सिख, मुसलमान, ईसाई और अन्य जातियों के बहुसंख्यकवाद) से बहुत आगे निकल गया है।
जितना हम लोग सोच सकते हैं, संघ उससे कहीं ज़्यादा लचीला और परिवर्तनशील है। अपनी विचारधारा के मर्म पर कायम रहने के अलावा किसी पहले कही गयी बात (चाहे वह गोलवलकर की हो या उपाध्याय की) को दुहराते रहने में उसकी दिलचस्पी नहीं है (यह अलग बात है कि यह ‘मर्म’ संघ के आलोचकों को बहुत धीरे-धीरे और टुकड़ों में ही समझ में आ रहा है, क्योंकि उनका ज़्यादातर समय अल्पसंख्यक विरोध और मनुस्मृति वगैरह का समर्थन करने वाली चमकदार किस्म की बातों को संघ का मर्म समझने में ही खर्च हो जाता है)। मोहन भागवत ने इस बारे में संघ के मौजूदा नेतृत्व का रवैया स्पष्ट किया है। वे लोग पहले कही गई बातों को दो भागों में बांट कर देखते हैं। एक भाग में वे बातें रखी जाती हैं जो किसी ़खास ‘प्रसंग-विशेष’ के कारण कही गई होंगी, और दूसरे भाग में वे जिनका महत्व ‘सदा काल’ के लिए है। इस युक्ति के कारण संघ को विभिन्न विमर्शों को अपनाने और छोड़ने की सुविधा मिल जाती है। संघ इस युक्ति को अपने विमर्श के दायरे से बाहर के विचारों के लिए इस्तेमाल करता है। इस मामले में देवरस का 1974 का व्याख्यान भी याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने हिन्दू समाज की कड़ी आलोचना करने वाले समाज सुधारकों की बातें भुला कर उन्हें ‘हिन्दू चिंतक’ के रूप में प्रात: स्मरणीय हस्तियों की तरह स्वीकार करने का कार्यक्रम पेश किया था।
समझने की बात यह है कि अब संघ परिवार अपने प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में है। पहला चरण चुनावी प्रभुत्व स्थापित करने और सार्वजिनक जीवन में राजनीतिक विमर्श को इस कदर हिन्दू-उन्मुख बनाने का था कि अगर कभी चुनावी प्रभुत्व गड़बड़ा जाये तो भी सत्ता में आने वाली ताकतें भाजपा की कार्बन-कॉपी ही लगें। दूसरा चरण आज्ञापालक समाज बनाने का है। वर्ग-संघर्ष, जाति-संघर्ष, समाज सुधारों के लिए संघर्ष, ब्राह्मणवाद-विरोध, सामाजिक न्याय के नाम पर अस्मिताओं का टकराव और इसे आरक्षण की मांग में घटा देना, अल्पसंख्यक अधिकारों की लड़ाई, नाना प्रकार के अन्य अधिकारों की दावेदारी, जेंडर डेमोक्रैसी के लिए संघर्ष, हर तरह के नये घटनाक्रम को क्रांति की संज्ञा देने का रवैया- यह पूरी भाषा उदारतावादी लोकतंत्र के दायरे में टकरावमूलक राजनीति की है जिसके हम सब अभ्यस्त हो चुके हैं। संघ भी ज़रूरत पड़ने पर टकरावमूलक राजनीति और गोलबंदी करता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रामजन्मभूमि आंदोलन है, परन्तु यह उसकी कार्यनीति होती है, दीर्घकालीन रणनीति और विचारधारा नहीं। दरअसल, संघ परिवार इस टकरावमूलक भाषा को मिल चुकी विमर्शी और व्यावहारिक वैधता को ़खत्म करना चाहता है। इसके लिए वह परम्परा का आह्वान कर रहा है, और भारतीय परम्परा इतनी विविध है कि उसमें से इस विचार के पक्ष में दृष्टांत खोज लेना आसान है। वैसे, यह उसका कोई नया विचार नहीं है। संघ के दस्तावेज़ों में उसके सिद्धांतवेत्ताओं द्वारा संघर्षविहीन सुधार, सामंजस्य और समरसता के पहलुओं को रेखांकित करने के विचारधारात्मक आग्रह स्पष्ट रूप से मौजूद हैं।
जहां तक किसान आंदोलन का ताल्ल़ुक है, उसकी निरन्तरता इसलिए महत्वपूर्ण है कि उसने इस वैचारिक प्रोजेक्ट की बेरोकटोक यात्रा को एकबारगी रोक दिया है। इसके ज़रिये बनने वाला प्रतिरोध का व्याकरण अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है लेकिन इसके कारण नये विमर्शों की गुंजाइश खुली है। नयी सामाजिक-राजनीतिक एकताएं उभरी हैं। साम्प्रदायिकता के दबाव में टूट चुकी पुरानी एकताओं की वापसी, और नयी बहसों की शुरुआत हुई है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह किसान आंदोलन व्यवस्था और उसकी संचालक सरकार द्वारा दी गई प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आज्ञाओं को तिरस्कार के साथ देखते हुए अवज्ञा की उस संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहा है जिसकी रचना गांधी के नेतृत्व में उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में हुई थी। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के इन आयामों ने मिल कर एक आज्ञा बनाम अवज्ञा के अंतर्विरोध को जन्म दे दिया है। व्यवस्था पर काबिज़ त़ाकतों ने अगर विभिन्न सामाजिक शक्तियों की सहमति प्राप्त करके इसे इसे जल्दी ही हल नहीं किया, तो लोकतांत्रिक प्रणाली तकरीबन वैसे ही संकट में फँस सकती है जैसा सत्तर के दशक के पूर्वार्ध और मध्य (सम्पूर्ण क्रांति आंदोलन से ले कर आपातकाल तक) में पैदा हुआ था।