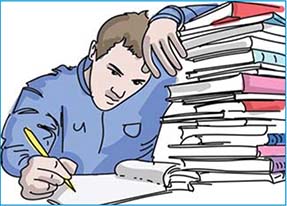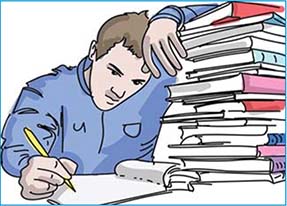सीखने के आनंद को समाप्त करता परीक्षा का दबाव
अभी कड़ाके की सर्दी जारी है और सीबीएसई बोर्ड की इस घोषण ने देशभर के किशोरों में गर्मी और घबराहट ला दी है कि 15 फरवरी से सीबीएसई के 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू होगी। खुद को बेहतर साबित करने के लिए इन परीक्षाओं में अव्वल नम्बर लाने का भ्रम इस तरह बच्चों व उससे ज्यादा उनके पालकों पर लाद दिया गया है कि अब ये परीक्षा नहीं, गला-काट युद्ध जैसी हो गई हैं। उधर कई हेल्प लाइन शुरू हो गई हैं कि यदि बच्चे को तनाव हो तो सम्पर्क करें। जरा सोचें कि बच्चों के बचपन, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की कीमत पर बढ़िया नंबरों का सपना देश के ज्ञान-संसार पर किस तरह भारी पड़ रहा है। कैसी विडम्बना है कि डाक्टर-इंजीनियर या ऐसे ही सपनों को साकार करने के लिए लालायित कक्षा दस के बच्चों, जो बीते दस साल से स्कूल जा रहे हैं, द्वारा वहां बिताया समय और बांची गई पुस्तकें उनको इतनी-सी असफलता को स्वीकार करने और उसका सामना करने का साहस नहीं सिखा पाती हैं। उनमें अपने परिवार, शिक्षक व समाज के प्रति भरोसा नहीं पैदा हो पाता कि महज एक परीक्षा के नतीजे के अच्छे नहीं होने से वे लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। परीक्षा देने जा रहे बच्चे खुद को याद करने से ज्यादा इस बात से ज्यादा चिंतित दिखते हैं कि उनसे बेहतर करने की संभावना वाले बच्चों ने ऐसा क्या रट लिया है जो उन्हें नहीं आता। असल में प्रतिस्पर्धा के असली मायने सिखाने में पूरी शिक्षा प्रणाली असफल हो रही है। मैं अपनी क्षमता के अनुरूप सबसे बेहतर करूं, यही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मूल मंत्र होता है, लेकिन आज की प्रणाली दूसरों की तुलना में अपनी क्षमता आंकने का पाठ पढ़ाती है।
हालांकि नई शिक्षा नीति को आए तीन साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज़मीन पर बच्चे न तो कुछ नया सीख रहे हैं और न ही उसका आनंद ले पा रहे हैं, जो वे पढ़ रहे हैं। बस एक ही दबाव है कि परीक्षा में जैसे-तैसे अव्वल या बढ़िया नम्बर आ जाएं। कई बच्चों का खाना-पीना छूट गया है । सन् 2020 की शिक्षा नीति में भी कहा गया था कि अब बच्चों को परीक्षा के भूत से मुक्ति मिल जाएगी। अब ऐसी नीतियां व पुस्तकें बन गई हैं जिन्हें बच्चे मज़े से पढ़ेंगे। 10वीं के बच्चों को अंक नहीं, ग्रेड देने का काम कई साल से चल रहा है, लेकिन इससे भी बच्चों पर दबाव में कोई कमी नहीं आई है। यह विचारणीय है कि जो शिक्षा 12 साल में बच्चों को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना न सिखा सके, जो विषम परिस्थिति में अपना संतुलन बनाना न सिखा सके, वह कितनी प्रासंगिक व व्यावहारिक है?
12वीं के परीक्षार्थी बेहतर संस्थानों में प्रवेश के लिए चिंतित हैं तो 10वीं के बच्चे अपना पसंदीदा विषय पाने के दबाव में। एक तरफ स्कूलों को अपने नाम की प्रतिष्ठा की चिंता है तो दूसरी ओर हैं मां-बाप के सपने। बचपन, शिक्षा, सीखना सब कुछ परीक्षा के सामने कहीं गौण हो गया है। रह गई है तो केवल नम्बरों की दौड़, जिसमें धन, शरीर, समाज सब कुछ दांव पर लग गया है। 12वीं के बच्चों पर दबाव है कि एक तो बोर्ड में अव्वल आना है, फिर अलग-अलग कालेजों में प्रवेश की परीक्षाओं में मुकाम पाना है।
क्या किसी बच्चे की योग्यता, क्षमता और बुद्धिमत्ता का तकाज़ा महज अंकों का प्रतिशत ही है? वह भी उस परीक्षा प्रणाली में जिसकी स्वयं की योग्यता संदेह से घिरी हुई है। सीबीएसई की कक्षा 10 में पिछले साल दिल्ली में हिन्दी में बहुत-से बच्चों के कम अंक रहे जबकि हिन्दी के मूल्यांकन की प्रणाली को गंभीरता से देखें तो वह बच्चों के साथ अन्याय ही है। कोई बच्चा ‘हैं’ जैसे शब्दों में बिंदी लगाने की गलती करता है, किसी को छोटी व बड़ी मात्रा की दिक्कत है। कोई बच्चा ‘स’ एवं ‘ष’ और ‘श’ में भेद नहीं कर पाता है। स्पष्ट है कि यह बच्चे की महज एक गलती है, लेकिन मूल्यांकन के समय बच्चे ने जितनी बार एक ही गलती को किया है, उतनी ही बार उसके नंबर काट लिए गए यानी मूल्यांकन का आधार बच्चों की योग्यता ना हो कर उसकी कमज़ोरी है। यह सरासर नकारात्मक सोच है जिसके चलते बच्चों में आत्महत्या, पर्चे बेचने-खरीदने की प्रवृत्ति, नकल व झूठ का सहारा लेना जैसी बुरी आदतें विकसित हो रही हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस नंबर-दौड़ में गुम हो कर रह गया है ।
छोटी कक्षाओं में सीखने की प्रक्रिया के लगातार नीरस होते जाने व बच्चों पर पढ़ाई के बढ़ते बोझ को कम करने के इरादे से मार्च 1992 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश के आठ शिक्षाविदों की एक समिति बनाई थी, जिसकी अगुवाई प्रो. यशपाल कर रहे थे। समिति ने देश भर की कई संस्थाओं व लोगों से सम्पर्क किया व जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। उसमें साफ लिखा गया था कि बच्चों के लिए स्कूली बस्ते के बोझ से अधिक बुरा है ना समझ पाने का बोझ। सरकार ने सिफारिशों को स्वीकार भी कर लिया और एकबारगी लगा कि उन्हें लागू करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। फिर देश की राजनीति में सरकारें बदलती रहीं और हर सरकार अपनी विचारधारा जैसी किताबों के लिए ही चिंतित रही। बच्चों की रिपोर्ट की सुध किसी ने नहीं ली।
कुल मिला कर परीक्षा व उसके परिणामों ने एक भयावह सपने, अनिश्चितता की जननी व बच्चों के नैसर्गिक विकास में बाधा का रूप ले लिया है। कहने को तो अंक सूची पर प्रथम श्रेणी दर्ज है, लेकिन उनकी आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूलों ने भी दरवाजों पर शर्तों की बाधाएं खड़ी कर दी हैं। सवाल यह है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है—परीक्षा में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना, विषयों की व्यावहारिक जानकारी देना या फिर एक अदद नौकरी पाने की कवायद? निचली कक्षाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान और ऐसी ही कई योजनाएं संचालित हैं। सरकार हर साल अपनी रिपोर्ट में ‘ड्राप आउट’ की बढ़ती संख्या पर चिंता जताती है, लेकिन कभी किसी ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि अपने पसंद के विषय या संस्था में प्रवेश ना मिलने से कितनी प्रतिभाएं कुचल दी गई हैं। एम.ए. और बी.ए. की डिग्री पाने वालों में कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अपनी पसंद के विषय पढ़े हैं। विषय चुनने का हक बच्चों को नहीं बल्कि उस परीक्षक को है जो कि बच्चों की प्रतिभा का मूल्यांकन उनकी गलतियों की गणना के अनुसार कर रहा है ।
आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा विभाग को कभी गंभीरता से नहीं लिया। इसमें इतने प्रयोग हुए कि आम आदमी लगातार कुंद दिमाग होता गया। हम गुणात्मक दृष्टि से पीछे जाते गए, मात्रात्मक वृद्धि भी नहीं हुई । कुल मिला कर देखें तो शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य और पाठ्यक्रम के लक्ष्य एक दूसरे में उलझ गए व गफलत की स्थिति बन गई। क्या कभी हमारे शिक्षाविद पुराने अनुभवों से कुछ सीखते हुए बच्चों की बौद्धिक समृद्धता को दरपेश चुनौतियों से निबटने की क्षमता के विकास के लिए कारगर कदम उठाते हुए नम्बरों की अंधी दौड़ पर विराम लगाने की सुध लेंगे?
-मो. 98919-28376