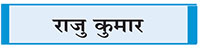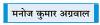बढ़ती डिजिटल निर्भरता के साथ बढ़ रहा ई-वेस्ट का खतरा
इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-वेस्ट) आज दुनिया के सामने एक बढ़ता हुआ पर्यावरणीय खतरा बन चुका है। आधुनिक जीवन में तकनीकी उपकरणों की बढ़ती संख्या ने जहां सुविधाएं बढ़ाई हैं, वहीं इनके अनुपयोगी या अपनी ज़रूरत से कमतर उपयोगी हो जाने के बाद उत्पन्न कचरे ने पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2024 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया भर में लगभग 62 मिलियन टन ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ था और अनुमान है कि वर्ष 2030 तक यह बढ़कर लगभग 82 मिलियन टन तक पहुंच जाएगा। विश्व स्तर पर इसका केवल 22.3 प्रतिशत भाग ही वैज्ञानिक रूप से रीसायकल किया जा रहा है, बाकी या तो खुले में फैंका जा रहा है या लैंडफिल में दबा दिया जाता है।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-वेस्ट उत्पादक देश है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन कार्य, ई-लर्निंग, ई-कॉमर्स और घर से काम करने की प्रवृत्ति ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की खपत को कई गुना बढ़ा दिया। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, कैमरा और नेटवर्किंग उपकरणों की मांग में आई इस अचानक वृद्धि ने ई-वेस्ट को भी तेज़ी से बढ़ाया। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यसभा में 16 दिसम्बर, 2024 प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले पांच वर्षों में ई-वेस्ट उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2019-20 में 10.14 लाख टन (1.01 मिलियन मीट्रिक टन) ई-वेस्ट उत्पन्न हुआ था, जो बढ़ कर वर्ष 2023-24 में 17.51 लाख टन (1.751 मिलियन मीट्रिक टन) हो गया। यह वृद्धि लगभग 72.5 प्रतिशत रही है, जो यह दर्शाता है कि पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों के उपयोग में तेज़ी से वृद्धि के साथ ई-वेस्ट का बोझ भी बढ़ा है। इससे यह स्पष्ट है कि डिजिटल निर्भरता जितनी बढ़ी है, पर्यावरणीय चुनौतियां भी उसी गति से बढ़ी हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता अभी भी सीमित है, वहां ई-वेस्ट एक गंभीर खतरे के रूप में उभर रहा है। पुराने कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर या प्रिंटर जैसे उपकरणों में मौजूद लेड, पारा और कैडमियम जैसी विषैली धातुएं जब मिट्टी या जल में घुलती हैं, तो यह न केवल पर्यावरण, बल्कि मानव शरीर के लिए भी घातक सिद्ध होती हैं। ग्रामीण इलाकों या शहरी झुग्गियों में जहां अनौपचारिक रूप से ई-वेस्ट को जलाकर कीमती धातुएं निकाली जाती हैं, वहां वायु प्रदूषण का स्तर अत्यधिक बढ़ जाता है। ऐसे लोग फेफड़ों और त्वचा से संबंधित गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। भारत में कुल ई-वेस्ट का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा अब भी अनौपचारिक क्षेत्र द्वारा एकत्र और संसाधित किया जाता है। इस प्रक्रिया में पर्यावरण सुरक्षा के मानकों की अनदेखी होती है। सरकार ने ई-वेस्ट (प्रबंधन) नियम 2022 लागू किए हैं, जिनमें उत्पादक कंपनियों को अपने उपकरणों के जीवनकाल के बाद उनके ज़िम्मेदार निपटान की जवाबदेही दी गई है, लेकिन इस नीति का प्रभाव तभी दिखेगा जब इसे सख्ती से लागू किया जाए और नागरिक स्तर पर भी जागरूकता बढ़े।
भारत सरकार ने इस साल के स्वच्छता माह में ‘ई-वेस्ट का निपटान एवं प्लास्टिक का कम से कम उपयोग’ थीम रख कर इस समस्या की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है। इसी क्रम में देशभर में कई सरकारी और औद्योगिक संस्थानों ने ई-वेस्ट प्रबंधन की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इनमें भोपाल की भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) इकाई का उदाहरण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भेल भोपाल ने यह दिखाया कि स्वच्छता केवल सफाई तक सीमित नहीं, बल्कि यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और तकनीकी नवाचार से भी जुड़ी है। पुरानी फाइलों का डिजिटल रूप में परिवर्तित करना और फिजिकल दस्तावेजों का ज़िम्मेदार निपटान एक ऐसा कदम है जो न केवल जगह की बचत करता ह,ै बल्कि कागज़ के अत्यधिक उपयोग को भी रोकता है। वहीं, पुराने कंप्यूटर और प्रिंटरों के व्यक्तिगत रूप से पुन: उपयोग के लिए कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रोत्साहित करनाए ई-वेस्ट को कम करने का व्यावहारिक उपाय है। इससे समाज में नए उपकरणों की आवश्यकता घटती है और पर्यावरण पर बोझ भी कम होता है। सबसे रोचक प्रयोग भेल भोपाल द्वारा मैग्नेटिक स्वीपर के रूप में किया गया, जिसके माध्यम से कारखाने के ब्लॉकों और सड़कों पर बिखरी लोहे की चिप्स को प्रभावी ढंग से एकत्रित किया गया। यह प्रयोग न केवल स्वच्छता बढ़ाने में सहायक साबित हुआ बल्कि धातु के पुनर्चक्रण का भी उत्कृष्ट उदाहरण बना। इस तरह के नवाचार उद्योगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, जिससे ई-वेस्ट कम करने की दिशा में ठोस प्रगति हो। (संवाद)