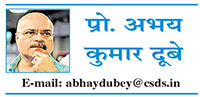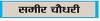रोग पता होने पर भी वित्त मंत्री ने इलाज क्यों नहीं किया ?
घोषित रूप से तो निर्मला सीतारमण ने बिहार को 60,000 करोड़ रुपए और आंध्र को 15,000 करोड़ रुपए ही दिये हैं। लेकिन, आंध्र से उन्होंने बजट से पहले 60 हज़ार करोड़ रुपए का पैकेज देने का ़खामोश वायदा भी कर रखा है। इस बात पर पड़ा पर्दा बजट पेश होते ही तेलुगु देशम के प्रवक्ता ने मीडिया में हटा दिया। सोचने की बात है कि अगर वित्त मंत्री ने दो गठजोड़ पार्टनरों के दबाव में पूरे एक लाख तीस हज़ार करोड़ रुपए केवल दो राज्यों को न दे दिये होते तो यह रकम किन-किन दूसरे मदों में आबंटित की जा सकती थी। इतनी बड़ी रकम से वित्त मंत्री कई राज्यों की ज़रूरतों को पूरा कर सकती थीं। प्रश्न यह है कि क्या इस रकम का 30-30 प्रतिशत जनता दल-यू और तेलुगु देशम पार्टी को देकर काम नहीं चलाया जा सकता था? क्या वे दोनों एनडीए छोड़ कर चले जाने की स्थिति में थे? ज़ाहिर है कि या तो मोदी-शाह को गठजोड़ सरकार चलाना नहीं आता, या फिर वे अपनी सरकार की अस्थिरता की कमज़ोर सी संभावनाओं से भी घबड़ाते हैं। लेकिन, उन्होंने जो किया है, उससे आर्थिक दायरे में पराजय की भरपायी करने की उनकी क्षमताओं में और कमी हो गई है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 4 जून को आये नतीज़ों का साया इतने अनिष्टकारी अंदेशों के साथ 23 जुलाई के बजट पर मंडराता हुआ दिखेगा।
वित्त मंत्री जब नयी सरकार का पहला बजट बनाने चली थीं, तो उन्हें पता था कि अर्थ-व्यवस्था के वे कौन-कौन से रोग हैं जिनका इलाज करने की तरफ बढ़ना उनके लिए ज़रूरी साबित होने वाला है। एक दिन पहले जारी किया गया आर्थिक सर्वेक्षण इस बात का सबूत है कि रोगों की सूची में सबसे ऊपर बेरोज़गारी का नाम था। आने वाले कई वर्षों तक सरकार को हर साल कम से कम 77 लाख नौकरियां देनी हैं। दूसरे नंबर पर निजी क्षेत्र का रवैया था। सर्वेक्षण में साफ कहा गया था कि निजी क्षेत्र अपने मुनाफे में आये ज़बरदस्त उछाल (30 प्रतिशत) के बावजूद नये रोज़गारों का सृजन नहीं कर पा रहा है। न ही वह अर्थव्यवस्था में नये निवेश करने की ज़िम्मेदारी निभाने के लिये तैयार है। उसकी इस दुहैरी अक्षमता के कारण कई साल से केवल सरकार ही नया निवेश करती रही है, और केवल सरकार को ही बेरोज़गारी की समस्या का समाधान न कर पाने को तोहमत का सामना करना पड़ रहा है।
कुछ रोग ऐसे भी हैं जिनका आर्थिक सर्वेक्षण में तो ज़िक्र नहीं था, लेकिन यह मानना नामुमकिन है कि वित्त मंत्री को उनकी जानकारी न हो। मसलन, अर्थव्यवस्था पर निगाह रखने वाला हर व्यक्ति जानता है कि भारत का असंगठित क्षेत्र 2016 की नोटबंदी के बाद से हर वर्ष पांच प्रतिशत की रफ्तार से गिर रहा है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसका महत्व देश की जनता के लिए निजी और सरकारी उद्यमों के तहत चलने वाले संगठित क्षेत्र (उद्योग, कृषि और सेवा) से भी ज्यादा समझा जाता है। आ़िखरकार इसमें देश की श्रमशक्ति का 94 प्रतिशत हिस्सा सक्रिय रहता है। बेरोज़गारी बढ़ने में इसकी प्रमुख भूमिका है। सर्वेक्षण में यह भी स्वीकार नहीं किया गया था कि लम्बे समय से हमारा बाज़ार मांग के ‘एनीमिया’ का शिकार है। जिस तरह कुपोषित बच्चे का सिर बड़ा और देह सूखी हुई होती है, उसी तरह बाज़ार में केवल ‘हाई एंड’ चीज़ें ही बिक रही हैं। छोटे और मंझोले स्तर के बिना बिके उत्पादन से वेयरहाउस भरे पड़े हैं।
सर्वेक्षण ने यह भी नहीं माना था कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र को पर्याप्त निवेश का पौष्टिक आहार आज़ादी के बाद से शायद ही कभी मिला हो। लेकिन यह भी नहीं माना जा सकता कि वित्त मंत्री मांग की कमी और शिक्षा-स्वास्थ्य की कुपोषित देह के यथार्थ से परिचित न हों। मोटे तौर पर इन सभी रोगों को मिला लिया जाए तो एक आंकड़ा सामने आता है। भारत प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में दुनिया में 142वें नंबर पर है। यह हमारी अर्थव्यवस्था की अरसे से अनसुलझी समस्याओं का संचित परिणाम है।
ज़ाहिर है कि एक बजट में ऐसे पुराने या नये सभी रोगों का इलाज सम्भव नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम यह तो हो ही सकता था इन समस्याओं को स्वीकार करके इनका कुछ दूरगामी इलाज प्रस्तावित किया जाता। कहना न होगा कि बजट में सरकार बेरोज़गारी से निबटने के लिए कुछ जद्दोजहद करते दिखती है। सरकार पहली बार निजी क्षेत्र को उसकी ज़िम्मेदारियां याद दिलाते हुए भी दिखती है। लेकिन, क्या इस दिखने को ठोस रूप से करने का पर्याय माना जा सकता है? सरकार ने नौकरियां देने की ज़िम्मेदारी निजी क्षेत्र को दे दी है। क्या पहली तऩख्वाह की सब्सिडी, इंटर्नशिप की छोटी सी सब्सिडी और मुद्रा योजना में कज़र् की सीमा दस से बढ़ा कर बीस लाख कर देने को ऊँट के मुँह में ज़ीरा नहीं माना जाएगा? जब निजी क्षेत्र की ़फैक्ट्रियां केवल 70-75 प्रतिशत क्षमता पर ही चलेंगी, तो वह नये कारखाने क्यों लगाएगा? यानी नया निवेश क्यों करेगा? सब्सिडी का लाभ लेने के लिए नयी नौकरियां कैसे देगा? जब मुद्रा योजना में स्वरोज़गार के लिए ऋण उठाने का सामान्य औसत पचास हज़ार रुपये ही है, तो उसका शीर्ष ऋण यानी बीस लाख रुपए केवल गिने-चुने व्यक्तियों के अलावा और कौन उठायेगा?
अर्थव्यवस्था मनुष्य के शरीर की तरह होती है। सारे अंग एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। जिन देशों में शिक्षा (केवल सवा लाख करोड़ की बढ़ोतरी) और स्वास्थ्य (सिर्फ 89,000 करोड़ की वृद्धि) पर खर्च नहीं किया जाता, उनके पास विकास के इंज़िन को खींचने वाला स्वस्थ और वास्तविक रूप से शिक्षित नागरिक ही नहीं होता। हमारे 75 प्रतिशत ग्रेजुएट ‘नौकरी देने लायक’ ही नहीं होते। हमारे यहां स्त्रियों और पुरुषों का कद घटता जा रहा है। केवल उनकी संख्या बढ़ रही है। ये लोग ऊंची प्रौद्योगिकी वाली मैन्य़ुफैक्चरिंग में लगाये जाने काबिल ही नहीं हैं। यानी, भारत की ज्यादातर आबादी निचले स्तर वाले कौशलों में ही खप सकती है।
वित्त मंत्री चाहतीं तो इस बजट में एक नयी परम्परा डाल सकती थीं। निजी अस्पतालों और निजी विश्वविद्यालयों पर भरोसा करने के बजाय स्वास्थ्य-शिक्षा पर आबंटन जम कर बढ़ाने का क्रांतिकारी ़कदम उठाया जा सकता था। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं को स्वीकार करके उसके आंकड़े जमा करके जीडीपी की वास्तविक तस्वीर सामने लाई जा सकती थी। कृषि के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने या उसका कॉरपोरेटीकरण करने के बजाय किसानों की आमदनी बढ़ाने के तरीके तलाश करने के लिए एक उच्चाधिकार सम्पन्न कमिशन बनाया जा सकता था। हालांकि मनरेगा को 86,000 करोड़ दिया गया है, लेकिन नीति आयोग के सुझाव पर अमल करते हुए ‘एक अरबन मनरेगा’ की शुरुआत की जा सकती थी। आ़िखरकार बेरोज़गारी एक टाइम बम है जिसकी लगातार टिक-टिक किसी भी नेता की लोकप्रियता का क्षय कर सकती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ज्यादा बड़ा इसका सबूत और क्या हो सकता है?
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।