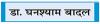बसंत, तुम कब आओगे!
अपने आगमन की तारीख पर भी बसंत सोया पड़ा था या उकड़ूं होकर चिंतन की मुद्रा में था। चिन्ता और चिन्तन आज के सत्य हैं। चिन्ता है तो चिन्तन ज़रूरी है, लेकिन आज चिन्तन हाशिए पर है। चहूं ओर चिन्ता का ही साम्राज्य है। बाहर कंपकंपी वाली ठंड थी और बसंत के पास रजाई भी नहीं थी। उठे बगैर गुज़ारा न होते देख वह अनमने से उठा और एक किसान की चौखट पर आकर उसने गुहार लगाई। भईया थोड़ी-सी रूई उधार दे दो, रजाई बनवानी है। अभी चुकाने के पैसे नहीं हैं, मंदी का दौर चल रहा है। उधर सर्दी है कि जाने का नाम नहीं ले रही। बसंत के मौसम में भी पसरी पड़ी है, जैसे महंगाई बारहों महीने पसरी पड़ी रहती है। मुआं प्याज ही सोने की तरह नाज-नखरे दिखलाता रहता है। किसान ने अपनी मरियल आंखें खोलीं और मायूसी में बोला- ‘बसंत भैया, तुम्हें रुई की क्या आवश्यकता, कुछ लोग तो कड़ाके की ठंडी के मौसम में भी फुटपाथ पर अपना पूरा जीवन बिना रजाई व्यतीत कर लेते हैं। उनकी बहादुरी को सलाम। फिर तुम तो बसंत हो, कलियों के मुस्काने का मौसम, फूलों के इठलाने का मौसम, भौरों के गाने का मौसम, सर्दी के जाने का मौसम। बसंत ने अपनी बेबसी के दर्द को न छिपाते हुए कहा-‘भैया, समय की सूई शायद अब विपरीत दिशा में घूमनी आरम्भ हो चुकी है। बसंत का मौसम कहलाने भर को है, मुई सर्दी पीछा नहीं छोड़ रही जैसे भ्रष्टाचार नहीं छोड़ता। गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है। मुझे भी एक अद्द रजाई की ज़रूरत है। किसान भाई ने अपनी फटी हुई चादर को अपने शरीर के गिर्द कस कर लपेटते हुए कहा- ‘भईया, मेरे पास भी रजाई कहां। मेरे पास रूई होती तो अपने लिए अवश्य ही एक-आध बनवा लेता। साहूकार ने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। कज़र् का बोझ ढोते-ढोते मेरी अपनी हड्डियां निकल आई हैं। असली बसंत तो सूदखोरों का है।’बसंत निराश था। उसकी शोभा का वर्णन अब कवियों की कविताओं में ही रह गया था। या बसंत उन नेताओं की सोचों में सिमट गया था, जो चुनाव के समय मतदाताओं को आश्वासनों की अफीम चटाते हैं ताकि पांच वर्षों तक गुलाबी बसंत का लुत्फ उठा सकें। बसंत उन व्यापारियों की तिजौरी में भी है जो चौड़ा सीना करके दो का तेरह कर लेते हैं। सरकार भी उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती। जीते हुए नेताओं को चुनाव के समय लिए गये चंदों का ‘रिर्टन-गिफ्ट’ तो देना ही होता है, वरना कृतघ्नता का अभिशाप मिल सकता है। बसंत उन सरकारी कर्मचारियों की बपौती भी होता है जो भ्रष्टाचार की हांडी पर अपना हलवा-मंडा पका लेते हैं। पुल बनवाने वाले इंजीनियर साहिब रेत और गारे का पुल बनवाकर अपना और अपने आकाओं का बसंत सदाबहार रखने की कुव्वत रखते हैं। बाकी लोगों के लिए चिंता और चिंतन का प्रसाद ही बचता है। उन्हीं के दम पर अपनी बची-खुची ज़िन्दगी गुज़ार लेते हैं। मुर्झाये फूलों की तरह मुर्झाये चेहरे समय के कंगूरों पर लटके रहते हैं। मटमैले आकाश की तरफ ताकते हैं और पूछते हैं कि आस्था के बसंत तुम कब आओगे। उधर बसंत अपने लिए एक अद्द रजाई की तलाश में हैं। लम्बा सर्दियों का मौसम जाने का नाम नहीं ले रहा।
-मो. 94171-08632