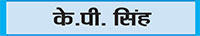बाघों के संरक्षण से समूचा पारिस्थितिकीय तंत्र सुरक्षित रहता है
29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर विशेष
हर साल 29 जुलाई के दिन ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत साल 2010 में रूस स्थित सेंट पीर्ट्सबर्ग में आयोजित ‘टाइगर समिट’ के दौरान हुई। वास्तव में उस समय दुनिया में बाघों की संख्या बहुत तेज़ी से घट रही थी। सम्मेलन में 13 बाघ रक्षित देशों में एक भारत भी शामिल था। इस सम्मेलन में यह साझा संकल्प लिया गया था कि साल 2022 में बाघों की संख्या दोगुनी की जायेगी। भारत ने यह लक्ष्य चार साल पहले यानी 2018 में ही हासिल कर लिया था। 2010 में भारत में बाघों की संख्या 1706 थी और 2018 में बढ़कर लगभग 3000 हो गई थी, जो कि करीब लक्ष्य पूर्ति के बराबर थी। साल 2022-23 में भारत में बाघाें की संख्या बढ़कर 3682 हो गई, जो कि वैश्विक बाघ आबादी का करीब 70 प्रतिशत है। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ और ग्लोबल टाइगर फॉर्म की 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में बाघों की संख्या 5574 आंकी गई थी। भारत के बाद सबसे ज्यादा बाघ रूस में, इसके बाद इंडोनेशिया और फिर नेपाल व भूटान में हैं।
सवाल है भारत के लिए बाघों का क्या महत्व है और अब तक के बाघ संरक्षण का भारतीय अनुभव क्या रहा है? दरसअल भारत के लिए बाघ या टाइगर केवल एक वन्यजीव नहीं है बल्कि यह हमारे राष्ट्रीय गौरव, पारिस्थितिकीय संतुलन का रक्षक और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। भारत में बाघ यानी रॉयल बंगाल टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है। बाघ को शक्ति, गर्व, आत्मविश्वास और चपलता का प्रतीक माना जाता है। क्योंकि बाघ पारिस्थितिकीय संतुलन में फूड चेन का शीर्ष शिकारी है, जो शाकाहारी प्रजातियों की संख्या को नियंत्रित करके जैव विविधता बनाये रखता है। इसलिए जहां बाघ सुरक्षित हैं, वहां जंगल भी स्वस्थ और समृद्ध होते हैं। भारत की संस्कृति से बाघाें का बहुत पुराना और अलौकिक रिश्ता रहा है। हमारी पौराणिक कथाओं में बाघ का जिक्र आता है। हमारी देवी दुर्गा की सवारी बाघ ही है। बाघ का बार-बार जिक्र हमारी लोककथाओं में आता है और भारत में जब से पेंटिंग का इतिहास शुरु होता है, हमेशा बाघ की पेंटिंग बनती रही है। इस तरह देखें तो बाघ हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताओं और हमारे लोकजीवन का हमेशा हिस्सा रहा है।
अगर बाघ न हो तो भारत में आदिवासी समुदायों की कहानियां फीकी पड़ जाएं। वास्तव में उनकी कहानियों को मानवीय जीवंतता और गौरव बाघ की उपस्थिति से ही मिलती है। भारत में बाघ संरक्षण का सिलसिला बहुत पहले सन् 1973 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जरिये शुरु हुआ था। शुरुआत में भारत में बाघों के संरक्षण के लिए 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 53 हो चुकी है। बाघों से संबंधित लिटरेचर में हाल के सालों में एक संकेत आता रहा है, जिसका मतलब था साल 2022 तक बाघों की संख्या को दोगुनी करना है। लेकिन भारत ने यह लक्ष्य समय से पहले 2018 में ही पूरा कर लिया था। आज बाघ संरक्षण में भारत दुनिया का न केवल अग्रणी देश है बल्कि पूरी दुनिया को बाघ संरक्षण के सफल तौर तरीके सिखा रहा है। आज भारत बाघों के संरक्षण में आधुनिक टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है जैसे- कैमरा ट्रैप, जीपीएस कॉलर, ड्रोन निगरानी और मोबाइल एप्स के जरिये बाघ संरक्षण पर नियंत्रण रख रहा है। भारत की विकसित की हुई एम-स्ट्रिप निगरानी प्रणाली पूरी दुनिया में सराही गई है। इसमें डिजिटल सिस्टम से निगरानी की जाती है।
सवाल है बाघ इस कदर विलुप्ति की कगार पर क्यों पहुंच गये थे? बाघों के विलुप्त होने के कगार में पहुंचने का सबसे बड़ा कारण बाघों का अंधाधुंध शिकार था। एक जमाने में बाघों का शिकार मर्दानगी और शिकार संबंधी कुशलता का पर्याय समझा जाता था। इसी कारण पूरी दुनिया में बाघों का इतना ज्यादा शिकार हुआ कि वे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गये। इसीलिए भारत में 70 और 80 के दशक में बाघ संरक्षण पर जोर दिया गया और आज हम किसी तरह से बाघों का संरक्षण कर पाने में सफल हैं लेकिन बाघों के लिए अभी भी समस्याएं कुछ कम नहीं हुईं। पहले जहां उनके खात्मे का सबसे बड़ा कारण शिकार की आदत थी, वहीं आज बाघों के खात्मे के पीछे सबसे बड़ा कारण उनकी अवैध तस्करी है। दरअसल दुनिया के कई हिस्सों में विशेषकर चीन में यह धारणा बनी हुई है कि बाघ की हड्डियों का सेवन करने से यौन क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ती है। इस कारण चीन में चोरी छुपे एक-एक बाघ करोड़ों रुपये में बिक जाता है। नतीजतन तमाम राष्ट्रीय संरक्षण नीतियों के बावजूद अवैध शिकारी बाघ का शिकार करने से नहीं चूकते।
बाघों के खात्मे का एक बड़ा कारण वनों की कटाई और मौजूदा वनों का अतिक्रमण भी है। वनों की कटाई के कारण भारत में बाघाें का आवास लगातार संकुचित होता जा रहा है। जंगलों के आसपास बसे गांवों में इसलिए बाघों के इंसानों पर हमले की घटनाएं बढ़ रही हैं। बाघों के संरक्षण की एक समस्या बाघ कारिडोरों की कमी भी है, जिस कारण बाघों को एक सुरक्षित क्षेत्र से दूसरे सुरक्षित क्षेत्र में जाने की जगह नहीं मिलती। इन सब समस्याओं के बावजूद भारत में बाघ संरक्षण का अनुभव काफी सकारात्मक है।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर