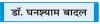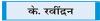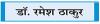रूस, चीन और भारत कर रहे व्यापार स्वायत्तता के प्रयास
डोनाल्ड ट्रम्प की आक्रामक टैरिफ व्यवस्था, जिसे अमरीकी ताकत बढ़ाने और खोई हुई आर्थिक ज़मीन वापस पाने के नाम पर शुरू किया गया है, ने दुनिया भर में एक ऐसी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है जो अंतत: उस लक्ष्य को ही विफल कर सकती है जिसे वह हासिल करना चाहती है। अमरीका की आर्थिक प्रधानता का दावा करने के लिए एक राष्ट्रवादी परियोजना के रूप में तैयार किया गया, यह टैरिफ युद्ध एक ध्रुवीय अमरीकी प्रभुत्व से एक वास्तविक बहु-ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर तेज़ी से बढ़ते वैश्विक बदलाव का उत्प्रेरक बन गया है। जो कभी काफी हद तक काल्पनिक था (एक वैश्विक आर्थिक ढांचे का विचार जो वाशिंगटन पर केंद्रित न हो) अब मूर्त रूप ले रहा है क्योंकि ट्रम्प की व्यापार संबंधी अस्थिरता अन्य देशों को पुनर्विचार करने, पुनर्गठित होने और पुनर्संरेखित करने के लिए मजबूर कर रही है।
ट्रम्प की रणनीति की मूल खामी यह मानकर चलती है कि बाकी दुनिया आर्थिक दबाव के बोझ तले अमरीकी मांगों के आगे झुक जाएगी, लेकिन दुनिया ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय अन्य देश उस आर्थिक दबाव का विरोध करने में साझा कारण ढूंढ रहे हैं जिसे वे बातचीत के रूप में देखते हैं। इसका परिणाम शक्तियों का एक परिवर्तनशील लेकिन लगातार सुसंगत पुनर्गठन है (जिनमें चीन, रूस और भारत प्रमुख हैं) जो अमरीका के वास्तविक प्रति-धुरी के रूप में कार्य करने लगे हैं। साझा शिकायतों और अपनी सामरिक स्वायत्तता की रक्षा के साझा उद्देश्य से प्रेरित होकर ये देश व्यापार, निवेश और ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक निकटता से सहयोग कर रहे हैं।
विडम्बना यह है कि आर्थिक वर्चस्व की ट्रम्प की कोशिश उसी व्यवस्था के क्षरण को तेज़ कर रही है जिसने दशकों तक अमरीकी प्रभुत्व को संभव बनाया।
चीन, जो लम्बे समय से ट्रम्प के टैरिफ का प्रमुख निशाना रहा है, ने जवाबी कार्रवाई और पुनर्निर्देशन, दोनों के साथ जवाब दिया है। वाशिंगटन की मांगों के आगे झुकने के बजाय चीन ने अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, विशेष रूप से एशिया और अफ्रीका में अपनी पहुंच का विस्तार किया है, साथ ही रूस और भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई), जिसे शुरू में वैश्विक बुनियादी ढांचे से जुड़ने के साधन के रूप में देखा गया था, अब आर्थिक पुनर्संरेखण का एक साधन भी बन गई है। जहां ट्रम्प टैरिफ की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, वहीं चीन सड़कें, बंदरगाह और वित्तीय नेटवर्क बना रहा है जो अमरीका को बाईपास करते हैं। मास्को ने अपनी ओर से इस बदलाव का स्वागत किया है। अमरीकी और यूरोपीय प्रतिबंधों से अलग-थलग पड़े रूस को चीन और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों में अवसर दिखाई दे रहे हैं, दोनों ने पश्चिमी दबाव का सामना करने की बढ़ती इच्छा दिखाई है।
भारत, हालांकि पारम्परिक रूप से पश्चिम के साथ अधिक जुड़ा हुआ है और वैश्विक उदार बाज़ारों में एक उत्साही भागीदार है, ने खुद को उभरते गैर-पश्चिमी धुरी की ओर बढ़ता हुआ पाया है। भारतीय वस्तुओं पर ट्रम्प के टैरिफ और उनके प्रशासन द्वारा रूस के साथ व्यापार करने वाले या ईरानी तेल खरीदने वाले देशों पर द्वितीयक प्रतिबंधों की धमकियों ने नई दिल्ली को लाल रेखाएं खींचने के लिए मजबूर कर दिया है। उदाहरण के लिए रूसी तेल पर भारत का रुख स्पष्ट रहा है—यह राष्ट्रीय हित और ऊर्जा सुरक्षा का मामला है। वाशिंगटन द्वारा इन खरीदों को कम करने के किसी भी प्रयास को न केवल आर्थिक हस्तक्षेप माना जाता है, बल्कि संप्रभु निर्णय लेने की प्रक्रिया को सीधी चुनौती भी माना जाता है। बदले की कार्रवाई में भारत ने प्रमुख रक्षा सौदों को रद्द करने का दबाव बनाया है, जिसमें एफ-35 लड़ाकू विमानों की प्रस्तावित खरीद भी शामिल है—एक प्रतीकात्मक उपेक्षा जो रणनीतिक संरेखण के व्यापक पुनर्मूल्यांकन का संकेत देती है।
इस पुनर्संरेखण को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने वाली बात इसका व्यापक दायरा है। यह केवल जवाबी शुल्क या कूटनीतिक बयानबाजी का मामला नहीं है, इसमें बुनियादी ढांचे पर सहयोग, तकनीकी एकीकरण और दीर्घकालिक निवेश योजना भी शामिल है। ऐतिहासिक मतभेदों के बावजूद चीन और भारत ने हाल के महीनों में व्यापार सुगमता और क्षेत्रीय सम्पर्क पर बातचीत बढ़ाई है। दोनों देशों के लिए एक साझा ऊर्जा साझेदार और सैन्य आपूर्तिकर्ता के रूप में रूस की भूमिका उसे इस त्रिकोण में बढ़त दिलाती है।
व्यापक रूप से ट्रम्प ने अनजाने में वैश्विक शक्ति संरचना की पुनर्कल्पना को जन्म दिया है। शीत युद्ध के बाद के अमरीकी नेतृत्व वाले वैश्वीकरण के भ्रम की जगह एक अधिक बहुलवादी, प्रतिस्पर्धी और खंडित व्यवस्था ले रही है। उभरती शक्तियां अब वाशिंगटन में लिखे नियमों से चलने से संतुष्ट नहीं हैं। वे समानांतर प्रणालियां बना रही हैं। चीन का डिजिटल युआन अब डॉलर पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखता है। भारत और रूस ने रुपया-रूबल व्यापार तंत्र को पुनर्जीवित किया है। आरसीईपी जैसे क्षेत्रीय व्यापार समझौते अमरीकी भागीदारी के बिना काम कर रहे हैं। जो पैदा हो रहा है वह एक नए प्रकार का वैश्वीकरण है—कम पदानुक्रमित, अधिक संतुलित और किसी एक देश पर बहुत कम निर्भर। (संवाद)