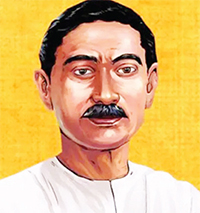कहानीकार ही नहीं, समाज के शिल्पकार थे प्रेमचंद
हिन्दी साहित्य की कालजयी परंपरा में यदि किसी साहित्यकार ने अपनी लेखनी से समाज की आत्मा को टटोला, उसकी पीड़ा को आत्मसात किया और शब्दों के माध्यम से उसके कष्टों का समाधान खोजने की कोशिश की तो वह थे मुंशी प्रेमचंद। उनका समूचा साहित्य सामाजिक यथार्थ का एक ऐसा आईना है, जिसमें आम आदमी की बेबसी, उसकी संघर्षशीलता और उसके अंतर्मन की गूंज को स्पष्ट सुना जा सकता है। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य को केवल मनोरंजन का साधन नहीं माना बल्कि उसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया और इसीलिए वे केवल लेखक नहीं बल्कि एक युगप्रवर्तक विचारक और समाज सुधारक बन गए।
मुंशी प्रेमचंद के लेखन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जीवन की जटिलताओं को अत्यंत सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे। उनकी कहानियों और उपन्यासों में जिस गहराई और मार्मिकता के साथ आम आदमी की पीड़ा उकेरी गई, वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है, जितनी उनके समय में थी। उन्होंने न केवल साहित्य को जनसरोकारों से जोड़ा बल्कि उसे आमजन का हथियार बना दिया। प्रेमचंद ने अपने पात्रों के माध्यम से समाज की उन परतों को उजागर किया, जिन्हें अधिकांश लेखक या तो नज़रअंदाज कर देते थे या छूने से कतराते थे। उनकी रचनाएं उस समय के समाज की सच्ची दस्तावेज बनकर उभरी। आज जब हम उनकी 145वीं जयंती मना रहे हैं, तब यह स्मरण करना आवश्यक हो जाता है कि प्रेमचंद महज एक साहित्यकार नहीं थे, वे अपने समय के सामाजिक यथार्थ के प्रवक्ता थे। उनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के लमही गांव में हुआ था। उनके पिता अजायबलाल डाक विभाग में क्लर्क थे। बचपन से ही आर्थिक तंगी और पारिवारिक संघर्षों से जूझते हुए प्रेमचंद ने जीवन की सच्चाइयों को निकट से देखा और यही उनके लेखन की प्रेरणा बनी। मां का साया बचपन में ही उठ गया और सौतेली मां की उपेक्षा ने उन्हें और अधिक संवेदनशील बना दिया। पिता की मृत्यु के बाद जैसे-तैसे उन्होंने जीवन को संभाला लेकिन कम उम्र में हुआ विवाह भी उनके लिए अभिशाप बन गया। उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वह विवाह उनके जीवन का सबसे त्रासद अनुभव था।
प्रेमचंद के जीवन की विषम परिस्थितियों ने उन्हें जीवन के यथार्थ को बहुत गहराई से समझने का अवसर दिया। वे वकील बनना चाहते थे लेकिन आर्थिक अभावों ने उन्हें शिक्षक बना दिया। उनके भीतर साहित्यिक चेतना की जो चिंगारी बचपन से सुलग रही थी, उसने किशोरावस्था में ही उन्हें लेखनी की ओर मोड़ दिया। गोरखपुर से उन्होंने उर्दू में लेखन की शुरुआत की और ‘नवाब राय’ के नाम से लिखना प्रारंभ किया। 1909 में उनका उर्दू में पहला कहानी संग्रह ‘सोज-ए-वतन’ प्रकाशित हुआ, जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया। उसके बाद उन्हें ‘प्रेमचंद’ नाम से लिखने का सुझाव मिला और यहीं से आरंभ हुआ हिन्दी साहित्य के इस महानायक का कालजयी सफर। प्रेमचंद की लेखनी में एक ओर जहां गांधीवादी आदर्श और भारतीयता की आभा दिखती है, वहीं दूसरी ओर वे सामाजिक रूड़ियों, जाति भेद, स्त्री शोषण, सामंतवाद और पूंजीवादी व्यवस्था की तीव्र आलोचना करते नज़र आते हैं। उन्होंने अपने समय की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था, धार्मिक पाखंड और सामाजिक विषमताओं को इतनी ईमानदारी से प्रस्तुत किया कि उनका साहित्य सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बन गया। सुमित्रानंदन पंत ने ठीक ही कहा था कि प्रेमचंद ने नवीन भारतीयता और नवीन राष्ट्रीयता का समुज्ज्वल आदर्श प्रस्तुत कर महात्मा गांधी के समान देश का मार्ग दर्शन किया।
जिस समय समाज में बाल विधवाओं की दुर्दशा पर किसी की दृष्टि नहीं जाती थी, प्रेमचंद ने उस समय न केवल विधवा विवाह का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह कर समाज के रूड़िवाद को चुनौती दी। उनके उस साहसिक निर्णय ने उनके निजी जीवन को भी स्थायित्व दिया और लेखन में भी एक नई परिपक्वता आई। लेखन की व्यस्तताओं के बीच वे नौकरी में भी थे लेकिन महात्मा गांधी के भाषणों से प्रभावित होकर उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और स्वतंत्र लेखन को अपना मिशन बना लिया। प्रेमचंद का साहित्यिक अवदान अत्यंत व्यापक है। उन्होंने 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल साहित्य की पुस्तकें और हजारों लेख, संस्मरण, आलोचनाएं इत्यादि लिखी। उनके उपन्यास ‘गोदान’ को हिन्दी साहित्य का क्लासिक माना जाता है, जो किसान जीवन की पीड़ा और शोषण को इतनी सजीवता से प्रस्तुत करता है कि वह आज भी समाज के हर तबके को झकझोर देता है।
अपने जीवन के अंतिम वर्षों में प्रेमचंद जलोदर की बीमारी से पीड़ित हो गए थे। लंबे समय तक बीमारी से जूझने के बाद 8 अक्तूबर 1936 को उन्होंने इस संसार से विदा ली लेकिन उनके विचार, उनकी रचनाएं और उनकी लेखनी आज भी उतनी ही प्रासंगिक और जीवंत हैं। वे अपने पीछे एक ऐसा साहित्यिक भंडार छोड़ गए हैं, जो हिन्दी साहित्य की नींव बन चुका है। आज भी उनका साहित्य हर पीढ़ी के पाठकों को प्रेरित करता है, झकझोरता है और सोचने को विवश करता है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं न केवल भारतीय साहित्य की धरोहर हैं बल्कि सामाजिक चेतना की अमिट विरासत भी हैं। उन्होंने जो लिखा वह आज भी समाज को दिशा देने की क्षमता रखता है। वे आज भी उतने ही जीवित हैं, जितना अपने जीवनकाल में थे।