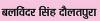‘सहकारी संघवाद’ का स्थान ले चुका है ‘राज्यपालवाद’
क्या किसी को इस समय ‘सहकारी संघवाद’ का ़िफकरा याद है? यह एक ऐसी राजनीतिक अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रचलित किया था। दरअसल, केन्द्र की सत्तारूढ़ पार्टी ने सहकारी संघवाद की शब्दावली और भावना को पूरी तरह से उठा कर ताक पर रख दिया है। संघवाद के नाम पर एक नये तरह का केंद्रवाद प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत राज्यपालों और उप-राज्यपालों द्वारा एक नयी भूमिका अपनायी जा रही है, जिसके तहत वे समांतर मुख्यमंत्री की तरह काम करते हुए दिख रहे हैं। इसे संघवाद कहना ही नहीं चाहिए। यह तो खुला ‘राज्यपालवाद’ है। केरल में आऱिफ मुहम्मद खान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के खिलाफ, तमिलनाडु में रवींद्र नारायण रवि स्टालिन की डी.एम.के. सरकार के खिलाफ, पुडुचेरी में उप-राज्यपाल किरण बेदी (सेवामुक्ति से पहले) कांग्रेस की सरकार के खिलाफ और दिल्ली में उप-राज्यपाल सक्सेना अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ जिस तरह से सक्रिय हैं, उससे केन्द्र सरकार ने बिना घोषित किये अपने इरादे साफ कर दिये हैं। वह राज्यों में किसी भी ़गैर-भाजपा सरकार को चैन से नहीं चलने देगी। अगर भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती तो वह राज्यपालों के ज़रिये राज्य में निर्वाचित सरकारों के काम में हस्तक्षेप तो कर ही सकती है। कुछ इस तरह से कि राजभवन विपक्षी राजनीति का केन्द्र बन जाए। इन राज्यपालों ने पिछले दिनों जो कदम उठाये हैं, उनसे साफ लगता है कि उनके कामों के पीछे एक नियोजित एजेंडा काम कर रहा है। राजनीति की जानकारी न रखने वाले भी समझ सकते हैं कि यह एजेंडा कहां से आ रहा है।
इस ‘राज्यपालवाद’ की शुरुआत व्यावहारिक रूप से उस समय हुई थी, जब पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ राज्यपाल थे। उनका आचरण एक अघोषित मुख्यमंत्री के तौर पर था, जो ममता बनर्जी के मुकाबले समांतर रूप से सक्रिय दिख रहे थे। ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी विधानसभा के प्रति जवाबदेह न होकर राज्यपाल के प्रति जवाबदेह हों। आज धनखड़ साहिब उप-राष्ट्रपति बन चुके हैं। अब वे अपने वक्तव्यों द्वारा उन नयी सीमाओं के निर्धारण करने का आग्रह कर रहे हैं, जो उनकी राय में विधानपालिका द्वारा बनाये गये कानूनों की समीक्षा करने के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार पर दोबारा विचार किया जाना चाहिए। केन्द्र सरकार राज्यपालों का दुरुपयोग करती रही है। उनके ज़रिये राज्य सरकारों को अपदस्थ करने का राजनीतिक खेल खेला जाता रहा है। लेकिन, इस समय राज्यपाल के पद के ज़रिये जो किया जा रहा है, वह कुछ अलग तरह का है। निर्वाचित राज्य सरकार को अपदस्थ करने के बजाय राज्यपाल की ‘अतिसक्रियता’ के ज़रिये उसके कामकाज को लगातार बाधित किया जा रहा है। ़खास बात यह है कि भाजपा शासित राज्यों के राज्यपाल चुपचाप राजभवन में बैठे रहते हैं और विपक्ष शासित राज्यों के राज्यपाल सुनिश्चित कर रहे हैं कि वे सरकार को चैन से काम नहीं करने देंगे। यह संघवाद की जगह चलाया गया ‘राज्यपालवाद’ है।
राज्यों में सरकार चला रही विपक्षी पार्टियों ने इस परिस्थिति को पहले ही भाँप लिया था। इसलिए एक फेडरल फ्रंट की भूमिका बननी शुरू हो गई थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार का तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल के ड्राइंग रूम में लम्बा धरना, आई.ए.एस. अ़फसरों का अंतत: उसके सामने झुकना और अकाली दल को छोड़कर सभी ़गैर-भाजपा पार्टियों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों का इस धरने के समर्थन में आ जाना इस रुझान का पक्का सबूत था। कांग्रेस दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी है, लेकिन पुडुचेरी के उसके मुख्यमंत्री ने जिस अंदाज़ में इस धरने का समर्थन किया था, उसने कांग्रेस को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी रणनीति पर नये सिरे से ़गौर करे। वी. नारायणस्वामी ने कहा था कि वे भी अपनी उप-राज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ केजरीवाल की तज़र् पर ही धरना देने के बारे में सोच रहे हैं। भारतीय राज्य संघवाद के उसूल को तो स्वीकारता है, लेकिन उनकी बुनियादी प्रवृत्ति केंद्रवाद की है। यानी संघवाद होते हुए भी केंद्रवाद उस पर हावी रहता है। इसकी सबसे ताकतवर अभिव्यक्ति इंदिरा गांधी के वर्चस्व के ज़माने में हुई थी, जब सभी तरह की क्षेत्रीय पार्टियों को राष्ट्र-विरोधी करार देने की राजनीति की गई थी। उस ज़माने में भाजपा ने आगे बढ़ कर क्षेत्रीय शक्तियों की मदद करने का बीड़ा उठाया था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी सरकारिया कमिशन की भाषा बोलते थे। लेकिन जैसे ही भाजपा को केन्द्र में पूर्ण बहुमत मिला, वह भी क्षेत्रीय शक्तियों को दरकिनार करने की राजनीति करने लगी। परिणाम यह निकला कि केन्द्र-राज्य संबंधों के मसले ने एन.आई.टी.आई. आयोग द्वारा संसाधनों को बांटने का सवाल तो उठाया ही, साथ में यह मसला इन सीमाओं को लांघ कर उसके परे राजनीतिक संघर्ष के मैदान में भी चला गया। दक्षिण भारत और पूर्वी भारत के राज्य अपनी ह़कतल़फी के खिलाफ बोलते रहे हैं, और बार-बार केंद्र सरकार को इस संबंध में सफाई देनी पड़ती है।
दिल्ली के ताज़ा घटनाक्रम ने इसके साथ एक नया पहलू जोड़ दिया है। नये उप-राज्यपाल का दावा है कि वह दिल्ली के ‘प्रशासक’ हैं और निर्वाचित सरकार और उनके बीच में अधिकारों के बंटवारे से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के अवलोकन भी उनकी निगाह में महज ‘सलाह’ की हैसियत रखते हैं, जिन्हें मानने के लिए वे मजबूर नहीं हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार और उप-राज्यपाल के बीच इस नये संघर्ष ने केंद्र-राज्य संबंधों के साथ ‘लोकतंत्र में जन-प्रतिनिधि की प्रभुसत्ता’ का मुद्दा भी जोड़ दिया है। ज़ाहिर है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना तकरीबन नामुमकिन है। अदालत ने भी घोषित कर दी है कि उप-राज्यपाल ‘दिल्ली के बॉस’ हैं (ठीक इसी तरह की हालत पुडुचेरी की है), लेकिन इसके बावजूद सवाल यह उठ गया है कि इन दोनों स्थितियों के बीच में चुने हुए प्रतिनिधि की हैसियत क्या है? क्या एक केन्द्र शासित प्रदेश का चुना गया मुख्यमंत्री केंद्र द्वारा नियुक्त उप-राज्यपाल के अधीन है। अगर कभी यह ‘अधीनस्थ मुख्यमंत्री’ अफसरशाही के साथ संघर्ष में फंस जाता है, तो लोकतंत्र के तकाज़े से किसका पक्ष लिया जाना चाहिए?
दिल्ली, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की इन घटनाओं से विपक्ष की भाजपा विरोधी एकता को एक नया रूप मिल सकता है, क्योंकि इसके कारण फेडरल फ्रंट की सम्भावनाएं एक बार फिर बन सकती हैं। दिल्ली और पुडुचेरी के उदाहरण बताती हैं कि संविधान के नाम पर केन्द्र सरकार किस तरह चुने हुए प्रतिनिधियों को हाशिये पर धकेल सकती है। सबकी निगाहें इस समय इन राज्यों पर हैं कि वहां मुख्यमंत्री, राज्यपालों और उप-राज्यपालों के बीच संबंध किस तरह के रहते है। अगर डी.एम.के. सरकार के दबाव के कारण राज्यपाल रवि को वापिस बुला लिया गया तो यह घटना संघवाद के संदर्भ में ‘गेमचेंजर’ (खेल बदलने वाली) साबित हो सकती है। लेकिन, इसकी संभवाना न के बराबर ही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दलों द्वारा एक मज़बूत फेडरल फ्रंट बनाने के अलावा कोई और चारा नहीं रह जाता।
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।