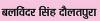भाजपा यानि उच्च् और कमज़ोर जातियों का गठबंधन
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल, 1980 को हुई थी। इमरजेंसी के बाद बनी जनता पार्टी में विलय करने वाले भारतीय जनसंघ ने जब फिर से अलग राजनीति करने का फैसला किया तो उसने न केवल अपना नाम बदला, बल्कि राजनीतिक रणनीति में भी परिवर्तन करके पहला कदम उठाया। इस लिहाज़ से यह एक ऐसी पार्टी थी जो नयी भी थी और पुरानी भी। नयी इसलिए कि उसने सीधे-सीधे हिंदुत्ववादी राजनीति करने के बजाय ़खुद को गांधीवादी समाजवाद का पैरोकार बताया। पुरानी इसलिए कि वह इसी के साथ-साथ जनसंघ के सांगठनिक पूर्वज दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रवर्तित ‘एकात्म मानववाद’ की थीसिस के साथ भी जुड़ी रही।
सावरकर के हिंदुत्व और जयप्रकाश नारायण के समाजवाद के बीच बनाया गया यह समीकरण परवान नहीं चढ़ा और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद चली हमदर्दी की लहर में हुए चुनाव में जनसंघ के इस नये संस्करण के परखचे उड़ गये। उसकी केवल दो सीटें रह गईं। बड़े-बड़े नेता चुनाव हार गए। पार्टी के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। क्या उस समय भाजपा का कोई नेता, उसके मुखिया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई पदाधिकारी या हिंदुत्व का कोई अन्य हमदर्द कभी सोच सकता था कि 39 साल बाद यही पार्टी अपना स्थापना दिवस एक ऐसी सत्तारूढ़ शक्ति के रूप में मनायेगी, जो न केवल पिछले 9 साल से बहुमत की सरकार चला रही है, बल्कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में भी उसके हारने का कोई अंदेशा नहीं है।
निश्चित रूप से दो सीटों से एक महाप्रबल पार्टी तक का सफर हर तरह से असाधारण ही कहा जाएगा। यह उपलब्धि कैसे हुई? कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे नरेन्द्र मोदी की करिश्माई श़िख्सयत की भूमिका है। कुछ लोग कहते हैं कि यह ़गैर-भाजपा दलों, ़खास तौर से कांग्रेस की विफलताओं का नतीजा है। कुछ लोग भाजपा का कामयाबी के पीछे एक विश्वव्यापी राजनीतिक प्रवृत्ति रेखांकित करते हैं। उनका कहना है कि सारी दुनिया में दक्षिणपंथी किरदार के आक्रामक और लोकलुभावन नेताओं का ज़माना चल रहा है। उदाहरण के रूप में अमरीका और तुर्की सहित कई नेताओं का नाम गिनाया जाता है। कुछ समीक्षक राम जन्म भूमि आंदोलन को भी भाजपा की सफलता के प्रमुख कारणों में से एक मानते हैं। ज़ाहिर है कि इन कारणों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता लेकिन मैं इन्हें भाजपा की सफलता के मुख्य कारण की हैसियत नहीं देना चाहता। मेरे विचार से यह पिछले साठ साल से एक ़खास तरह के सामाजिक समीकरण को साधने का संचित परिणाम है।
साठ के दशक में जनसंघ के मुख्य संगठनकर्ता दीनदयाल उपाध्याय ने द्विज जातियों (ब्राह्मण, ठाकुर और वैश्य) के साथ दो तरह के सामाजिक समुदायों को जोड़ने का योजनाबद्ध यत्न शुरू किया था। ये दो तरह के समुदाय थे शूद्रों (यानी पिछड़ी जातियों) के कुछ हिस्से और हिंदू समाज के वे हिस्से (जैसे, जाट, भूमिहार और कायस्थ) जो उच्च जातियां तो नहीं थे, लेकिन जिनकी आत्मछवि ऊंची जातियों वाली ही थी। यह हिंदू एकता बनाने का पहला चरण था। दूसरे चरण में यानी 1975 के बाद और विशेष तौर से अस्सी के दशक में संघ परिवार ने समाज के बेहद कमज़ोर हिस्सों को अपने साथ जोड़ने का उद्यम किया। उसने आदिवासियों में, दलित जातियों में और शहरी गरीबों में काम करना शुरू किया। यह इन कोशिशों का परिणाम ही है कि आज भाजपा को अपने प्रभाव क्षेत्रों में 45 से 50 प्रतिशत हिंदुओं के वोट मिलते हैं। चुनाव-दर-चुनाव उसकी जीत का सबसे बड़ा कारण यही है।
इसके पीछे जो विचारधारात्मक तर्क है वह बेहद सरल और व्यावहारिक किस्म का है। संघ परिवार ने इसे दो चरणों में पूरा किया। पहले उसने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में वर्णित विराट पुरुष के अंगों और उनके पूर्व-निर्धारित कर्तव्यों की व्याख्या ़खास तरीके की। इसके ज़रिये संघ ने लगातार यह दिखाने की कोशिश की कि शूद्र समाज को अन्य वर्णों से कम नहीं समझा जाना चाहिए। हिंदू-राष्ट्र की स्थापना के प्रोजेक्ट में पिछले 99 साल से लगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पुरुष वाले भाग में अक्सर ‘ऑर्गनिक यूनिटी’ या समाज की ‘आंगिक एकता’ की दावेदारी करता रहा। इसका एक नमूना जनसंघ के नेता दीनदयाल उपाध्याय के शब्दों में देखा जा सकता है : ‘चार जातियों के हमारे विचार में, उन्हें विराट पुरुष के चार अंगों के रूप में माना गया है। माना जाता है कि विराट पुरुष के सिर से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शुद्रों का उत्पत्ति हुई। जब हम इस विचार का विश्लेषण करते हैं तो हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या विराट पुरुष के सिर, हाथ, पेट, और पैरों के बीच के कोई संघर्ष खड़ा हो सकता है। अगर संघर्ष मूलभूत है तो शरीर काम ही नहीं कर पाएगा। एक ही शरीर के विभिन्न हिस्सों के बीच कोई संघर्ष हो ही नहीं सकता। इसके विपरीत ‘एक व्यक्ति’ प्रबल होता है। ये अंग एक दूसरे के पूरक ही नहीं हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा ये स्वतंत्र इकाई हैं। वहां पूरी तरह से प्यार और निकटता का भाव है। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति ऊपर बताए आधार पर ही हुई। अगर इस विचार को नहीं समझा गया तो जातियों में एक-दूसरे का पूरक बनने की बजाए संघर्ष पैदा होगा। लेकिन तब यह विकृति है। यह व्यवस्थित व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें कोई योजना या व्यवस्था नहीं है। सचमुच हमारे समाज की आज यही दशा है। ...परस्परानुकूलता और परावलम्बन वर्ण व्यवस्था का आंतरिक भाव है। सर्वसमभाव ही वर्ण व्यवस्था है।’
दिलचस्प बात यह है कि पहले तो संघ परिवार ने वर्णव्यवस्था को सर्वसमभाव के रूप में प्रदर्शित किया और फिर दूसरे चरण में 1974 में सरसंघचालक बालासाहब देवरस ने कह दिया कि, ‘वास्तव में देखा जाए तो आज की सम्पूर्ण परिस्थिति इतनी बदल चुकी है कि समाज धारण के लिए आवश्यक ऐसी जन्मत: वर्ण-व्यवस्था अथवा जाति-व्यवस्था आज अस्तित्व में ही नहीं है। सर्वत्र अव्यवस्था है, विकृति है। अब यह व्यवस्था केवल विवाह संबंधों तक ही सीमित रह गई है। इस व्यवस्था का उत्साह ही समाप्त हो गया है, केवल शब्द ही शेष रह गया है। भाव समाप्त हो गया, ढांचा रह गया। प्राण निकल गया, पिंजर रह गया। समाज धारण से उसका कोई संबंध नहीं है। अत: सभी को मिल कर सोचना चाहिए कि जिसका समाप्त होना उचित है, जो स्वयं ही समाप्त हो रहा है, वह ठीक ढंग से कैसे समाप्त हो।’ संघ को इस विचारधारात्मक रुझान पर पूरी भाजपा और पूरे संघ को लाने में क़ाफी समय लगा। इस रास्ते पर वह धीमीगति से चला, लेकिन चलता रहा। इसके ज़रिये संघ ने कमज़ोर जातियों के राजनीतिक तत्वों को यह भरोसा देने में कामयाबी हासिल की कि अगर वे हिंदुत्व की राजनीतिक परियोजना से जुड़ेंगे तो उन्हें दूसरों जितने मौके ही मिलेंगे। मेरे विचार से इस प्रोजेक्ट की कामयाबी ही भाजपा की असाधारण सफलता के मर्म में है।
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।