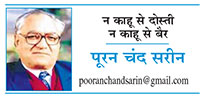शिक्षा, नौकरी व व्यवसाय - आज़ादी के बाद भी हर तरफ है भ्रष्टाचार का बोलबाला
जीवन के तीन पड़ाव हैं। सबसे पहले पढ़ाई लिखाई, फिर उसके बल पर मनचाही या जैसी तैसी नौकरी या कोई काम धंधा और फिर ऐसा समय जिसमें अब तक जो हुआ उसे याद करने, संस्मरण सुनते सुनाते प्रतीक्षा करते रहना कि कब परलोक सिधारने का समय आ जाये। यही हकीकत है।
योग्यता का पैमाना
इसे इस घटना से समझते हैं : देश के संस्थान एनईईटी अर्थात् विभिन्न व्यवसायों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सरकारी संस्थानों में प्रवेश की योग्यता सिद्ध करने वाला उपक्रम नीट। इसके अंतर्गत ठेका सिद्धांत के आधार पर एनटीए या राष्ट्रीय स्तर पर इच्छुक विद्यार्थियों की परीक्षा लेने वाली एजेंसी का गठन हुआ ताकि युवा वर्ग को इधर-उधर भटकना न पड़े और वे निश्चिंत होकर अपना निर्धारित लक्ष्य या सपना पूरा कर सकें।
चिकित्सा के क्षेत्र में जाने के लिए लालायित युवा वर्ग एक बहुत ही कड़े और पारदर्शी कहे जाने वाली परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। स्कूल में जो पढ़ा, वह नाकाफी होने से ऐसी दुकानों का खुलना अनिवार्य हो गया जहां सभी तरह के व्यवसायों की समझ दिलाने और फिर अगर कोई प्रतियोगिता होती है तो उसमें उत्तीर्ण होने की गारंटी दी जा सके। इनका पनपना निश्चित था क्योंकि सरकार की तरफ से कोई इंतज़ाम न था। ऐसे में उन लोगों की पौ बारह हो गई जिन्होंने अपनी घोंसलेनुमा दुकान या बेकार पड़ी बड़ी हवेली की काट छांट कर क्लास रूम, हॉस्टल में परिवर्तित कर उसके आंगन में सोना चांदी बरसने का प्रबंध कर लिया। वहां काल्पनिक योग्यता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति हुई जिन्हें लक्ष्य दिया गया कि चाहे जो कुछ करना पड़े, उनके यहां पढ़ने वाले केवल पास ही नहीं बल्कि मेरिट हासिल करें ताकि उनका दाखिला बड़े और प्रतिष्ठित संस्थानों में संभव हो जाये।
यदि विद्यार्थी इस योग्य है कि मार्गदर्शन से सही दिशा तक पहुंच सकता है तो इन्हें पढ़ाने वालों को अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे उपाय अपनाये जाते हैं कि काबिलियत को भाड़ झोंकना पड़ जाये और पैसे के बल पर प्रथम आने वालों की भीड़ लग जाये। इनके लिए परीक्षा केन्द्र पर सांठ-गांठ हो जाती है, प्रश्न पत्र लीक कर रटवाने और नकल करने की सुविधा अतिरिक्त चार्ज पर उपलब्ध कर दी जाती है। जो अपनी दिन रात की मेहनत और परिवार को आर्थिक रूप से कंगाल तक कर देने के बल पर इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने का सपना देखते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। लाखों युवाओं को निराशा, अवसाद और मानसिक तनाव के दौर से गुज़रना पड़ता है। कोचिंग इतनी महंगी कि माता-पिता से एक और चांस लेने की बात कह नहीं पाते और जो भी रोज़गार मिल जाये, उसकी कोशिश में लग जाते हैं।
इस बात में संदेह नहीं है कि इन सब विकट परिस्थितियों के होते हुए भी कुछ प्रतिभाशाली अपना मनचाहा कोर्स करने में सफल हो जाते हैं। विडम्बना यह है कि उन्हें उनसे कम्पटीशन करने के लिए विवश होना पड़ता है जो धन, बल और सिफारिश के दम पर इन स्थानों में उनसे आगे बैठे होते हैं। ये सब मुन्नाभाई हर जगह सफल होते रहते हैं और वे सब पद पा लेते हैं जिन पर किसी दूसरे का अधिकार था। उल्लेखनीय यह है कि यह परम्परा आज़ादी के बाद से अब तक अनवरत चल रही है। इसे तोड़ना या बदलना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हमारी राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक सोच ऐसी है कि यदि थोड़ी-सी पहुंच, खानदानी रुतबे और पैसा फेंक कर तमाशा देखने को मिल जाये तो इसमें बुराई क्या है?
यह अन्याय ही है।
चलिए एक व्यक्तिगत संस्मरण का ज़िक्र किया जाये। किस्सा यह है कि साठ के दशक में आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो ने तय किया कि युव वाणी के नाम से एक नया चैनल शुरू किया जाये। अपने पर भरोसा था, आवेदन कर दिया। इंटरव्यू आदि की औपचारिकताएं पूरी हुईं और मौखिक संदेश मिल गया कि प्रोड्यूसर के रूप में चयन हो गया है। चयनकर्ताओं में साहित्य अकादमी के मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर प्रभाकर माचवे जैसे व्यक्तित्व थे और सब कुछ सही ढंग से हुआ था। उन्होंने ही बाहर निकलते समय सूचित कर दिया था कि नियुक्ति पत्र मिल जायेगा।
अब हुआ यह कि जब काफी समय तक कोई सूचना नहीं मिली तो आकाशवाणी कार्यालय जाकर पता किया और यह जानकारी मिली कि एक सातवें नम्बर पर आई महिला का चयन हो गया है और उन्हें नियुक्ति पत्र भेज दिया गया है। जब पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ तो बताया गया कि यह एक केन्द्रीय मंत्री के आदेश पर हुआ है। अपनी किस्मत को कोसने और वापिस मुंह लटका कर लौटने के अतिरिक्त कुछ किया भी क्या जा सकता था? इस प्रकार का घटनाएं कई बार हुईं और पाठकों को भी उनके साथ इस तरह की गई कोई न कोई ज़्यादती यह पढ़ते हुए अवश्य ही दिमाग में कौंध रही होगी। बात यह नहीं है कि तब यह सब क्यों होता था बल्कि यक्ष प्रश्न यह है कि आज़ाद होने के इतने वर्ष बीत जाने पर भी सिस्टम वैसा ही है, उसका रूप आज चाहे कम्प्यूटर और आधुनिक टेक्नोलॉजी ने लिया हो!
शिक्षा के क्षेत्र में चाहे व्यापम घोटाला हो या आज का चिकित्सा संस्थानों में दाखिले के लिए किए गए पेपर लीक, ग्रेस अंक देने और करोड़ों रुपये के लेन-देन की पृष्ठभूमि हो, कुछ नहीं बदला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी कितनी अहमियत रखते हैं, किसी से छिपा नहीं है। उन्हें अपने स्वार्थ के अनुसार तोड़ने-मरोड़ने वालों की कमी नहीं है। इसी के साथ ऐसे युवाओं की भी संख्या कम नहीं होने वाली जो यहां की प्रणाली से भरोसा उठ जाने के कारण किसी भी तरह से विदेश जाकर पढ़ने और फिर कभी न लौटकर आने के संकल्प की दृढ़ता पर विश्वास करने लगते हैं। जहां तक ग्रेस आंकों की बात थी, उसका बहुत आसान हल यह था कि जितना समय किसी सेंटर पर व्यर्थ गया, उसकी भरपाई अतिरिक्त समय देकर कर ली जाती, लेकिन खेल तो यह था ही नहीं, वह तो सैंकड़ों करोड़ की कमाई का था और शायद इसका कभी खुलासा ही न हो।
अंतिम दिनों की याद में
15 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अनुमोदित बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार न हो, इसके लिए कुछ वर्ष पहले इसे इस तरह मनाने की परम्परा शुरू हुई थी, जिसमें साल में एक दिन अपने बड़े-बूढ़ों के लिए यह सोचने का हो कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार या लापरवाही तो नहीं हो रही है?
विकसित और अमीर देशों तथा उनकी पारम्परिक सभ्यताओं में यह व्यवस्था हो गई है कि एक उम्र के बाद लोग अपनी इच्छा और हैसियत के अनुसार अपना शेष जीवन जी सकते हैं। हमारे जैसे विकासशील और गरीबी की मार झेल रहे अधिकतर नागरिकों वाले देशों में यह एक कल्पना ही है कि यह पीढ़ी सुकून से रह सके। जिनकी हैसियत है, जमा पूंजी का सहारा है, इतने भाग्यशाली हैं कि उनके हाथों में पली बढ़ी युवा या अधेड़ पीढ़ी उनका यथासंभव ध्यान रखती हो। अधिकतर जनसंख्या ऐसे व्यक्तियों की है जो एकाकी जीवन जी रहे हैं, अकेलेपन के शिकार हैं, अनेक बीमारियों से ग्रस्त है, कोई देखभाल करने वाला नहीं है, धार्मिक और परोपकारी व्यक्तियों के आर्थिक सहयोग से चल रही संस्थाओं में जीवन काट रहे हैं और जैसे-तैसे अंतिम क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
सरकारी स्तर पर हो या सामाजिक दायरे में रह कर की जाने वाली सहायता हो अथवा परिवार में रख कर की जाने वाली सेवा हो, अधिकतर भाव यह रहता है कि यह वह पीढ़ी है जिसकी चाहे कितनी भी उपलब्धियां रही हों, हम पर एक बोझ है। हमारा सहारा न हो, दया न दिखाएं, अपनी सुविधाओं में से कटौती कर इनका भरण पोषण न करें तो इन्हें एक दिन भी जीने का अधिकार नहीं है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि जब जीवन एक भार जैसा लगने लगे, किसी की मेहरबानी पर जीने की मजबूरी न हो, अपने सुख-दुख और ज़िन्दगी की ज़रूरतों के बारे में सोचने की चिंता न हो और जब चिर विश्राम का समय आये तो शांति से आंखें मूंद ली जायें।