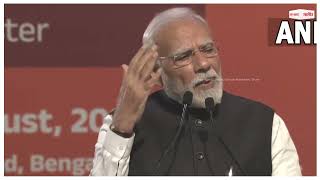उत्तराखंड में क्यों घटित होता है प्रकृति का कहर
धराली क्षेत्र को ‘गंगा के मायके’ कहा जाता है क्योंकि गौ-मुख जहां से गंगा शुरू होती है, के साथ ही, गंगोत्री मंदिर के सर्दियों में बंद होने के उपरांत गंगा जी की प्राचीन मूर्ति को धराली गांव के बसीमे के गांव मुखबा में स्थापित कर दिया जाता है परन्तु धराली ठहरने-रहने के लिए अधिक सुखद और अलौकिक है। नि:संदेह मुखबा की बजाय धराली अधिक प्रसिद्ध है। धराली, उत्तराखंड के उत्तरकाशी ज़िले में स्थित है जो देहरादून-गंगोत्री मार्ग तथा देहरादून से 28 कि.मी. दूर, गंगोत्री से 13 कि.मी. के पास और इसी मार्ग पर पड़ती हर्षिल छावनी से 8 कि.मी. आगे है। गंगोत्री जाते हुए यह विशेष ठहराव, अर्थात यात्री-पड़ाव है। यह सुविधाओंठहराव, बड़े होटलों, रैस्टोरेंट और होम-स्टेयज़र् के साथ प्रसिद्ध पर्यटक केन्द्र के तौर पर स्थापित हो चुका है। निष्कर्ष के तौर पर स्थानीय निवासियों और सरकार को इसने यथायोग्य दौलत से नवाज़ा है, परन्तु कई धन कुबेरों के कारण लोगों को अकसर त्रासदी की कीमत चुकानी पड़ती है, जो धराली को भी चुकानी पड़ी है।
विगत दिवस इसी धराली के साथ बहुत बुरा हुआ। हुआ यह कि ‘सुक्खी टॉप’ और ‘खीर गंगा केचमैंट’ के पुरातन ‘कलपा मंदिर’ में बादल फटने से कुछ सैकेंड में ही उस मंदिर सहित इस खूबसूरत नगर का बहुत हिस्सा मलबे के अंबार तले दब गया। जानी-माली नुकसान सहित इमारतें, वास्तव में जिनमें से बहुत सी मुख्य जल धारा के पाट में घुस या तीखे मोड़ों के साथ बनाई गुई थीं, ताश के पत्तों की तरह गिर गईं। अफसोस! दूर पड़ते महाराष्ट्र या वायनाड (केरल) की तो बात ही छोड़ो। इसी उत्तराखंड में वर्ष 2013 के, निकटतम जोशीमठ (केदारनाथ) में बादल फटने से हुई त्रासदी और 2021 में चमोली ग्लेशियर के यकदम-पघलाव के उपरांत हुई घटना से किसी ने कोई सबक नहीं लिया, खासतौर पर निजाम ने।
बादलों का फटना प्राकृतिक क्रिया-प्रक्रिया है। पहले समय में यह एक आम और सीमित क्रिया थी। जान-माल का नुकसान भी कम था। इससे यह भाव न लिया जाए कि तब भगवान हम पर अधिक दयालू थे। हमें बादल फटने की परिभाषा और इसकी क्रिया-प्रक्रिया के बारे में नहीं पता था। दो शब्दों की वैज्ञानिक भाषा में इसको ’बारिश के बादलों की आकाशीय उड़ान (एरोग्राफिक लिफ्ट) के तहत बहुत ही कम समय में बारिश के पानी से भरे बादलों का सीमित क्षेत्र पर एकदम खुल जाना और अधिक नुकसान कर जाने की क्रिया’ कहा जाता है। बारिश के मौसम में अकसर बादल गर्मी के कारण ज्यादा ऊपर उठ जाते हैं और ठंडक से यह बेहद घने और वेगमयी हो जाते हैं जिनको हम ‘आकाशी दरिया’ कहते हैं। इनके बीच जल बिन्दुओं का आकार भी न सिर्फ मोटा और भारी, करीब 25 एम.एम. गोलाई का हो जाता है, बल्कि बादलों की चाल भी भटक जाती है। परिणाम यह कि वे डगमगा कर फट कर गिर जाते हैं। इस स्थिति में एक सीमित क्षेत्र में यह आकाशीय दरिया पानी की धरालों, अमूमन 25000 मीट्रिक टन प्रति वर्ग किलोमीटर फैंक देता है। धराली का तो अभी पता नहीं परन्तु पहले भी ऐसी भीषण वर्षा की बेहद उच्च गति 100 एम.एम. (4 ईंच) प्रति सैकेंड थी, जिसने डरावने जल प्रलय बना दिए।
जल प्रलय का एक बड़ा कारण है ‘ग्लोबल वार्मिंग’। वैज्ञानिकों के मुताबिक,‘अधिक तपिश के कारण बे-जोड़ जल वाष्प हो रहा है, जिसके फलस्वरूप उच्च खलाव में उड़ते दरियाओं का सृजन हो रहा है, जो बादलों की तरह आंखों से नहीं दिखते। मौका-मेल के साथ वे इस ज़मीन पर अनिश्चित पानी फैंकते हैं। पहले मानसूनी बादलों के फटने की घटनाएं सिर्फ ऊंचे पहाड़ों में ही होती थीं, अब यह घटनाएं कहीं भी हो जाती हैं। मानसून के दौरान भारतीय उप-महाद्वीप में ऐसा होना भी शुरू हो गया है। निचले पहाड़ों पर भी हमारी, खासतौर पर निजाम हेतु धन कुबेरों की दखलअंदाजी के कारण बड़े हादसे होने लगे हैं।
पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में प्रकृति से तालमेल बिठाए बिना किए गए विकास की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विगत डेढ़ दशक में अधिकतर वोट राजनीति के तहत, उत्तराखंड में तीस हज़ार मील चार मार्गीय सड़कें बनाई गईं। पहाड़ों को धराशायी करते हुए करीब दो अरब घन मीटर मलबा खड्डों में धकेल दिया गया, जिसने जल बहाव को रोक दिया। बाद में यह गार बनकर बहने लगी। इस राज्य की पांच ज़िलों को जोड़ती चारधाम 100 मील लम्बी रेल लाईन पर कई विराट पुल और सुरंगें बनेंगी, मलबे को कहां रखना है और प्रकृति को कैसे दोबारा बहाल करना है, किसी ने सोचा भी नहीं। इस जल्दबाज़ी में लगभग 60,000 वृक्ष काटे जा चुके हैं, बाकियों की बारी अभी आनी है।
पहाड़ों में 50 प्रतिशत हिस्से के हिसाब के साथ वृक्ष न लगे हों तो बारिश पहाड़ों-मैदानों की मिट्टी को खोखला करती है। प्रत्येक वर्ष 6 करोड़ टन मिट्टी जल कुंडों को जा रही है। जब पानी ढलान से नीचे उतरता है, वहां या तो धरती नंगी हो या सामने रुकावटें न हों तो गति हज़ारों टन मलबा भी ले आती है। खोखली और ढलान वाली ज़मीन पर पानी की गति चार गुणा बढ़ जाती है और वज़न उठाने की समर्था 32 और धक्का देने की शक्ति 64 गुणा बढ़कर जल प्रलय का रूप धारण कर सब कुछ दबाकर और बहाकर ले जाती है। तीन गुणा जल गति की सीधी कटाई या ढलान पर बहाने की ताकत 729 गुणा हो जाती है। निष्कर्ष के तौर पर पहाड़ खिसकते और बह जाते हैं। अब भूमि और जंगलों-पहाड़ों का उपयोग उसकी योग्यता और प्रकृति स्रोतों के मद्देनज़र नहीं हो रहा, जिस कारण ऋतुओं का बिगड़ना, बादलों का फटना, मरुस्थलीकरण, जल संकट और जल प्रलय बढ़ रहे हैं।
बादल फटने की घटनाओं में वृद्धि, ग्लेशियरों का पिघलना आदि सब नाकारात्मक तबदीलियों में वृद्धि इस प्रकृति विरोधी मुनाफाखोरी ढांचे का परिणाम है। धराली का दु:खांत अंधाधुंध बनाए जा रहे पुलों, सुरंगों, होटलों द्वारा विकास माडलों को कटघरे में खड़ा करता है। उत्तराखंड में पिछले वर्ष में पर्यटन और धार्मिक प्रपंचों की भीड़ में बड़ी वृद्धि हुई है। ‘चार धाम प्रोजैक्ट’ के तहत बनाए जा रहे सड़कों, सुरंगों और निर्माणों ने इस क्षेत्र की खूबसूरत प्रकृति को नज़र लगा दी है। लोगों और प्रकृति विरोधी यह विकास माडल पूरी हिमालय पट्टी में दोहराया जा रहा है, जिसने कुदरती स्रोतों को बिगाड़ कर रख दिया है। निष्कर्म के तौर पर मनुष्य खुद रगड़ा जा रहा है। धन-कुबेरों का यह पक्ष विकास माडल नहीं, विनाश माडल बन रहा है। धराली जैसी त्रासदी इसका घिनौना रूप है।
मो. 94634-39075