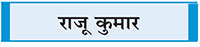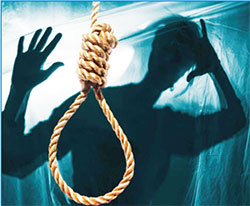चिन्ताजनक हैं देश में आत्महत्या के आंकड़े
भारत में आत्महत्या एक गंभीर सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य संकट बन चुकी है। आत्महत्या के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक जैसे राज्यों से हैं। दक्षिण भारत के राज्यों में विशेष रूप से आत्महत्या दर अधिक है जबकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में भी यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। आत्महत्या के कारण बहुस्तरीय और जटिल हैं।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में कुल 1,70,924 आत्महत्या के मामले दर्ज किए गए जो 2021 की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक थे। हर दिन औसतन 467 लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आत्महत्या दर (प्रति एक लाख जनसंख्या पर) 12.4 है, जो अब तक की सबसे उच्चदर है। एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार पारिवारिक समस्याएं और बीमारियां प्रमुख कारणों में हैं जो सभी आत्महत्याओं का लगभग 66 फीसदी हैं। बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, व्यावसायिक हानि परीक्षा में असफलता, प्रेम प्रसंग की असफलता और मादक पदार्थों का सेवन भी मुख्य कारण रहे हैं। भारत में किसानों और छात्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि कैसे सामाजिक दबाव और संस्थागत समर्थन की कमी कई ज़िंदगियों को असमय समाप्त कर रही है।
वैश्विक परिप्रेक्ष्य में भारत आत्महत्या के वैश्विक आंकड़ों में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार विश्व की लगभग 17 फीसदी जनसंख्या भारत में है, लेकिन आत्महत्या के मामलों में यह आंकड़ा लगभग 36 फीसदी है। आत्महत्या करने वालों में किशोर, युवा, महिलाएं, किसान और मजदूर प्रमुख समूहों के रूप में सामने आते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि आत्महत्या को रोकने के लिए सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि व्यापक सामाजिक ढांचे में सुधार की आवश्यकता है।
भारत में सामाजिक कारकों का आत्महत्या दर पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जातिगत भेदभाव, जेंडर असमानता, आर्थिक विषमता और तेज़ी से होते शहरीकरण के चलते बढ़ते अकेलेपन ने स्थिति को जटिल बना दिया है। पारंपरिक सामाजिक ढांचे के टूटने से समुदाय आधारित समर्थन तंत्र भी कमज़ोर हुआ है। सामाजिक कारणों से लोग मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में खुलकर बात करने से हिचकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की भारी कमी, विशेषकर ग्रामीण भारत में स्थिति को और जटिल बनाती है। भारत में प्रति एक लाख जनसंख्या पर मनोचिकित्सकों की संख्या केवल 0.75 है, जबकि डब्ल्यूएचओ न्यूनतम 3 मनोचिकित्सक प्रति एक लाख की सिफारिश करता है। यह असमानता बताती है कि अधिकांश लोग या तो इलाज तक पहुंच ही नहीं पाते या फिर असंगठितऔर अविश्वसनीय स्रोतों का सहारा लेते हैं।
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आत्महत्या अक्सर मानसिक स्वास्थ्य विकारों जैसे—अवसाद, चिंता विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर और मादक पदार्थों की लत से जुड़ी होती है। हालांकिए यह भी स्पष्ट है कि अकेले मानसिक रोग ही कारण नहीं हैं, सामाजिक असहायता, भावनात्मक अलगाव, असफलता का भय और निरंतर तनाव भी बड़े कारक हैं। अमरीकी मनोवैज्ञानिक संघ (एपीए) के अनुसार सामाजिक समर्थन की कमी, जीवन में उद्देश्य का अभाव और सामाजिक अस्वीकार्यता आत्महत्या के जोखिम को कई गुना बढ़ा देते हैं। भारत में अभी भी मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सामाजिक भ्रांतियां हैं, जिससे लोग सहायता मांगने में संकोच करते हैं और संकट की स्थिति में खुद को अकेला पाते हैं।
नीति और कार्यक्रम स्तर परए पिछले वर्षों में आत्महत्या रोकथाम के लिए कई प्रयास हुए हैं। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 के तहत आत्महत्या को अपराध से बाहर करना ‘किरण’ हेल्पलाइन जैसी सेवाओं की शुरुआत और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिला मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं का विस्तार उल्लेखनीय पहलें हैं। राष्ट्रीय स्तर पर ‘टेली-मानस’ कार्यक्रम के माध्यम से लोग टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर मुफ्त टेली-काउंसलिंग सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। आत्महत्या रोकथाम के लिए 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति भी लागू की गई।
राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति-2022 की अनुशंसाओं को आधार मानकर भोपाल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट सायकियाट्री (आईएपीपी) के तत्वावधान में दो दिवसीय मिड-टर्म सीएमई 2025 का आयोजन किया गया, जो आत्महत्या जैसी गंभीर समस्या की रोकथाम और मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर केन्द्रित था।
सीएमई के समापन के बाद आयोजन समिति के चेयरपर्सन वरिष्ठ मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. आर. एन. साहू ने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कार्यक्रम में आत्महत्या की सोच वाले लोगों के मस्तिष्क में होने वाले बदलावों और उनको समझने की तकनीकों पर चर्चा की गई।
आत्महत्या रोकने के लिए शिक्षा संस्थानों, कार्यस्थलों और समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर खुली बातचीत, समय पर काउंसलिंगए और मजबूत सामाजिक नेटवर्क की आवश्यकता है। भारत में आत्महत्या केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि सामाजिक विफलताओं का भी प्रतीक है। जब तक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और सम्मानजनक नहीं बनाया जाएगा, जब तक आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को गंभीरता से नहीं सुलझाया जाएगा, तब तक आत्महत्या के आंकड़ों में स्थायी गिरावट लाना कठिन रहेगा। ऐसी संरचनाएं बनाने की ज़रूरत है, जहां व्यक्ति बिना भय और शर्मिंदगी के अपनी पीड़ा साझा कर सके और उसे तत्काल एवं प्रभावी सहायता मिल सके। (संवाद)