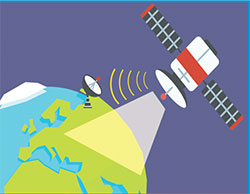भारतीय सेनाओं के लिए ज़रूरी है सैटेलाइट्स की स्टीक नज़र
कोई भी ज़ंजीर उतनी ही मज़बूत होती है जितनी कि खुद उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। इस तथ्य को पहलगाम घटना ने एक बार फिर याद दिलाया है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में। यह सही है कि जिस तरीके से पहलगाम में हमले को अंजाम दिया गया, उसकी पूर्व-सूचना शायद सैटेलाइट्स के माध्यम से प्रत्यक्ष तौर पर न मिल पाती, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे पहले जो कुछ भारतीय सीमा के निकट घटित हुआ (या हो रहा है) उसकी जानकारी तो सैटेलाइट के ज़रिये हासिल हो ही सकती थी? इसलिए सरकार को भारत की स्पेस-आधारित क्षमताओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले राष्ट्र के रूप में भारत ने निरन्तर स्पेस में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है व लोहा मनवाया है, जैसा कि 1975 में आर्यभट्ट की लॉन्चिंग से लेकर चंद्रयान-3 का चांद के दक्षिणी ध्रुव के विजयी स्पर्श से ज़ाहिर है। इसके बावजूद भारत को इस असहज सत्य का भी सामना करना चाहिए कि उसकी सैन्य स्पेस क्षमताएं अपर्याप्त हैं और वह भी ऐसे समय में जब स्पेस तेज़ी के साथ भू-राजनीतिक वर्चस्व का अगला जंगी मैदान बनता जा रहा है।
गौरतलब है कि साल 2020 में जब चीन ने पूर्वी लद्दाख में घुसपैठ की थी, तब भारत ने सबसे पहले स्पेस-बेस्ड सर्विलांस (एसबीएस) की कल्पना की थी। देर से पहल की गई इस दीर्घकालीन योजना का उद्देश्य भारत की स्ट्रेटेजिक स्थितिगत जागरूकता को सैटेलाइट्स के समर्पित तारामंडल से मज़बूत करना था ताकि सशस्त्र बलों को सीमाओं की निगरानी व चौकसी करने में मदद मिल सके। इसलिए ज़रूरी है कि इसरो व अन्य स्टेकहोल्डर्स एसबीएस कार्यक्रम को वरीयता दें, विशेषकर इसलिए कि भारत केवल 9 या 11 रक्षा सैटेलाइट्स ही ऑपरेट करता है, जबकि अमरीका व चीन के पास 240 से अधिक के बेड़े हैं और रूस के पास 100 से अधिक रक्षा सैटेलाइट्स हैं। यह अंतर केवल संख्या का ही नहीं है बल्कि यह स्ट्रेटेजिक क्षमता में बुनियादी फासला है, चूंकि जो चीन के पास है, वह पाकिस्तान को स्वत: ही मिल जाता है। मसलन, हाल ही में पाकिस्तान को चीन के बेईडोउ नेविगेशन सिस्टम का ग्राउंड स्टेशन मिला। कहने का अर्थ यह है कि पाकिस्तान को चीन की सैन्य स्पेस क्षमताएं प्राप्त हैं, जबकि भारत के सशस्त्र बलों के पास समर्पित सैटेलाइट्स सिस्टम का अभाव है। रिसेट-2बी व जीसेट-7 सीरीज़ जैसे प्लेटफॉर्म्स विकसित करने के बावजूद भारतीय सेना के पास समर्पित सैटेलाइट सिस्टम नहीं है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क में चिंताजनक कमज़ोरी प्रतीत होती है। अब नई दिल्ली को अपना एसबीएस नेटवर्क अपग्रेड कर लेना चाहिए।
हालांकि वरिष्ठ रक्षा योजनाकारों व राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने एसबीएस पहल का समर्थन किया है और भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को मंज़ूरी दे दी है 52 सैटेलाइट्स के साथ, जिसमें से 31 का निर्माण निजी उद्योग द्वारा होगा, लेकिन इन सैटेलाइट्स को वास्तव में ऑर्बिट में पहुंचाने के सिलसिले में मामूली-सी ठोस प्रगति हुई है। यह चिंताजनक है क्योंकि निशाने, कम्युनिकेशन, लोजिस्टिक्स व अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के लिए आधुनिक युद्ध स्पेस आधारित एसेट्स पर अत्यधिक निर्भर होता जा रहा है। ग्लोबल पावर्स के पास सैटेलाइट्स का विशाल तारामंडल है, जिससे वह आशंकित टकराव क्षेत्रों का रियल-टाइम कवरेज कर लेती हैं, लेकिन अपने सीमित इन्फ्रास्ट्रक्चर के कारण भारत को अंधीगलियों का भी सामना करना पड़ता है। भविष्य के टकराव में ‘देखने, समझने व प्रतिक्रिया’ की क्षमताओं में अंतर ही निर्णायक साबित होगा।
बजट आवंटन भी इतना ही चिंताजनक है। नासा का बजट 25 बिलियन डॉलर है, चीन का 18 बिलियन डॉलर और यूरोपीयन स्पेस एजेंसी का 7.7 बिलियन यूरो। इनके सामने भारत का 2 बिलियन डॉलर का स्पेस बजट बौना प्रतीत होता है। जहां तक रक्षा-स्पेस क्षमताओं की बात है तो 2024 में अकेले अमरीका स्पेस फोर्स का वार्षिक बजट 30 बिलियन डॉलर था और अनुमान यह है कि चीन अपनी सैन्य स्पेस क्षमताओं में लगभग 10 बिलियन डॉलर का निवेश करता है। इसके विपरीत भारत का खर्च विभिन्न एजेंसियों में विभाजित रहता है, जिससे फोकस्ड निवेश नहीं हो पाता, जोकि ज़रूरी है काउंटर स्पेस सिस्टम्स, एंटी-सैटेलाइट्स डिफेन्स और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध हथियार विकसित करने के लिए। इससे भी खराब बात यह है कि भारत अपनी आधी से अधिक अंतरिक्ष रक्षा-संबंधी ज़रूरतें आयात करता है। भारत का कमर्शियल स्पेस सेक्टर तो मज़बूत है और अनुमान यह है कि 2040 तक हमारी स्पेस अर्थव्यवस्था 44 बिलियन डॉलर तक पहुंच जायेगी, लेकिन अगर रक्षा ज़रूरतों की भरपाई नहीं होगी तो यह विकास अर्थहीन ही रहेगा। सबसे पहले तो भारत को विस्तृत राष्ट्रीय योजना के ज़रिये एसबीएस को वरीयता देनी चाहिए।
एसबीएस को वरीयता देने के लिए समन्वित कार्रवाई की ज़रूरत है। वर्तमान में रक्षा व्यवस्था और स्पेस उद्योग अलग अलग काम कर रहे हैं, जिससे विचारों व आवश्यकताओं को लेकर आपस में सीमित संपर्क होता है। संस्थागत डायलॉग की आवश्यकता है। दूसरा यह कि फ़िलहाल हमारा फोकस सैटेलाइट्स विकास के सिलसिले में सिविल एप्लीकेशन पर है, जिसमें सैन्य ज़रूरतों के डिज़ाइन को शामिल करना ज़रूरी है। इसका अर्थ है कि एडवांस्ड सेन्सर्स, सुरक्षित कम्युनिकेशन क्षमताओं, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम्स और सैटेलाइट्स को ऐसा बनाने पर निवेश करना है ताकि वह आशंकित काइनेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या साइबर हमलों से सुरक्षित रहें। भारत को देशज लांच क्षमताओं में तेज़ी लाने की भी ज़रूरत है। आधुनिक युद्ध की मांग यह है कि सैटेलाइट के खराब होते ही तुरंत उसकी जगह दूसरा लांच कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त भारत को अमरीका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया व जापान के साथ रक्षा स्पेस सेक्टर में स्ट्रेटेजिक भागीदारी करनी चाहिए। भारत ने 2019 में मिशन शक्ति (एंटी- सैटेलाइट्स मिशन) का प्रदर्शन किया था, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आज का दौर अपने जैसों के साथ मिलकर चलने का है।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर