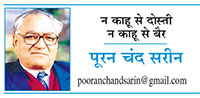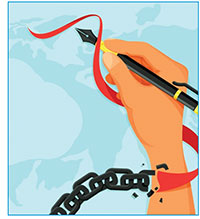स्वयं को शीशे में देखना ही महत्वपूर्ण होता है
आज के लिए विशेष
विश्व प्रैस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है। इसके अगले दिन 4 मई को इस बार विश्व हास्य दिवस भी संयोग से पड़ रहा है। यह दोनों ही लिखने से संबंधित हैं। दोनों में एक समानता है और वह यह कि दोनों ही कलम के ज़रिए लेखकों को सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी बंधनों से मुक्त करने की बात करते हैं।
प्रैस की आज़ादी का अर्थ यह लगाया जाता है कि समाचार पत्रों, जनसंपर्क के विभिन्न माध्यमों और मीडिया तथा मनोरंजन के साधनों के ज़रिए लोगों को पढ़ने, सुनने और देखने के लिए कुछ भी परोसा जा सकता है। जहां एक ओर निष्पक्ष पत्रकारिता किसी भी लोकतांत्रिक देश की पहचान है, वहीं अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी लिखने, सुनाने और दिखाने को अपना मौलिक अधिकार समझ लिया जाना गलत है। इससे न केवल भ्रम की स्थिति पैदा होती है बल्कि समाज में अव्यवस्था भी फैलती है जिससे लोगों के बीच तनाव उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है।
आलोचना और उसकी मर्यादा
सामान्य व्यक्ति के सामने आज चुनौती यह है कि वह किस की बात को सही माने—पत्रकारों, लेखकों और फिल्मकारों के विचारों पर या सरकार द्वारा रखा गया पक्ष जिसे बड़ी सफाई से संविधान और उसके अंतर्गत बने कानूनों के तहत सही ठहरा दिया जाता है। तर्क यह दिया जाता है कि जिस प्रकार कोई पत्रकार गहन खोजबीन करने के बाद ही किसी मामले पर कुछ लिखता है, उसी प्रकार सरकार भी तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखती है, कानून बनाती है और उन पर अमल करवाती है। प्रश्न यह नहीं कि कौन सही या गलत है, बल्कि यह कि यदि इन दोनों में कहीं मतभेद या अंतर है तो दोनों पक्षों द्वारा तार्किक बहस से सुलझाया जाना चाहिये जो सामान्यता होता नहीं, दोनों ही हठ पर उतर आते हैं कि वही ठीक हैं। सरकार के पास डंडा चलाने का अधिकार है तो वह व्यक्ति या संस्थान के प्रति कठोर कार्रवाई कर अपनी शक्ति दिखाती है तो दूसरी ओर मीडिया कर्मी भी पाठकों और दर्शकों तक अपनी व्यापक पहुंच के बल पर मोर्चा संभाल लेते हैं। यह सब देखकर आश्चर्य नहीं होता कि जिन विषयों पर गहन चर्चा होनी चाहिए, उन्हें उठाया ही नहीं जाता!
हमारा देश प्रेस की आज़ादी के मामले में 180 देशों की सूची में 159 के क्रम पर है। समझा जा सकता है कि हमारी स्थिति क्या है और यह भी कि इसके पीछे कौन ज़िम्मेदार है? हकीकत यह है कि यदि कोई व्यक्ति, संस्थान या संचार माध्यम अगर चाहे भी तो सत्य को बिना सरकार की अनुमति के उजागर नहीं कर सकता। किसी भी विषय को संवेदनशील कह कर उस पर कुछ भी बोलने से मना कर देना उचित नहीं कहा जा सकता। इससे सच्चाई का पता नहीं चल सकता। आप अंधेरे में रहते हैं और गलत नीति की बदौलत देश को नुकसान पहुंचाते हैं। आज भी संसार में अनेक देश हैं जहां आपातकाल जैसी स्थिति है। वहां कुछ भी प्रकाशित करने या दिखाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होती है। हमारे देश में ऐसी स्थिति तो नहीं है, लेकिन यह भय बना रहता है कि यदि सत्य होने के बावजूद और सभी प्रमाण होने पर भी कुछ लिखा या दिखाया गया तो जांच से पहले गिरफ्तारी की तलवार लटक सकती है।
वर्तमान चुनौतियां
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि एआई गलत जानकारी भी देता है, डीपफेक तकनीक से किसी के चरित्र का चीरहरण हो सकता है। यह इतना तेज़ है कि संभलने का मौका भी नहीं मिलता और दुनिया भर में गलत छवि फैल जाती है। इसके ज़रिए पत्रकारों की निगरानी करना आसान हो गया है, कुछ भी व्यक्तिगत या गोपनीय नहीं रहा। यह अलग तरह की हिंसा और उत्पीड़न है जिसका प्रतिकार करना मुश्किल है। राजनीतिक दबाव के कारण ऑनलाइन ट्रोलिंग का इस्तेमाल किया जाता है, पत्रकार को कमज़ोर करने के प्रयत्न किए जाते हैं। जिस स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को लोकतंत्र की आधारशिला माना जाता था वह ढांचा अब चकनाचूर होकर ढह गया है। सरकार आपराधिक तथा मानहानि जैसी धाराओं के तहत कार्रवाई करती है। राजद्रोह और यूएपीए के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप लगाकर वर्षों तक मुकद्दमे चलाए रख सकती है जिनका मकसद यही होता है कि विरोधी स्वर दबाए जा सकें
हमारे देश में एक समस्या यह है कि पत्रकारिता हो या फिल्मकारिता, व्यक्ति हो या संस्थान, वे ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत उदाहरण हैं जो पूंजीपतियों की जेब भरने का काम करते हैं। सरकार की नीतियों की अच्छाई और बुराई के आधार पर तर्कसहित आलोचना करने के स्थान पर कथित चाटुकारिता करते दिखाई देते हैं। क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर निकलने वाले अखबार और टीवी चैनलों के पास साधनों की कमी है, लेकिन केवल सरकार की कृपा पर ही टिके रहने को प्रैस की आज़ादी नहीं कहा जा सकता।
नई व्यवस्था बनाई जाए
प्रश्न यह है कि क्या सरकार और पूंजीपतियों तथा बुद्धिजीवियों के सम्मिलित प्रयास से कोई ऐसी व्यवस्था लागू की जा सकती है जिसके अंतर्गत वे सभी साधन उपलब्ध कराए जा सकते हों जिनकी आवश्यकता किसी समाचार पत्र या चैनल को होती है। इसके अतिरिक्त इस नई सोच में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। उसका नियंत्रण केवल आर्थिक मामलों पर होगा और शेष सभी निर्णय लेने में वह व्यक्ति या संस्था स्वतंत्र होंगे। इससे मुखौटा लगाकर पत्रकारिता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी या फिल्म के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को उठाने में आप निर्भय होकर अपनी बात कह सकेंगे और उस पर बहस भी कर पाएंगे। नई व्यवस्था हो उसमें सरकारी दवाब और सेंसरशिप का कोई स्थान न हो। ऐसे मानदण्ड बनाये जायें जिनका पालन अपनी इच्छा से करना संभव हो, किसी लालच या स्वार्थ की पूर्ति के लिए न हो। स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के व्यक्तियों ने औद्योगिक घरानों द्वारा संचालित संस्थानों से लेकर आपातकाल का दौर और उसके बाद तेज़ी से उभरा व्यक्तिगत छवि पर आधारित प्रकाशन और मीडिया, जो अब उद्योग बन चुका है, उसका निर्माण होते देखा है। यदि हमारा मीडिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा तो समाज में सहिष्णुता बढ़ेगी और लोगों को वास्तविक जानकारी मिलेगी। कानूनी शिकंजा एक हद तक तो ठीक है, लेकिन किसी को बिना किसी प्रमाण के राष्ट्रविरोधी कहना अन्याय है। ऐसे अनेक मामले हैं जिनमें किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाने के बाद मौन धारण कर लिया गया और उसका जीवन बर्बाद हो गया। उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं, यह उत्पीड़न है।
जिन देशों में सबसे अधिक प्रैस की आज़ादी है, वे लोकतांत्रिक रूप से मज़बूत हैं, उन्हें अपनी बात रखने की संवैधानिक सुरक्षा है। इसका कारण वहां पारदर्शिता का होना है। इसके साथ ही विश्व हास्य दिवस के अवसर पर मंद मंद मुस्कुराते हुए, चेहरे पर मुस्कान के साथ खुलकर हंसने-हंसाने और ठहाके लगाने की अग्रिम बधाई।