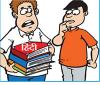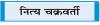जाति जनगणना से मुस्लिम जातियों की भी वास्तविक स्थिति पता चलेगी
भारत में धर्म अस्थायी है, जाति स्थायी है। व्यक्ति धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं बदल सकता। इसलिए जिन लोगों ने सिद्धांत: जातिवहीन समाज की कल्पना करने वाले इस्लाम को अपनाया, उनमें भी त्यागी, राजपूत, जाट, गुर्जर, दलित आदि जातियां हैं। हद तो यह है कि जातियों में भी उप-जातियां हैं। मसलन, अंसारी (जुलाहा) समुदाय में तीन उप-जातियां हैं- थमैती, पारवे और देसवाले। यह उप-जातियां आपस में रिश्ता नहीं रखती हैं। इनमें जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक व राजनीतिक असमानताएं हैं, वह जग जाहिर हैं। यह हाल मुस्लिमों की लगभग सभी जातियों का है। इसका अंदाज़ा सर्विदित है, लेकिन ठोस डाटा का अभाव है। इसलिए आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जो जाति जनगणना (मुस्लिमों की जातिगत जनगणना सहित) को शामिल किया गया है। इससे मुस्लिम जातियों की वास्तविक स्थिति भी मालूम हो जायेगी और डाटा की रोशनी में उनके विकास के लिए भी उचित कदम उठाये जा सकेंगे। हालांकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने मुस्लिमों की दयनीय स्थिति को उजागर कर दिया था, लेकिन उन्हें आरक्षण जैसी सुविधाओं से इसलिए वंचित रखा गया, क्योंकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान नहीं है। अनुमान यह है कि जनगणना से जब मुस्लिमों की जातिगत स्थिति सामने आ जायेगी तो उनकी कमज़ोर जातियों के विकास के लिए सरकारों की तरफ से कुछ कदम भी ज़रूर उठाये जायेंगे।
बहरहाल, मुस्लिमों में जो सम्पन्न अशरफ जातियां (सैयद, शेख, मुग़ल, पठान आदि) हैं, वह अब भी ख्वाब की दुनिया में ही रहना चाहती हैं या अपने राजनीतिक वर्चस्व को खोना नहीं चाहतीं। उनकी तरफ से यह मुहिम चलायी जा रही है कि जनगणना में धर्म इस्लाम व जाति मुस्लिम लिखवायी जाये। मुस्लिम कोई जाति नहीं है। जो भी इस्लाम को मानता है, वह मुस्लिम है। भारतीय उप-महाद्वीप के मुस्लिमों में जातियों का होना एक सामाजिक सच्चाई है, जिस पर अनेक शोध हो चुके हैं, विशेषकर जेएनयू के शोधकर्ताओं द्वारा।
दरअसल, समाजशास्त्रियों के अनुसार भारत के हिन्दुओं व मुस्लिमों में 97.5 प्रतिशत समानताएं हैं। इसलिए यह सोचना ही व्यर्थ है कि उनके व्यवहार या किसी भी मुद्दे पर प्रतिक्रिया में कोई खास अंतर होगा। अगर हम चाहते हैं कि कल को जाति का महत्व कम हो जाये तो हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आज भी जाति का महत्व क्या है? इसके लिए जनगणना आवश्यक होने के बावजूद पर्याप्त नहीं है। केवल गहरे सैंपल सर्वे ही विस्तृत डायग्नोसिस प्रदान कर सकते हैं। हां, इस बात से इन्कार नहीं है कि जाति जनगणना साक्ष्य-आधारित, समावेशी प्रशासन की ओर परिवर्तनकारी कदम हो सकती है. अगर उसे ध्यानपूर्वक, स्पष्टता व उद्देश्य के साथ लागू किया जाये। दशकों से हम जाति को अनदेखा करते हुए विकास कर रहे हैं। हमने जीडीपी विकास, डिजिटाइजेशन व वैश्विक प्रतिस्पर्धा का तो पीछा किया, लेकिन जाति को अक्सर अनदेखा किया, जबकि जाति एक ऐसी संरचना है जो शिक्षा, रोज़गार, हेल्थ केयर, हाउसिंग व न्याय को आकार दे रही है।
अनदेखा करने की इस प्रवृत्ति ने एक विरोधाभास उत्पन्न कर दिया है। हम आरक्षण नीतियों पर बहस करते हैं बिना यह जाने कि वास्तविक नुकसान का वितरण कहां है और गहरे विभाजित समाज में जाति-तटस्थ नीतियां लागू करने का प्रयास करते हैं। अच्छे उद्देश्य वाली नीतियां भी अक्सर निशाने पर नहीं लगतीं, क्योंकि सूचना का आधार अधूरा होता है। जाति जनगणना इसे सुधारने का अवसर प्रदान करती है। इससे न सिर्फ यह मालूम होगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, बल्कि यह भी जानकारी मिलेगी कि वह किन आर्थिक व सामाजिक स्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रही है। यह पहचान स्थापित करना नहीं है बल्कि संरचनात्मक असमानताओं को पहचानना है। कल का जातिवहीन समाज निर्मित करने के लिए आज जो जाति की हकीकत है, उसे समझना ज़रूरी है। लेकिन साथ ही यह समझना भी आवश्यक है कि जनगणना वैज्ञानिक सैंपल सर्वे का विकल्प नहीं है। जनगणना से दायरा मिलता है, गहराई नहीं। जनगणना की भूमिका विविधता का बुनियादी नक्शा प्रदान करने के संदर्भ में है, विस्तृत डायग्नोसिस देने के सिलसिले में नहीं। इससे वह प्रश्न प्रासंगिक हो जाते हैं जो सामाजिक व आर्थिक हकीकत की तस्वीर दिखाते हैं, जैसे शिक्षा, रोज़गार, एसेट कितने हैं और बुनियादी सेवाओं तक कितनी पहुंच है।
यह डाटा जब एकत्र हो जाये तब गहरे, आवश्यकता-आधारित अध्ययनों की ज़रुरत होगी। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या स्वतंत्र शोध संस्थाओं द्वारा फोकस सर्वे कराने होंगे ताकि क्षेत्रीय, समुदाय-विशिष्ट आदि असमानताएं मालूम हो सकें। इस किस्म के डाटा से ही सही जाति-आधारित कल्याणकारी योजनाएं और आरक्षण नीतियां बन सकती हैं। -इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर