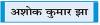वंचित लोगों तक पहुंचना चाहिए आरक्षण का लाभ
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई का यह विचार कि सम्पन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करना चाहिए, भारत में सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यह विचार आरक्षण नीति को और समावेशी और प्रभावी बनाने की और सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। हालांकि इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हैं, जिनमें सामाजिक भेदभाव की निरन्तरता, संवैधानिक प्रावधानों का पालन और प्रशासनिक जटिलताएं शामिल हैं।
भारत में आरक्षण नीति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को समान अवसर प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन रही है। यह नीति संविधान के तहत अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए विशेष प्रावधानों के माध्यम से लागू की गई है। हालांकि समय के साथ आरक्षण के दुरुपयोग, इसके लाभ के असमान वितरण और सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों ने इस नीति की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता पर सवाल उठाए हैं। इस संदर्भ में मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई का यह विचार कि ‘सम्पन्न लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर करना चाहिए’ एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दा बन कर उभरा है। बी.आर. गवई ने 14 मई, 2025 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की थी। गवई ने अनेक अवसरों पर आरक्षण नीति में सुधार की वकालत की है। उनका मानना है कि आरक्षण का लाभ उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं। उन्होंने क्रीमी लेयर (सम्पन्न वर्ग) की अवधारणा को अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी लागू करने की सिफारिश की है, जैसा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए पहले से लागू है। उनका तर्क है कि जब कोई व्यक्ति या उसका परिवार आरक्षण के माध्यम से उच्च पदों, जैसे कि आईएएस, आईपीएस या अन्य प्रतिष्ठित सेवाओं में पहुंच जाता है तो उनकी अगली पीढ़ी को सामाजिक और आर्थिक असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ता। ऐसे में उन्हें आरक्षण का लाभ देना नीति के मूल उद्देश्य को कमज़ोर करता है।
मुख्य न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी की थी, ‘जो वर्गीकरण का विरोध कर रहे हैं, वह उस मुसाफिर की तरह है, जो रेल के डिब्बे में घुस जाता है, फिर दूसरों को डिब्बे में आने से रोकता है।’ यह कथन उनके इस विश्वास को दर्शाता है कि सम्पन्न दलित या अन्य आरक्षित वर्ग के लोग जो पहले ही आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं, अब वंचितों के हक को छीन रहे हैं। क्रीमी लेयर की अवधारणा पहली बार 1992 में इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेश की गई थी। इस फैसले में कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण में क्रीमी लेयर को बाहर करने का प्रावधान किया, ताकि आरक्षण का लाभ केवल उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। क्रीमी लेयर की पहचान आय, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति जैसे मापदंडों के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए उच्च आय वाले परिवार, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के बच्चे या पेशेवर डिग्री धारक क्रीमी लेयर के अंतर्गत आ सकते हैं।
हालांकि यह अवधारणा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लागू नहीं की गई थी क्योंकि इन समुदायों को ऐतिहासिक रूप से गहरे सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा है, लेकिन बी.आर. गवई सहित कई विशेषज्ञों का मानना है कि समय के साथ इन समुदायों में भी आर्थिक और सामाजिक असमानता उभरी है। कुछ परिवारों ने आरक्षण के माध्यम से उच्च सामाजिक-आर्थिक स्थिति प्राप्त कर ली है जबकि अन्य अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ऐसे में क्रीमी लेयर की अवधारणा को एससी/एसटी के लिए लागू करना सामाजिक न्याय को और समावेशी बना सकता है।
आरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों को मुख्यधारा में लाना था। सम्पन्न लोग जो पहले ही उच्च शिक्षा, नौकरी या सम्पत्ति प्राप्त कर चुके हैं, इस नीति के मूल लक्ष्य से बाहर हो जाते हैं। उन्हें आरक्षण का लाभ देना संसाधनों का दुरुपयोग है। क्रीमी लेयर को बाहर करने से आरक्षण का लाभ उन तक पहुंचेगा जो अभी भी सामाजिक भेदभाव और आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। इससे समुदाय के भीतर असमानता कम होगी। मुख्य न्यायाधीश का तर्क है कि सम्पन्न लोग जो पहले ही समाज में उच्च स्थान प्राप्त कर चुके हैं, नैतिक रूप से उन लोगों के हक पर दावा नहीं कर सकते जो अभी भी वंचित हैं। जस्टिस गवई का यह विचार भारत की सामाजिक और राजनीतिक गतिशीलता को गहराई से प्रभावित कर सकता है। यह नीति को और समावेशी और न्यायसंगत बना सकता है। मुख्य न्यायाधीश के विचार को लागू करने के लिए संसद की मंजूरी और व्यापक सामाजिक सहमति की आवश्यकता होगी। इस मुद्दे पर एक संतुलित और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांतों को बनाए रखे और साथ ही नीति को समय के साथ प्रासंगिक बनाए। मुख्य न्यायाधीश गवई का यह दृष्टिकोण न केवल आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने का अवसर प्रदान करता है बल्कि भारत के सामाजिक ताने-बाने को और मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। (अदिति)