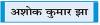देश की सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं सेना और नागरिकों के अच्छे संबंध
अक्सर ही सेना, सैनिकों और उनके द्वारा की गई कोई कार्रवाई बाले नेताओं से लेकर आम जन द्वारा आलोचना की जाती रहती है। कोई भी टिप्पणी करने से पहले यह समझना ज़रूरी है कि भारत की सैन्य व्यवस्था का संचालन कैसे होता है और कौन करता है।
सैन्य व्यवस्था : स्वतंत्रता मिलने से पहले भारतीय सेना का गठन ब्रिटिश हुकूमत द्वारा देशवासियों को दबाने और उन पर अत्याचार कर उन्हें हमेशा गुलाम बनाये रखने के लिए किया गया था। सेना प्रमुख की हैसियत गवर्नर जनरल के बाद थी और वह सभी तरह के फैसलों में प्रमुख भूमिका निभाता था। अधिकारियों में भारतीय भी थे और जब आज़ाद हुए तो उनकी मानसिकता में भी बदलाव आया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिशा में सबसे पहला काम यह किया कि सेना को राजतंत्र से बाहर निकाला और देश के रक्षा मंत्रालय के अधीन कर दिया। इससे हुआ यह कि सैन्य कमांडरों की देश की सुरक्षा के अतिरिक्त अन्य कोई ज़िम्मेदारी नहीं थी। प्रशासनिक व्यवस्था में उनका दखल नहीं था और वे किसी भी प्रकार के नीति निर्धारण के लिए सरकार पर आश्रित थे। मंत्रालयों के सचिव किसी भी योजना की जांच परख कर मंत्रियों के पास भेजते थे और स्वीकृति मिलने के बाद उस पर अमल किया जाता था।
देखा जाए तो यह व्यवस्था का पहला चरण था जो 1947 से 1962 तक चला। चीन से युद्ध की चुनौती सामने आई और हम पराजित हुए तो लगा कि कहीं न कहीं कुछ ऐसा है जिसे अगर समझा और बदला नहीं गया तो देश सैन्य ताकत में पीछे रह जाएगा। 1957 से 1962 तक तब के रक्षा मंत्री कृष्णा मेनन की राजनीतिक सोच की भी आलोचना हुई और उन्हें इस पराजय के लिए ज़िम्मेदार माना गया था।
पंडित नेहरू चीन से युद्ध के बाद बीस महीने जीवित रहे और उन्होंने इस दौरान अपने को हार का ज़िम्मेदार समझते हुए भारत की सैन्य शक्ति का विस्तार करने की योजना बनाई। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने भारत की सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान नहीं दिया। उनकी सोच थी कि दूसरे विश्व युद्ध की भयानक तस्वीर देखकर कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को युद्ध के ज़रिए सुलझाने की कोशिश नहीं करेगा। चीनी आक्रमण ने उन्हें वास्तविकता के दर्शन करवाए क्योंकि उस समय चीनी सेना के सामने हमारी सेना बौनी साबित हुई थी। हालांकि हमारे सैनिक बहुत बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन तथ्य यही था कि यदि भारतीय सेना मज़बूत होती तो परिणाम अलग होते। नेहरू जी ने इस बात को गंभीरता से लिया और युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए आवश्यक शक्ति जुटाने के प्रयास शुरू कर दिए।
सेना की प्रतिष्ठा : सन् 1963 से 1998 का दौर सेना और नागरिकों के संबंधों का दूसरा चरण कहा जा सकता है। लाल बहादुर शास्त्री ने सैनिक मामलों पर सामान्य जनता से संवाद करने के लिए जय जवान का उद्घोष किया। 1965 के पाकिस्तान के साथ युद्ध में जीत मिलने का कारण हमारी सैन्य क्षमता थी, लेकिन उससे अधिक भारतीयों ने एकजुटता और साहस का परिचय दिया। सरकार ने नागरिकों और सैनिकों के बीच जो दूरी बन गई थी, उसे कम करने के प्रयास किए और अपनी कमियों को सुधारने में लग गई। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें आधुनिक हथियारों से लैस किया और युद्ध की नई तकनीक से परिचित कराया। हमने अमरीका और रूस दोनों से युद्ध के शस्त्र और तकनीक लेने की बात की थी। इस अवधि में जो भी युद्ध हुए उनमें भारत की विजय हुई। इसका सबसे बड़ा कारण नागरिकों का अपने राजनीतिक नेतृत्व में विश्वास और सैनिकों के शौर्य पर आस्था थी।
सरकार ने शुरू में ऐसे लोगों को रक्षा मंत्रालय में नियुक्त किया जिन्हें सैन्य मामलों की जानकारी थी। सैनिकों के प्रशिक्षण में उन्हें प्रत्येक क्षेत्र में काम करने के लिये प्रशिक्षित करना और जब भी कोई आवश्यकता हो, नागरिकों की सुरक्षा का दायित्व लेने के तैयार रहने के लिए योग्य बनाना सम्मिलित है। अधिकारियों का चयन और प्रशिक्षण दोनों ही क्षेत्रों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि सैन्य अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर काम किया जाए।
इस व्यवस्था का तीसरा चरण 1999 से 2019 का कहा जा सकता है जिसकी शुरुआत कारगिल युद्ध से हुई थी। सेना का पुनर्गठन हुआ और चीफ ऑफ डिफैंस स्टाफ का एक नया पद बनाया गया। अभी तक सामान्य नागरिक सैनिक गतिविधियों को लेकर अधिक ध्यान नहीं देते थे। यद्यपि सेना के कार्यकुशल होने पर किसी को संदेह नहीं होता था, लेकिन कुछ विपक्षी दल और उनके नेताओं की तरफ से विवादास्पद बयान आने लगे जिस पर केंद्र सरकार को चिंता होनी स्वाभाविक थी।
एक बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह का कड़ा प्रशिक्षण भारतीय सेनाओं के सभी अंगों के जवानों को दिया जाता है, उसी का परिणाम यह हुआ कि वे हर मोर्चे पर सफलता हासिल करते रहे। यह ज़बरदस्त समन्वय और अदम्य साहस का प्रतीक है जिसने हमेशा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया। शस्त्रों का परिचालन आसान नहीं होता लेकिन उनका व्यवहार ऐसा होता है कि जैसे इन्हें चलाना कोई बड़ी बात नहीं। इतनी सक्षम सेना के बारे में जब कोई नेता सवाल खड़े करता है तो सैनिक टिप्पणी नहीं करते बल्कि आम लोग उस नेता को जवाब देते हैं। कुछ नेता जब सैन्य कार्रवाइयों के सबूत मांगते हैं, तब उनके अपने ही दल के लोग उनकी आलोचना करते दिखाई देते हैं।
सन् 2020 से अब तक का दौर बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। चीन और पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वे भारतीय सैन्य बलों के साथ मुठभेड़ में टिक नहीं सकते। इसलिए वे कोशिश करते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से हमारा और सैनिकों का मनोबल तोड़ सकें, लेकिन इसमें भी वे कामयाब नहीं हो पाते।
सामान्य नागरिक के रूप में हमें यह समझना होगा कि हमारी सेना पूर्णतया सक्षम और मज़बूत है, यह बात ऑपरेशन सिंदूर से एक बार फिर साबित हो चुकी है। राजनीतिक नेतृत्व की आलोचना करने के बहाने सेना के शौर्य पर सवाल खड़े करना कतई उचित नहीं है। इन नेताओं को यदि कुछ घंटे भी सेना की तैयारियों और उनके प्रशिक्षण को देखने का अवसर मिल जाए तो वे निश्चित रूप से भविष्य में कभी सैनिक नेतृत्व की आलोचना नहीं कर पाएंगे। एक सैनिक को अपना बलिदान देने के लिए सदा तैयार रहना होता है ताकि देशवासियों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। विश्व में अमरीका, रूस, चीन के बाद हमारी बड़ी सैन्य शक्ति है और हमारे सैनिकों ने सिद्ध किया है कि हम अपने इरादों में हमेशा सफल रहे। उनकी प्रशंसा के स्थान पर आलोचना करना उचित नहीं है। यह सैनिक नेतृत्व के सोचने का विषय है कि कब और किस प्रकार शत्रु को हराना है, विशेषकर तब राजनीतिक नेतृत्व ने उन्हें कोई भी कार्रवाई करने की अनुमति दी हुई है। नागरिक और सैन्य संबंधों के हित में यही ठीक होगा कि दोनों अपनी सीमा में रह कर काम करें।