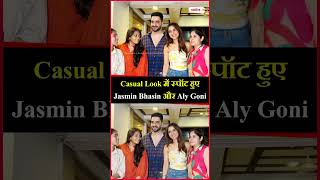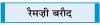पानी-पानी होते शहर, आखिर कौन है ज़िम्मेदार ?

देश के अनेक शहरों में जलभराव एक ऐसी समस्या है जो हर साल खासकर मानसून के दौरान एक भयावह रूप ले लेती है। देश के ‘स्मार्ट सिटी’ कहे जाने वाले महानगरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक, थोड़ी-सी भी मूसलाधार बारिश होते ही सड़कें नदियों और तालाबों में तब्दील हो जाती हैं। इस स्थिति में सारा दोष सीधे तौर पर प्रशासन पर मढ़ दिया जाता है और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन यह समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि यह केवल ‘सिस्टम फेल’ होने का मामला नहीं है, बल्कि इसमें नागरिकों की लापरवाही का भी एक बड़ा योगदान हो सकता है। यह एक जटिल समस्या है जिसके कई पहलू हैं और इसका समाधान भी बहुआयामी दृष्टिकोण से ही संभव है।
हाल के दिनों में देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने स्मार्ट सिटी की पोल खोल कर रख दी है। मुम्बई, दिल्ली, गुरुग्राम, पटना, लखनऊ, कोलकाता और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से लेकर छोटे-छोटे कस्बों तक, हर ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया, वाहन बहते नज़र आए और सड़कों पर नावें चलती दिखीं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ, लेकिन हर साल मानसून आते ही यही दृश्य देखने को मिलते हैं। इस साल की जुलाई की शुरुआत में ही मुम्बई में मात्र दो दिनों की बारिश ने लोकल ट्रेन सेवाओं को ठप कर दिया। कई स्कूल-कॉलेज बंद करने पड़े और निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए। दिल्ली-एनसीआर में कई मुख्य सड़कों पर 3-4 फुट तक पानी भर गया, जिससे घंटों तक ट्रैफिक जाम लगा रहा। गुरुग्राम की आईटी कम्पनियों में कामकाजी लोग ऑफिस तक नहीं पहुंच सके। लखनऊ में एक अस्पताल की आपातकालीन सेवाएं ठप हो गईं क्योंकि जलभराव ने एम्बुलेंस को प्रवेश ही नहीं करने दिया। ये घटनाएं केवल प्रकृति की मार नहीं हैं, बल्कि सामाजिक लापरवाही का भी परिणाम हैं।
शहरों की जल निकासी प्रणाली बेहद जर्जर हालत में है। कई जगहों पर सीवर और नालों दशकों पुराने हैं, जिनका आधुनिकीकृत नहीं किया गया। जल निकासी के मार्गों की सफाई व मरम्मत न होने और बाढ़ नियंत्रण योजना की अनुपस्थिति के कारण तेज़ बारिश बड़े शहरों के लिए आपदा बन जाती है। कई शहरों में पुराने नालों और जलमार्गों पर अतिक्रमण कर इमारतें, दुकानें और बस्तियां बना दी गई हैं। कुछ क्षेत्रों में झीलें और तालाब या तो पाट दिए गए हैं या उन्हें रिहायशी इलाकों में तब्दील कर दिया गया है। इसके कारण वर्षा का पानी निकलने का प्राकृतिक रास्ता बंद हो जाता है और पानी सड़कों, गलियों, अंडरपास और घरों में भर जाता है। घरों, दुकानों, रेस्तरां और निर्माण स्थलों से निकलने वाले कचरे को सही तरीके से ठिकाने नहीं लगाया जाता। लोग बेझिझक प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट, खाने-पीने का बचा हुआ सामान, कपड़ों के टुकड़े, यहां तक कि निर्माण सामग्री का मलबा नालियों और सीवर लाइनों में फेंक देते हैं। उन्हें यह समझने की ज़रूरत है कि नाली या सीवर लाइन कोई कूड़ेदान नहीं है। सरकार ने भले ही सिंगल-यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा रखा हो, लेकिन हकीकत यह है कि प्लास्टिक का उपयोग हर गली, हर दुकान और हर घर में जारी है। यह प्लास्टिक नालों और सीवर में जाकर उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। जब बरसात आती है तो यह प्लास्टिक सैलाब का कारण बन जाती है। कई बार जलभराव की असली जड़ यही प्लास्टिक अपशिष्ट होता है, जिसे नागरिक बेझिझक नालियों व सीवर लाईनों में फेंक देते हैं।
भारतीय समाज में स्वच्छता के प्रति एक गहरी उदासीनता देखी जाती है। लोग अपने घरों के अंदर तो साफ-सफाई रखते हैं, लेकिन घर के बाहर या सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने में जरा भी संकोच नहीं करते। ‘यह मेरा काम नहीं है’ या ‘यह सरकार की जिम्मेदारी है’ जैसी मानसिकता समस्या को और बढ़ाती है। जब तक हर नागरिक अपने आस-पास की स्वच्छता को अपनी व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक स्थिति नहीं सुधरेगी। अपने आस-पास की सफाई या जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त रखने में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी बेहद कम होती है। लोग अक्सर समस्याओं के समाधान के लिए केवल सरकारी मशीनरी पर निर्भर रहते हैं। यदि स्थानीय समुदाय एकजुट होकर अपने क्षेत्र की नालियों व सीवर लाईन की सफाई में मदद करें या कचरा फेंकने वालों को रोकेंतो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। हर नागरिक को अपने घर और दुकान से निकलने वाले कचरे को कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने की आदत डालनी चाहिए ताकि उसका सही तरीके से निपटारा हो सके। प्लास्टिक और पॉलीथिन का उपयोग पूरी तरह से बंद होना चाहिए या कम से कम किया जाए। खरीदारी के लिए कपड़े या जूट के थैलों का उपयोग किया जाना चाहिए। प्लास्टिक की बोतलों की जगह दोबारा उपयोग की जा सकने वाली बोतलों का इस्तेमाल किया जाए। ऐसी आदतें बड़ा बदलाव ला सकती हैं।
पानी-पानी होते शहर की समस्या केवल इंजीनियरिंग या प्रबंधन की नहीं है, बल्कि यह सामाजिक व्यवहार और नागरिक चेतना का भी प्रश्न है। जब प्रशासन के साथ-साथ आमजन भी अपनी ज़िम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाएगा, तभी वास्तव में स्मार्ट और स्वच्छ शहरों का सपना साकार हो सकेगा। यह एक साझी लड़ाई है जिसे सबको मिलकर जीतना है। यह समझना है कि शहर हमारा घर है, और इसकी देखभाल करना सबकी सामूहिक ज़िम्मेदारी है।
-मो. 70271-20349