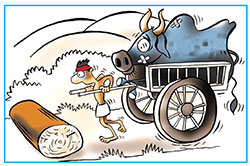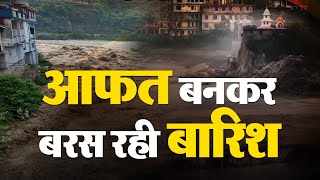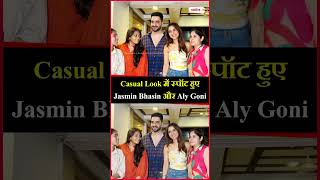असमानता संबंधी सरकारी दावे ह़क़ीकतों पर आधारित नहीं
पिछले कुछ महीनों में कई संस्थाओं ने भारत में लोगों की आमदनी का अध्ययन करके इनकम का पिरामिड बना कर दिखाया है। इन प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि देश के 90 प्रतिशत लोगों की बुरी हालत पर रोशनी पड़ी। इसका दूसरा नतीजा यह हुआ कि सरकार के बड़े-बड़े दावों पर सवालिया निशान लगा। सरकार कहती है कि इस समय देश की अर्थव्यवस्था का नंबर दुनिया में 5वें स्थान पर है, और जल्दी ही वह तीसरे स्थान की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। और तो और, सरकार 2047 तक यानी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे होने को अमृतकाल करार देती है, और यह भी कहती है कि तब तक भारत को विकसित बना दिया जाएगा और वह दुनिया की सर्वोत्तम अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगा। विकसित भारत का नारा इसी लहज़े में दिया जाता है। इन इनकम पिरामिडों ने इस तरह की दावेदारियों की हवा निकाल दी। यह देख कर सरकार ने सोचा कि क्यों न इस चर्चा को पटरी से उतारने के लिए एक और बढ़ा-चढ़ा दावा किया जाए।
लोकतांत्रिक राजनीति में अर्धसत्यों का चतुराई से इस्तेमाल करके कई तरह के संकटों का प्रबंधन किया जाता है। मीडिया की राज्य-भक्ति, एकतरफा आंकड़ों, स्पिन-डॉक्टरी और नैरेटिव के ज़रिये आज के प्रबंधन-विशेषज्ञ राजनीतिक नुकसान को न्यूनतम कर देते हैं लेकिन एक संकट ऐसा है जिसका प्रभाव प्रबंधन के इन हथकंडों से कम नहीं होता। वह है आर्थिक संकट। मुद्रास्फीति के आंकड़ों को डेटा-तिकड़म के ज़रिये कितना भी कम दिखाते रहिए, अगर महंगाई वास्तव में बढ़ी हुई है तो वह राजनीतिक नाराज़गी को बढ़ा कर मानेगी। इसी तरह बढ़ी हुई बेरोज़गारी का नतीजा युवाओं और शिक्षितों के बीच असंतोष में निकलना लाज़िमी है, भले ही बेरोज़गारों की संख्या को विभिन्न विधियों से कितना भी कम क्यों न दिखा दिया जाए। इसी तरह कुल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों को तो आकर्षक बनाया जा सकता है, लेकिन उनके आधार पर निजी क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए राज़ी नहीं किया जा सकता। मेक इन इंडिया के कितने भी दावे क्यों न किये जाएं, उपभोक्ताओं को बाज़ार में यह देखने से कोई नहीं रोक सकता कि वहां तो चीन का माल भरा हुआ है।
सरकार अच्छी तरह से जानती है कि प्रति व्यक्ति आमदनी के लिहाज़ से हमारा देश एक कमतर आय वर्ग वाले देशों में आता है। अगर ऊपर के 10-12 प्रतिशत लोगों को छोड़ दिया जाए तो ब़ाकी लोग किसी न किसी स्तर की गरीबी और विपन्नता का ही सामना कर रहे हैं। इसके बावजूद सरकार अपने बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों की मदद से बीच-बीच में आंकड़ा-प्रबंधन की मदद से दावा करती रहती है कि देश में गरीबी घट रही है, या आर्थिक विमषमता में कमी आ रही है लेकिन जैसे ही इन आंकड़ों की जांच की जाती है, ये दावे अपना मुंह छिपा कर कोने में चले जाते हैं। 2024 के चुनाव से कुछ पहले एनआईटीआई आयोग की तरफसे गरीबी कम करने का दावा करवाया गया था। इसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने तत्परता से अपने भाषण में कर डाला लेकिन यह पता लगने में देर नहीं लगी कि वह आयोग का दावा न होकर निजी स्तर पर लिख कर आयोग को पेश किये गये एक लेख का दावा था। ज़ाहिर है कि आयोग ने इस दावे की अधिकारिक पुष्टि कभी नहीं की। इसी महीने विश्व बैंक के हवाले से सरकार की तरफ से एक नया दावा यह किया गया है कि भारत दुनिया में सबसे कम विषमता वाला चौथा देश बन गया है। आर्थिक मामलों के जानकारों ने इस दावे की भी धज्जियां बिखेर दी हैं।
हम जानते हैं कि विश्व बैंक हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये संगठन किसी देश की अर्थव्यवस्था के आंकड़े स्वतंत्र रूप से जमा नहीं करते। वे उन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपने अनुमान लगाते हैं जो सरकारें उन्हें मुहैया कराती हैं। इसी महीने में विश्व बैंक के पॉवर्टी ऐंड इक्विटी ब्ऱीफ में बताया गया कि भारत का 2011-12 में उपभोग आधारित जिनी इंडेक्स 28.8 था जो 2022-23 में घट कर 25.5 रह गया। बैंक के इस अवलोकन को पकड़ कर सरकार ने तुरंत भारत को विषमता घटाने वाली दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। चालाकी यह दिखाई गई कि विश्व बैंक द्वारा कही गई पूरी बात छिपा ली गई। बैंक ने साथ में यह भी कहा था कि संभत: उसने विषमता का कम अनुमान लगाया है, क्योंकि उसके पास आंकड़े सीमित थे। इसी के बाद बैंक ने यह भी कहा कि विश्व-विषमता डेटाबेस दिखाता है कि आमदनी संबंधी विषमता का जिनी इंडेक्स 2004 के 52 से बढ़ कर 2023 में 62 हो गया है। ज़ाहिर है कि सरकार ने बैंक को आमदनी संबंधी आंकड़े नहीं, या बहुत कम ही दिये। जो दिये गये वे उपभोग संबंधी आंकड़े ही थे।
यहां सरकारी नियत उपभोग संबंधी आंकड़ों का अपने पक्ष में दोहन करने की थी। पहली नज़र में ही ये आंकड़े भारत की सच्चाई से परे साबित हो जाते हैं। क्या किसी को यकीन होगा कि भारत के सबसे अमीर पांच प्रतिशत लोग साल भर में प्रति व्यक्ति ढाई लाख रुपए के आसपास (20,824 रु. प्रति माह) ही ़खर्च करते हैं? असलियत तो यह है कि ये लोग रेस्त्रां में खाने-पीने, डेस्टिनेशन वेडिंग करने, विदेशों और भारतीय रिज़ोर्ट्स में सैर-सपाटा करने, डिज़ायनर कपड़े ़खरीदने, महंगी घड़ियां और इलेक्ट्रानिक सामान खरीदने में इसकी कई गुना रकम खर्च करते हैं। इसके मुकाबले दिल्ली और मुम्बई में रहने वाला 4 लोगों का सामान्य परिवार (देश की आबादी का 80 प्रतिशत) बताता है कि वह एक महीने में 30,692 रुपए खर्च करता है। इस तरह के आंकड़ों से जो तुलनात्मक जिनी इंडेक्स बनती है, वह हमारी आर्थिक असलियत की नुमाइंदगी नहीं करती।
आर्थिक असमानता की चर्चा करते समय हमें हमेशा आमदनी और सम्पत्ति संबंधी स्वामित्व के आंकड़ों पर ही ़गौर करना चाहिए। ह़क़ीकत यह है कि देश के ऊपरी दस प्रतिशत लोगों का आमदनी में हिस्सा 57.7 प्रतिशत है। नीचे के 50 प्रतिशत लोगों की हिस्सेदारी केवल 14.6 प्रतिशत ही है। सम्पत्ति के लिहाज़ से देखा जाए तो ऊपर के 10 प्रतिशत लोग 65 प्रतिशत सम्पत्तियों के स्वामी हैं, और नीचे के 50 प्रतिशत लोग महज़ 6.4 प्रतिशत सम्पत्तियां रखते हैं। यानी आमदनी से भी अधिक विषमता सम्पत्तियों के मामले में है। बीच के 30 प्रतिशत लोग ही ऐसे हैं जो रोज़ी-रोटी चलाने की शर्तों को पूरा कर पाते हैं, लेकिन उनकी आमदनी भी इतनी नहीं होती कि वे मनचाही चीज़ों को ़खरीदने का साहस कर सकें। बात ़खत्म करने से पहले इस विडम्बना पर भी ़गौर करने की ज़रूरत है कि जीएसटी का 64 प्रतिशत इन्हीं नीचे के 50 प्रतिशत लोगों से आता है, और ऊपर के 10 प्रतिशत जीएसटी का 4 प्रतिशत ही देते हैं।
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।