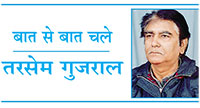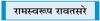गरीबी के अंधकार में जीने को मजबूर लोग
याद कीजिए सन् 1990 तब आर्थिक नीतियां लागू हुई थीं। उस समय भारत में सर्वाधिक पैरवी करने वाले थे, डा. मनमोहन सिंह। उनका यह दावा था कि इन सुधारों से भारत विकास के नये प्रतिमान खड़े करेगा। जी.डी.पी. छलांग मार कर आगे बढ़ेगी। भारत में उन्हें तथा मोंटेक सिंह आहलूवालिया को बहुत समझदार और आर्थिक संकटों के असरदार देखने वाले दृष्टि सम्पन्न व्यक्ति स्वीकार किया गया था। तब आई.एम.एफ. ने भी एक कदम आगे जाकर इसे भारत के लिए ‘आर्थिक पुनर्जागरण’ बताया था। बताया जा रहा था कि देश में जितने अधिक अमीर होंगे उतना ही देश को लाभ पहुंचेगा। तरीका क्या सुझाया कि इनसे रिस-रिस कर धन-सम्पदा गरीब अवाम तक जाएगी। व्यवहार में कुछ समय बाद ही ये तमाम भविष्यवाणियां कपोल काल्पनिक सिद्ध हो गईं। बताया गया कि फोर्ब्स की बिलियनेयर रैकिंग के अनुसार 1991 में भारत में केवल एक खरबपति था। आज 271 हैं। हम इस पर ज़रूर खुश हो जाते अगर गरीबी में बेतहाशा वृद्धि न हुई होती।
मार्क्सवादी चिंतन मजदूर किसान को सर्वहारा वर्ग कहता रहा और इसकी मुक्ति के उपाय सोचता रहा। भारत समाजवादी दर्शन से प्रभावित रहा। भारतीय लेखक भी गरीब वर्ग के ऊपर उठने का स्वप्न देखते रहे, लेकिन ज्यादा कुछ यथार्थ के पटल पर हो न पाया। बाद में सोवियत संघ रूस भी मार्क्स की अवधारणाओं के अनुरूप चल न पाया और बिखर गया।
नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रतिदिन 30 किसान और खेतिहर मजदूर कंगाली और कज़र् का बोझ न उठा पाने के कारण आत्महत्या का फंदा चूमने को विवश होते हैं। कुछ जाने-माने अर्थ-शास्त्री यह कह रहे हैं कि ़गैर ज़िम्मेदार और पूंजीपरस्ती ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। उन्हें यह कहते हुए कोई हिचक नहीं होती कि हम लगभग तबाह हो चुकी अर्थ-व्यवस्था के भग्नावशेषों पर खड़े हैं और इस मलबे में वे स्वदेशी और विदेशी कॉर्पोरेट भी बिखरे हैं जिनकी खैरख्वाही में हर वैध और अवैध फैसला किया जाता रहा है। कुछ समय पहले प्रकाशित रिपोर्ट द्वारा खुलासा किया गया कि देश के केवल दस खरबपतियों की जी.डी.पी. का 10 प्रतिशत, यानी 34 लाख करोड़ रुपए की सम्पत्ति है जो निर्धनतय पचास करोड़ लोगों की सम्पत्ति से भी ज्यादा है। ये वे लोग हैं जिनका ऊर्जा, टैलीकॉम, आई.टी., रिटेल आदि क्षेत्रों में एकाधिकार है। ये सरकार के लिए ‘यूनिकार्न’ और मुख्यधारा की मीडिया के लिए विकास का पर्याय हैं।
दूसरी तरफ बलूम वेंचर्स की रिपोर्ट बताती है कि देश में एक सौ करोड़ लोग ऐसे भी हैं, जिनके पास खर्च करने के लिए रुपये ही नहीं है। वे अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर पाने में अक्षम हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत बहुसंख्यक मज़दूरों के लिए कोई श्रम कानून नहीं है। जबकि उन्हें देश की नींव कहा जाता है इनके श्रम के पक्ष पर ही खेत और कारखाने चलते हैं। श्रम मंत्रालय के अनुसार इनकी एवरेज मासिक मज़दूरी दस हज़ार रुपए से भी कम है। इनमें महिला मज़दूर की दशा और भी खराब है। उनकी मासिक आय पांच हज़ार रुपए भी नहीं हो पाती। प्रसिद्ध विद्वान जेमेसन ने कहा है कि विश्व-अर्थ व्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय नियमों के पहले नियंत्रण और ‘मुक्त विश्व’ की अवधारणा के साथ-साथ हमारे समय का महत्त्वपूर्ण यह हो गया है कि बिजली से चलने वाली मशीनों की तरह कम्प्यूटर, मास मीडिया और सूचना-संसाधान वाले उपकरण ज्यादा महत्त्वपूर्ण हो गए हैं।
अमीर-गरीब के बीच अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। यह स्थिति किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। गांधी या भगत सिंह को भारत की यह दशा स्वीकार न होती। यह अंतर कम होना चाहिए नहीं तो गरीब के लिए नरक और अमीर के लिए स्वर्ग जैसे हालात होंगे।