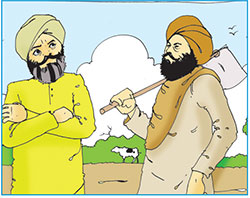किसानों की आय बढ़ाने के लिए लाभदायक मूल्य देना ज़रूरी
किसानों की आय कम होना बेहद चिन्ता का विषय है। इसकी वार्षिक दर बढ़नी चाहिए, परन्तु आय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो रही। विगत वर्षों के मुकाबले गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ कर 2585 रुपये हो जाने के बावजूद किसान संतुष्ट नहीं, क्योंकि खर्च बढ़ गया है और उसके अनुसार फसल की की कीमतें नहीं बढ़ीं। किसान यूनियन ने मांग की है कि फसलों की कीमत किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिलनी चाहिएं, जिसके बिना कृषि का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए फसलों की कीमतें बढ़ाने के अतिरिक्त कई अन्य भी चुनौतियां सामने हैं, जिन्हें दूर करना ज़रूरी है।
सबसे बड़ी चुनौती अनुसंधान की है, जिसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है और इसे तेज़ किया जाना ज़रूरी है। गेहूं, धान के योग्य विकल्प किसानों को दिए जाएं। अनुसंधान गेहूं तथा धान के अतिरिक्त अन्य समस्याओं तथा फसलों संबंधी भी सफलता तथा मज़बूती से किए जाने की दरकार है। विशेषकर बासमती की गुणवत्ता की ओर अनुसंधानकर्ताओं का विशेष ध्यान होना चाहिए, जिससे विदेशों की मंड़ी में इसका उच्च दाम मिले। अनुसंधानकर्ताओं द्वारा बागवानी, सब्ज़ियों की काश्त, तेल बीज, दाल फसलों, पशु पालन तथा मछलियों आदि के अनुसंधान तथा उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है ताकि इन क्षेत्रों के किसानों की आय बढ़े तथा फसली विभिन्नता में सफलता मिले।
विगत दो वर्षों में मार्च में अधिक तपिश के कारण गेहूं की फसल पर प्रभाव पड़ा। इस वर्ष बारिश तथा बाढ़ से धान, बासमती का उत्पादन कम हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्ष 2050 तक तपिश 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने की सम्भावना है। अनुसंधान में भविष्य के पर्यावरण को ध्यान में रखना पड़ेगा। किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही तकनीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। धान की फसल में लगातार पानी खड़ा करने की प्रथा को विशेषज्ञों की सिफारिशों के अनुसार छोड़ना पड़ेगा और पानी की अधिक बचत वाले तिपका तथा छिड़काव सिंचाई आदि साधन अपनाने पड़ेंगे। चावल के विश्व प्रसिद्ध विशेषज्ञ डा. गुरदेव सिंह खुश ने पंजाब तथा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को सलाह दी थी कि बड़े किसानों को बिजली की मुफ्त सुविधा बंद कर दी जाए, जिससे पानी की बचत होगी। चाहे छोटे तथा सीमांत किसानों को यह सुविधा उपलब्ध रहे। डा. सरदारा सिंह जौहल द्वारा इस संबंधी ज़ोर देने के बावजूद राजनीतिक कारणों से इस सुझाव को क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा सका।
किसानों द्वारा फसलों को ज़रूरत से अधिक नाइट्रोजन डाली जा रही है, जिससे पर्यावरण और पानी के प्रदूषित होने की समस्या भी पैदा होती है। रबी की मुख्य फसल गेहूं में पी.ए.यू. द्वारा की गई 110 किलो प्रति एकड़ यूरिया डालने की सिफारिश की बजाय किसान 225 किलो प्रति एकड़ तक भी यूरिया फसल को डाल रहे हैं। गेहूं पंजाब में 35-36 लाख एकड़ क्षेत्रफल तथा भारत में लगभग 3 करोड़ एकड़ क्षेत्रफल पर काश्त की जाती है। चाहे भारत सरकार ने थैले में 50 किलो यूरिया डालने की बजाय 45 किलो यूरिया पैक करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी खपत कम हो सके जबकि ऐसा नहीं हुआ। अभी गेहूं की बिजाई शुरू होने में तीन सप्ताह से अधिक समय शेष है (चाहे बिजाई नवम्बर में ज़ोर पकड़ेगी), परन्तु किसान अभी से ही डी.ए.पी. तथा यूरिया का प्रबंध करने के लिए इधर-उधर घूम रहे हैं। किसानों को यह खाद लेने के लिए अन्य कृषि सामग्री जैसे कि कीटनाशक तथा अन्य दवाइयां आदि खाद के साथ खरीदनी पड़ती हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है, परन्तु फिर भी यह सिलसिला व्यापक स्तर पर जारी है।
धान की काश्त अधीन क्षेत्रफल कम करके विभिन्नता लाने की ज़रूरत है, परन्तु यह क्षेत्रफल कम होने की बजाय बढ़ रहा है, जो 31 लाख हैक्टेयर को छू गया। बासमती के अतिरिक्त धान के योग्य विकल्प जिनके अपनाने से धान के समान आय हो, अनुसंधान करके किसानों को दिए जाने की ज़रूरत है। भारत तेल बीज तथा दालों का आयात कर रहा है। इसलिए इन फसलों की काश्त बढ़ाने की ज़रूरत है। किसानों का खर्च बढ़ रहा है। आय और उत्पादन में कमी आ रही है। इस वर्ष धान तथा बासमती का उत्पादन कम होने की सम्भावना है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होगी। राज्य के किसानों पर 2 लाख से अधिक प्रति घर कज़र् है जबकि भारत में यह आंकड़ा लगभग 74000 रुपये है।
एक राष्ट्रीयकृत बैंक के गांव की शाखा के प्रबंधक ने बताया कि उस बैंक से सभी गांव के घरों ने कज़र् लिया हुआ है जब तक वह पिछला कज़र् वापिस नहीं करते, बैंक आगे कज़र् नहीं देता जिस कारण किसानों को मुश्किल आती है। फसलों की काश्त के लिए किसानों को कई तरह की सामग्री पहले लेनी पड़ती है, जबकि किसानों को पिछली बेची गई फसल के पैसे बाद में मिलते हैं। किसानों को आढ़ती या बड़े ज़िमीदारों से कज़र् लेना पड़ता है।
किसानों की आय इसलिए भी कम है कि अधिकतर किसानों के खेत छोटे हैं। वर्तमान हालात में यह कृषि व्यवहारिक नहीं। कोई कोआप्रेटिव फार्मिंग जैसी विधि नहीं है, जो इस समस्या का समाधान कर सके। किसानों के कज़र् खत्म करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए उनकी आय बढ़ानी पड़ेगी। उनका उत्पादन बढ़ा कर ही कृषि लाभदायक बनाई जा सकती है।