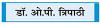इज़राइल-हमास समझौता -क्या स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य के बिना शांति संभव है ?
हमास ने अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा कर दिया है और लगभग 2,000 फिलिस्तीनी भी इज़राइल की जेलों से आज़ाद हो गये हैं। आखिरकार दो साल बाद डरावने सपने का अंत हुआ है। लोग अपने घर वापस आये हैं, लेकिन सभी के चेहरों पर मुस्कान नहीं लौटी है। युद्ध का अंत हमेशा ही आशावादी होने का समय होता है। लोग राहत की सांस लेते हैं, खुशी के फव्वारे फूट उठते हैं और एक प्रकार की सामूहिक भूलने की बीमारी पैर पसारने लगती है कि कोई उन खूनी दिनों को याद नहीं करना चाहता है। जब समाज शांत दिनों की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो कोई यह याद नहीं करना चाहता कि जंग क्यों शुरू हुई थी और इसके बजाय वह पुनर्निर्माण, योजना में निवेश करने लगते हैं, बेहतर भविष्य के सपने देखते हुए। इसके बावजूद पश्चिम एशिया में उत्साह के दिन हमेशा ही गिनती के रहते हैं। वर्तमान समझौता इस बात की गारंटी नहीं है कि टकराव फिर से जल्द आरंभ नहीं हो सकता। दरअसल जब तक फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा दिये जाने का विरोध होता रहेगा और यह बेवकूफी की मांग उठती रहेगी कि हमास से हथियार गिरवा दिये जाये व इज़रायल को आधुनिक हथियारों से लैस किया जाये, तब तक पश्चिम एशिया में स्थायी शांति की कल्पना करना ही फिजूल है।
हालांकि 2 नवम्बर 1917 की बालफौर घोषणा में इज़रायल राज्य के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं था, केवल यहूदियों को फिलिस्तीन में बसाने की बात थी और वह भी फिलिस्तीनियों की अनुमति के बिना यानी घोषणा पूर्णत: एकतरफा थी लेकिन आज जब इज़रायल को अपने ‘अस्तित्व की रक्षा करने के अधिकार’ की वकालत की जाती है तो फिलिस्तीन राज्य के गठन का विरोध करना न्यायोचित कैसे हो सकता है? जबकि 1948 में उनकी ही ज़मीन पर जबरन कब्जा करके इजरायल को थोपा गया। पश्चिम एशिया का इतिहास हमें बताता है कि शांति व सुनहरे भविष्य के वायदे जो ‘नोबेल शांति पुरस्कार’ के स्वयंभू दावेदार करते हैं, उनकी सोच पर जल्द ही (बल्कि बहुत जल्द) कबीलाई युद्ध के बादल छाने लगते हैं। अमरीका के अनेक राष्ट्रपति पश्चिम एशिया में शांति बहाली के नाम पर नोबेल शांति पुरस्कार के ‘विजेता’ बन चुके हैं। लेकिन उनमें से एक ने भी इज़रायल को हथियार सप्लाई करना बंद नहीं किया बल्कि दूसरे देशों पर अजीबोगरीब पाबंदियां लगायी हैं। मसलन लेबनान को वायु सेना रखने से वंचित किया हुआ है, नतीजतन इज़राइल जब चाहता है लेबनान पर हवाई हमला कर देता है और पश्चिम एशिया में तनाव बना रहता है।
अब डोनाल्ड ट्रम्प ने गाज़ा में इज़रायल व हमास के बीच दो साल से चल रहे युद्ध पर विराम लगाया है (नोबेल शांति पुरस्कार के लालच में), लेकिन वह भी इस क्षेत्र की खूनी प्रवृत्ति को बदलने में नाकाम रहे हैं। इज़रायल संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ‘नये मध्य पूर्व में ऐतिहासिक सुबह’ की घोषणा अवश्य की है, लेकिन साथ ही इज़रायल को आधुनिक हथियार देने का वायदा भी किया। कमाल है, आप हमास से तो हथियार त्यागने की उम्मीद करते हो (जिससे उसने इंकार कर दिया है) लेकिन इज़रायल को हथियार देना चाहते हो, क्या यह कसाई द्वारा जानवर को रस्सी से बांधकर काटने जैसा कृत्य नहीं है? ट्रम्प का शांति फ्रेमवर्क युद्धविराम से अधिक पर निर्भर है। यह अमरीका, अरब राज्यों और यूरोपीय नेताओं के सहयोग व राजनीतिक इच्छा पर आधारित है। इसमें हमास को हथियारों से वंचित करने की तो इच्छा है, लेकिन बेंजामिन नेतान्याहू को युद्ध अपराधों से मुक्त करने का भी प्रयास है, जैसे निर्दोष बच्चों, महिलाओं व पत्रकारों को ‘कोल्ड ब्लड’ में मारना कोई जुर्म ही न हो। ट्रम्प ने तो इजरायल के राष्ट्रपति से आग्रह किया है कि वह भ्रष्टाचार के मामलों में नेतान्याहू को माफी प्रदान कर दें।
नेतन्याहू पर इज़रायल की अदालतों में भ्रष्टाचार के तीन अलग-अलग मुकदमे चल रहे हैं, जिनमें उनके खिलाफ अकाट्य साक्ष्य होने का अनुमान है। कुछ इज़रायली विशेषज्ञों का कहना है कि अदालत द्वारा सज़ा से बचने के लिए ही नेतन्याहू ने जंग को इतना लम्बा खींचा और बीच में जो युद्धविराम व शांति समझौते के अनेक अवसर आये उन्हें नाकाम किया। नेतन्याहू पर आरोप हैं कि राजनीतिक लाभ पहुंचाने के बदले में उन्होंने रईसों से 2,60,000 डॉलर मूल्य के ज़ेवरात, सिगार, शैम्पेन आदि लिए। नेतान्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑ़फ जस्टिस ने भी नरसंहार का दोषी माना है जिस कारण वह अनेक देशों की यात्रा नहीं कर सकते; क्योंकि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। पिछले दो सालों में एक बात तो एकदम स्पष्ट हो गई है कि जब तक फिलिस्तीन राज्य का गठन नहीं होने का, जिसका इज़राइल में अब भी विरोध है, तब तक पश्चिम एशिया में स्थायी शांति संभव न हो सकेगी। इस क्षेत्र में विस्तृत सुरक्षा फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, जिसकी सफलता सभी स्टेकहोल्डर्स की गुंजाइश पर निर्भर करती है कि वह एक-दूसरे का सम्मान करते हुए साथ रहने के लिए तैयार हो जाएं। यहूदी इतिहासकार प्रोफेसर अवि शलैम ने लिखा है, ‘1948 में इज़रायल के बनने से पहले अरब संसार विशेषकर लेबनान, सीरिया, फिलिस्तीन व इराक में लगभग 8,00,000 यहूदी शांतिपूर्वक रहते थे और इराक का यहूदी समाज इनमें सबसे अधिक प्रभावी था, जो वहां 2,500 वर्षों से रह रहा था। वह बहुत सफल था और स्थानीय लोगों के साथ मिल-जुलकर रहता था। मुस्लिम, यहूदी व ईसाई सह-अस्तित्व संभव व मज़बूत था, वह रोजमर्रा की हकीकत थी।
मगर 1948 में ज़ियोनिस्ट के आने से सबकुछ बदलने लगा। मैं और मेरा परिवार अरब यहूदी थे, हम अरबी बोलते थे। हम कोई अन्य भाषा नहीं बोलते थे। हमारी संस्कृति अरब संस्कृति थी और हमारा फूड स्वादिष्ट व मसालेदार था, वह यूरोपीय फूड नहीं था। हम अरब यहूदी यूरोपीय यहूदियों से भाषा व संस्कृति में एकदम भिन्न थे। मार्च 1950 में इराक की संसद ने कानून बनाया कि अगर कोई अरब यहूदी देश छोड़कर जाना चाहता है तो वह एक साल के नोटिस पर एकतरफा वीज़ा के साथ जा सकता है। गिनती के यहूदियों ने ही जाने के लिए पंजीकरण कराया। अगले वर्ष बगदाद की यहूदी बस्तियों में पांच बम विस्फोट हुए, जिससे पैनिक फैल गया और इज़रायल की ओर पलायन होने लगा। 28 वर्षीय यहूदी वकील युसूफ बसरी इन विस्फोटों के लिए ज़िम्मेदार था, जो उसने मोसाद के इशारे पर कराये थे।’ इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पश्चिम एशिया में शांति भंग करने के लिए कितनी गहरी साजिशें होती हैं, इसलिए यह कहना गलत न होगा कि ट्रम्प के शांति प्रयास कभी भी दम तोड़ सकते हैं।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर