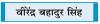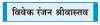जल, जंगल, ज़मीन, हवा और हम
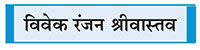
जल, जंगल, ज़मीन और हवा के सवाल आज जीवन और अर्थव्यवस्था की धमनियों के प्रश्न बन गये है। ‘पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज’ ने स्पष्ट किया है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण मौसमी चक्र बदल रहे हैं। अतिवृष्टि और सूखा दोनों की तीव्रता बढ़ रही है और यह बदलाव सीधे तौर पर नदियों के प्रवाह, जल भंडारण और खेतों की सिंचाई क्षमता को प्रभावित कर रहा है।
देश में इस बदलाव को स्पष्ट देखा जा सकता है। नदियों की सफाई के कई प्रयासों के बावजूद 645 नदियों में से ज़्यादातर हिस्सों में प्रदूषण चिंताजनक स्तर पर है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़े बताते हैं कि 271 नदियों के 296 हिस्सों में पानी ऐसे स्तर पर पहुंचा है जहां स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी और दैनिक उपयोग पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। गंगा, यमुना जैसी प्रमुख नदियां जहां धार्मिक और आर्थिक जीवन की रीढ़ हैं, वहीं इनकी जल गुणवत्ता की गिरावट पारम्परिक उपयोग और जैव विविधता दोनों के लिए खतरनाक संकेत है। ज़मीन की उर्वरता पर खतरा नए-नए रूप ले रहा है। औपचारिक शोध और सर्वे बताते हैं कि भारत के बड़े हिस्से में मिट्टी का कटाव तेज़ी से बढ़ा है। कुछ अध्ययनों का अनुमान है कि प्रति हेक्टेयर औसत मिट्टी क्षरण दर कई टन प्रति वर्ष है और देश का एक बड़ा हिस्सा गंभीर कटाव के प्रभाव में है। खेती के तरीकों में परिवर्तन, नदियों की घाटियों में निर्माण, पहाड़ी कटाव और अत्यधिक वर्षा की घटनाओं का संयोजन मिट्टी की ऊपरी सतह को क्षरित कर रहा है जिससे जैविक कार्बन और खेतों की दीर्घकालिक उपजाऊ शक्ति प्रभावित हो रही है। उपजाऊ मिट्टी ही खेत की ताकत होती है।
कृषि में रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक और असंतुलित प्रयोग से तात्कालिक उत्पादन तो बढ़ा, परन्तु दूसरी तरफ ज़मीन और भू-जल दोनों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रिपोर्टों और आंकड़ों के अनुसार उर्वरक की खपत में वृद्धि जारी है और 2023-24 में कुल खपत के आंकड़े लाखों टन में दर्ज हैं, जिसके प्रभाव मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की कमी, नाइट्रेट और फॉस्फेट के घुलाव से भू-जल में प्रदूषण और जल तंत्रों में पोषक तत्व के संकट के रूप में सामने आ रहे हैं। यही पोषक तत्व नदियों और जलाशयों में जाकर अल्गल ब्लूम का कारण बनते हैं, जिससे डाइऑक्सीजनीकरण और जलीय जीवन का विनाश होता है। भू-जल का स्तर गिरना कोई कहानी नहीं, वास्तविकता है जो आंकड़ों में दर्ज है। भूमि के भीतर छिपा वह पानी जो पीने के योग्य बनाने और खेतों की सिंचाई के लिए दशकों तक भरोसे का स्रोत रहा, अब अंधाधुंध दोहन से कई हिस्सों में तेज़ी से घट रहा है। केंद्रीय भू-जल बोर्ड और समकक्ष आकलनों से पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में वार्षिक क्षरण और निकासी की दर रिचार्ज से अधिक है।
औद्योगिक विकास ने देश को तेज़ आर्थिक उछाल दिए, पर उसका पर्यावरणीय बिल भी अद्यतन हो कर आया है। कच्चे तेल, कोयले और रसायनों पर आधारित खपत और उत्पादन केंद्रों के पास वायु गुणवत्ता की सीमा रेखा कम होना, जल निकासी में भारी धातुओं का मिश्रण और ठोस कचरे का असुरक्षित निपटान आसपास की ज़मीन और पानी को संक्रमित कर देता है। औद्योगिक विकास के मॉडल को हरित प्रौद्योगिकी और सर्कुलर अर्थव्यवस्था की शर्तों पर न बांधा गया तो विकास सिर्फ एक संख्यात्मक उपलब्धि रहेगी, परन्तु जीवन की गुणवत्ता घटती जाएगी। आम जन इन समस्याओं के केंद्र में हैं और समाधान भी उससे ही जुड़े हैं। मिट्टी की रक्षा के लिए खेती के नए तरीके, जैसे मूल रक्षा, मिल-जुल कर कवर क्रॉप्स, सीमांत वनरोपण और कटाव नियंत्रक संरचनाएं आवश्यक हैं। उर्वरकों का बुद्धिमानी से उपयोग, जैविक खाद को प्रोत्साहन और पोषक तत्वों के संतुलन की मॉनिटरिंग भू-जल और नदियों पर दबाव कम कर सकती है। औद्योगिक क्षेत्र में उत्सर्जन नियंत्रण, ट्रीटमेंट प्लांट की समयबद्ध क्षमता, विकास और सत्यापन तथा कचरा प्रबंधन की कठोर व्यवस्था शहरी हवा और ज़मीन की दशा सुधार सकती है। हम बड़े-बड़े सेमीनार या आधे अधूरे उपायों से संतोष नहीं कर सकते। ऐसे परिवर्तन चाहिए जिसमें कृषि, उद्योग, शहरी नियोजन और जल प्रबंधन एक दूसरे से जुड़े रणनीतियों के हिस्से हों।
नीति निर्माताओं के साथ-साथ स्थानीय समाज, किसान, उद्योगपति और नीति प्रवर्तक मिलकर तब तक स्थिति नहीं बदल पाएंगे, जब तक जल, जंगल, ज़मीन और हवा को केवल संसाधन मानकर उपभोग मात्र करने का समाज का मनोवैज्ञानिक रुझान नहीं बदलेगा। यह परिवर्तन आर्थिक प्रोत्साहनों, सामुदायिक शिक्षा और पारदर्शी आंकड़ों के माध्यम से लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जल पुनर्भरण और सीमा आधारित जल उपयोग नीतियों से भू-जल में सुधार दिखा है और नदियों के नज़दीकी बायो रेमिडिएशन तथा छोटे पैमाने पर सीवरेज निवारण से जल गुणवत्ता में स्थानीय सुधार हुए हैं, परन्तु यह पर्याप्त नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वित, विज्ञान संचालित और जनता से जुड़े सतत अभियानों की आवश्यकता है। अंतत: जल, जंगल, ज़मीन, हवा और हम का सवाल नैतिकता का भी है, यह मात्र तकनीकी समस्या नहीं है। (युवराज)