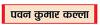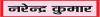क्या सरकारी दिशा-निर्देशों से ए.आई. नियंत्रित हो पायेगी ?
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय ने 5 नवम्बर, 2025 को भारत ए.आई. शासन-विधि दिशा-निर्देश जारी किये। यह 66 पृष्ठों का दस्तावेज़ है, जो भारतीय समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए.आई.) तकनीक को विनियमित करने और उसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के तरीकों को रेखांकित करता है। यह जो दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं, वह उन अनेक प्रयासों में शामिल हैं, जो सरकार ए.आई. प्रभाव शिखर सम्मेलन-2026 से पहले कर रही है। इस सम्मेलन का आयोजन भारत नई दिल्ली में करेगा। सवाल यह है कि दिशा-निर्देश क्या हैं? यह आवश्यक क्यों हैं? इनमें मुख्य बल किस बात पर है? भारतीय परिस्थितियां ए.आई. मॉडल्स के दिशा-निर्देश किस तरह से देखते हैं? इनसे ए.आई. इस्तेमाल और बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारों के संदर्भ में क्या चिंताएं उत्पन्न होती हैं?
बहरहाल, पहले यह समझना आवश्यक है कि इन दिशा-निर्देशों से सरकार किन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में भी ए.आई. का इस्तेमाल निरन्तर बढ़ता जा रहा है, अन्य देशों की तरह। ऐसे में यह ज़रूरी था कि ए.आई. उद्योग और उसके टूल्स को विनियमित करने के लिए कोई निरन्तर तरीका सरकार के पास हो, विशेषकर इसलिए भी कि अमरीका के बाद भारत लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स (एल.एल.एम.) जैसे चैटजीपीटी आदि का प्रयोग सबसे अधिक करता है। अगर यह सब अनियंत्रित रहेगा तो अराजकता की आशंका बनी रहेगी। दिशा-निर्देशों में कहा गया है, ‘भारत का लक्ष्य ए.आई. की परिवर्तनकारी क्षमता का दोहन करना है, समावेशी विकास व वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए, लेकिन साथ ही उन खतरों को भी संबोधित करना जो लोगों व समाज के लिए इससे उत्पन्न हो सकते हैं।’ उल्लेखनीय है कि भारत से पहले ब्लेटचेली पार्क (यूनाइटेड किंगडम), सियोल (दक्षिण कोरिया) व पेरिस (फ्रांस) में जो बहु-पक्षीय ए.आई. सम्मेलन हुए, उनमें आमतौर से एलएलएम व ए.आई. के विस्तार के अस्पष्ट प्रारम्भिक बिन्दुओं के अपने देशों में प्रबंधन पर सहमति बनी, जो खतरे उत्पन्न हो सकते हैं, उन पर नज़र रखी जाये व उनका वर्गीकरण किया जाये, अगर कुछ गलत हो जाये तो उसके लिए नीतियां बनायी जाएं और अन्य अनेक चीज़ों के अतिरिक्त सुरक्षा शोध भी आयोजित किये जाएं।
इस प्रक्रिया में सम्मलित होने हेतु भारत ने अपने लिए दिशा-निर्देशों के माध्यम से योजना रेखांकित की है। इससे पहले ड्राफ्ट फ्रेमवर्क उप-समिति ने तैयार किया था, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के नेतृत्व वाले सलाहकार गुट के तहत। लेकिन इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप जुलाई 2025 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने दिया है, जो उप-समिति से एकदम अलग है। इस समिति का नेतृत्व आईआईटी मद्रास में सेंटर फॉर रेस्पोंसिब्ल ए.आई. के प्रमुख बालारमण रविन्द्रन ने किया है। व्यक्ति-केन्द्रित जवाबदेही, निष्पक्षता व ए.आई. मॉडल्स की समझ आदि जैसे सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में दिशा-निर्देशों में सिफारिश की गई है कि सरकार के विभिन्न विभागों जैसे मंत्रालयों, क्षेत्रीय नियामकों, मानक स्थापित करने वाली एजेंसीज़ आदि के बीच में कम्युनिकेशन की लाइनें स्थापित की जाएं। यह सिफारिश भी की गई है कि यह गुट अक्सर आपस में मुलाकातें करें और कानून, स्वैच्छिक प्रतिबद्धता, मानक तय करने और ‘ए.आई. सुरक्षा टूल्स के एक्सेस में वृद्धि’ में बदलाव लाने के लिए सुझाव दें। इसकी निगरानी करने के लिए अंतर-मंत्रालय संस्था प्रस्तावित ‘ए.आई. गवर्नेंस ग्रुप’ होगी। मंत्रालयों से अलग दिशा-निर्देशों में वित्तीय उद्योग के लिए आरबीआई (जिसने अगस्त 2025 में बैंकिंग व वित्तीय आयोग के लिए अपनी एफ .आर.ई.ई.-ए.आई. कमेटी रिपोर्ट स्थापित की थी), नीति आयोग और मानक संगठन जैसे ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की भी सिफारिश की गई है।
दिशा-निर्देशों में निजी सेक्टर को भी सलाह दी गई है, मसलन कि वह ‘सभी भारतीय कानूनों का पालन सुनिश्चित करे, स्वैच्छिक फ्रेमवर्क अपनाये, पारदर्शी रिपोर्ट्स प्रकाशित करे, शिकायत निवारण व्यवस्था उपलब्ध कराये और टेक्नो-लीगल समाधानों से खतरों को कम करे’। अधिकतर सुरक्षा संबंधी सिफारिशें ए.आई. सेफ्टी इंस्टीच्यूट (ए.आई.एस.आई.) पर आधारित हैं, जो फ्रेमवर्क भारत सहित अनेक देशों में लागू है, जबकि इसके लिए कोई भौतिक इंस्टीच्यूट नहीं है, लेकिन सरकार ने इंडिया ए.आई. मिशन के तहत कुछ शिक्षाविदों को एकत्र किया है ऑनलाइन ए.आई.एस.आई. के रूप में। अन्य जगहों के समान ए.आई. नीतियों से इन दिशा-निर्देशों में मुख्य अंतर यह है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने व उसे सुलभ कराने पर बल दिया गया है। सिफारिश यह की गई है कि राज्य सरकारें ए.आई. को अपनाने में वृद्धि करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में पहल करें और डाटा व कंप्यूटिंग संसाधनों को एक्सेस कराने में इजाफा करें। दूसरी ओर सिफारिशों में ए.आई. व बौद्धिक सम्पत्ति से संबंधित अन्य देशों की चिंताओं का भी संज्ञान लिया गया है और कॉपीराइट कानून में परिवर्तन का सुझाव दिया है ताकि इस क्षेत्र में सामने आ रहे मुद्दों को संबोधित किया जा सके।
दिशा-निर्देशों में अन्य भारत-विशिष्ट वरीयताओं को भी दोहराया गया है जोकि सरकार ने व्यक्त की हैं, जैसे भारतीय भाषाओं के लिए ए.आई. मॉडल्स बनाना। एक सिफारिश में स्थानीय तौर पर प्रासंगिक डाटासेट्स पर बल दिया गया है ताकि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करने वाले मॉडल्स व एप्लीकेशंस बनाये जा सकें। सवाल यह है कि क्या दिशा-निर्देश ए.आई. से संबंधित सरकार की योजना के अनुरूप हैं? अधिकतर देशों की तरह केंद्र सरकार ने पूर्व-निवारक ए.आई. विनियमन से खुद को दूर ही रखा है, सिवाय एक महत्वपूर्ण अपवाद के डीपफेक का मुद्दा। दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेंट प्रमाणीकरण एक ज्वलंत मुद्दा है। दिशा-निर्देशों के जारी होने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय ने उन नियमों का प्रस्ताव रखा था, जिनके तहत सोशल मीडिया कम्पनियों कि ए.आई. के ज़रिये बनायी गईं तस्वीरों व वीडियोज को लेबल करना होता है। दिशा-निर्देशों के कुछ अन्य हिस्से भी हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पहले से ही किये जा रहे कामों के अनुसार हैं, मसलन इंडिया ए.आई. मिशन साझा कंप्यूट फैसिलिटी के लिए पहले से ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स (जीपीयू) हासिल कर रहा है और शोधकर्ताओं व स्टार्टअप्स से यह कंप्यूट कैपेसिटी की एक्सेस साझा कर रहा है। एक अन्य सिफारिश भी गतिशील प्रतीत होती है कि डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को ए.आई. व नीति सक्षम बनाने वालों से मिला दिया जाये। -इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर