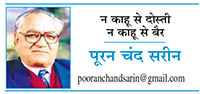लोगों के लिए पौष्टिक तथा मिलावट रहित भोजन सुनिश्चित बनाने की ज़रूरत
किसी भी देश की समृद्धि इस बात पर निर्भर है कि नागरिकों का खानपान कैसा है, वे कितने ऊर्जावान और स्वस्थ हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रति वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की शुरुआत सन् 2019 में की जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग अपने शरीर की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पौष्टिक भोजन करें। इस वर्ष का थीम भी यही है। समस्या यह है कि इसे प्राप्त करने में आने वाली रुकावटों को कैसे दूर किया जाये?
खाद्य सुरक्षा का मतलब
इस विषय का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि भोजन जीवित रहने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है, बल्कि मामला यह है एक ओर पौष्टिक भोजन की ज़रूरत है, दूसरी ओर तेज़ी से बढ़ते हुए हानिकारक विषाक्त खाद्य पदार्थों का उत्पादन है। यह बात मई 2024 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की एक रिपोर्ट में उजागर हुई है। इसमें कहा गया है कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड यानी किसी वस्तु को बहुत अधिक समय तक खाने लायक बनाये रखने के लिए रसायनों के इस्तेमाल से बना भोजन अपने दुष्प्रभावों के कारण सीमित तथा कुछ मामलों में वर्जित होना चाहिए। इसे इस तरह से समझते हैं। यह तो सब ही जानते हैं कि आज चारों तरफ जल्दबाज़ी में रहने से लेकर अफरा-तफरी तक का माहौल है। वक्त नहीं है, यह अक्सर सुनाई देता है। सब कुछ बहुत जल्दी पा लेने की चाहत में लोगों की दिनचर्या ऐसी बन गई है कि उनके पास चाहे सब कुछ करने का समय हो, लेकिन खाने का समय नहीं है। इसके लिए जब जैसा जो भी मिल जाये, पेट भर लेना ही काफी है। भोजन का कोई निश्चित समय न होना आज की युवा और अधेड़ पीढ़ी के लिए सामान्य है। अब यहां से खेल या व्यापार शुरू होता है। उन खाद्य पदार्थ निर्माताओं का जो कई दिन, सप्ताह या महीनों तक खाने योग्य उत्पादों को इस विशाल आबादी को उपलब्ध कराने का काम करते हैं।
विपरीत प्रभाव
असल में इन खाद्य पदार्थों को तैयार करने में जिन धातुओं और रसायनों का इस्तेमाल होता है, उनके दूरगामी परिणाम न केवल चिंताजनक हैं, बल्कि ख़तरनाक भी हैं। लम्बी अवधि तक इन्हें खाते पीते रहने से कैंसर, हृदय रोग, सांस संबंधी, मानसिक, पेट से जुड़ी बीमारियां और मृत्यु तक होने के आंकड़े दिये गये हैं। विडम्बना यह है कि इनका उत्पादन रोका नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने पर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट पहुंच सकती है। इसके अतिरिक्त पिछले दशकों में विज्ञान तथा टैक्नोलॉजी के इस्तेमाल से खाद्य पदार्थों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। उसकी पूरी खपत होना कठिन है और गोदामों में भी कब तक रखा जा सकता है। इसलिए प्रोसेस्ड फूड का चलन और उसके लिए औद्योगिक इकाई लगाना प्राथमिकता हो गया है। इसके अतिरिक्त खेत, खलिहान से लेकर कारखानों तक कच्चा माल पहुंचाने को ध्यान में रखकर सड़क परिवहन और आने जाने के साधनों का विकास हुआ है। पशु पालन, डेयरी उद्योग, जलीय जीवों को खाने योग्य बनाने और प्रोसेसिंग के ज़रिए उन्हें तरोताज़ा बनाये रखने के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अनिवार्य है। यह सब विशाल पैमाने पर होता है।
यदि इस उद्योग पर अंकुश लगाने की चर्चा भर की गई तो किसी एक नहीं बल्कि विश्व के अनेक विकासशील देशों में आर्थिक संकट आ सकता है। गरीब देशों में भुखमरी तथा बेरोज़गारी अपने चरम पर पहुंच सकती है। नागरिकों के इम्यून सिस्टम पर विपरीत प्रभाव पड़ना तय है। उनकी शारीरिक, मानसिक स्थिति कमज़ोर हो सकती है। असमय वृद्ध होने और जल्दी थक जाने के लक्षण दिखाई देने सामान्य हैं।
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर इस रिपोर्ट को लेकर सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर समझने के लिए व्यापक बहस होना आवश्यक है। हमारे देश में तो यह और भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हम आर्थिक दशा सुधारने के लिए अपने बढ़ते कदमों की गति नहीं रोक सकते, यह आत्मघाती होगा। लेकिन इसी के साथ यह भी सच है कि नागरिकों के स्वास्थ्य को लेकर कोई ढीलापन भी नहीं दिखा सकते। हमारी खेतीबाड़ी, फलों का उत्पादन और मुर्गी या मछलीपालन जैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन चुके कुटीर उद्योगों में रोज़गार की असीम संभावनाओं की अनदेखी नहीं की जा सकती।
अनुमान है कि हमारे शरीर की ताकत बनाये रखने के लिए साठ प्रतिशत ऊर्जा खानपान से प्राप्त होती है और शेष व्यायाम, प्रदूषण रहित वातावरण और सही जीवन शैली से मिलती है। अब इसमें डिब्बाबंद खाने पीने वाली चीज़ें बड़ी-बड़ी मशीनों से बनती हैं। उनमें रंग, फ्लेवर और एडिटिव मिलाये जाते हैं। इनमें सेहत के लिए नुकसानदायक रसायन भी शामिल हैं। यदि इसमें आजकल तेज़ी से बढ़ रहे डायटीशियन के व्यवसाय को जोड़ लिया जाए तो इन चीज़ों की खपत का आंकड़ा बहुत अधिक है।
उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट खानपान के क्षेत्र में हुए परिवर्तन और शरीर की आवश्यकता पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि सभी अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन तत्वों के उपयोग पर पाबंदी लगाने की बात कही गई है जिनसे मृत्यु तक हो सकती है। दूसरी बात यह है कि यह काम इन वस्तुओं के उपयोग को सीमित करने से भी हो सकता है। इसके साथ ही बच्चों को ताज़ा दूध, फल, सब्ज़ी और अन्य खाद्य पदार्थ ही दिये जायें, इसकी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए। उनके लिए डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। पौष्टिकता के नाम पर उन्हें सेहत के लिए हानिकारक पदार्थ नहीं दिये जा सकते। इस बारे में देशव्यापी नीति और कानून बन सकते हैं ताकि बच्चे जब युवा हों तो उनके शरीर की संरचना ऐसी हो कि वे खानपान के कारण होने वाली बीमारियों से रक्षा के लिए अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर सकें।
मिलावट और नकली खाद्य पदार्थ
खाद्य सुरक्षा से जुड़ा एक और विषय है जो खाने पीने की चीज़ों में की जाने वाली मिलावट से जुड़ा है। यह बहुत गम्भीर है और समाज इसके प्रति अक्सर नर्म रुख अपनाता है क्योंकि उसे मिलावट करने वालों से जो कानूनी सुरक्षा मिलनी चाहिए, वह लगभग नदारद है। मिलावटियों को केवल साधारण जुर्माना या थोड़ी सी कैद दी जा सकती है जबकि यह इतना गम्भीर अपराध है कि इन्हें मृत्यु दंड या आजीवन कारावास मिलना चाहिए। वर्तमान कानून इतने कमज़ोर हैं कि उनका उल्लंघन करना बाएं हाथ का खेल है। उनका न तो सामाजिक बहिष्कार होता है और न ही न्यायालय उचित दण्ड दे पाते हैं। मिलावट कहीं भी की जा सकती है। खेतीबाड़ी, पशु पालन, दूध और उससे बने पदार्थ और यहां तक कि अंडे, मांस, मछली और पेड़ों पर लगने वाले फल तक मिलावटी हो सकते हैं। हालांकि फूड सेफ्टी का नियम और कानून है, लेकिन उसकी परवाह कौन करता है, यह किसी से छिपा नहीं है।