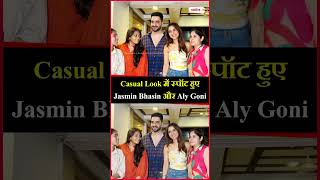दहेज प्रथा अभी भी सामाजिक द़ाग
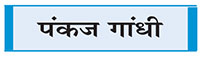
आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस की बात करने और दुनिया में तीसरी अर्थव्यवस्था की राह पर चलने वाले देश में हाल ही में एक वाक्य ने मुझे काफी निराश किया। इस वाक्य के दौरान यह देखकर मुझे गहरी निराशा हुई कि गुलामी से मुक्ति और विकसित भारत का दावा भरने के बावजूद हमारे समाज ने दहेज़ को लेकर उतनी उन्नति नहीं की है। इस वाक्य के दौरान मैं एक टीचर की लड़की से मिला व यह सुनकर हैरान था कि उसके शादी को 28 साल होने को आये लेकिन उसके ससुराल में उसके सास ससुर, देवर देवरानी द्वारा अभी भी शादी में मिले उपहारों को लेकर उसे हेय दृष्टि से देखते हैं और उसे अक्सर अपने और अपने पिता और परिवार के बारे में अपमानजनक शब्द और ताने सुनने पड़ते हैं। पति तो उसके साथ है लेकिन आज भी उसके बाकी के ससुराल वाले उसे दरिद्र की बेटी कहते हैं क्योंकि उस बहु ने बाकी बहुओं के मुकाबले कम सामान लाया था। यह बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक हालात हैं। अगर इस तरह के समाज के कीड़े शिक्षा में इतनी प्रगति के बावजूद भी मौजूद हैं तो इन कीड़ों से मुक्ति नहीं पाई जा सकती, इसके लिए लंबे सामाजिक प्रयास और कानूनी प्रयास एक साथ करने पड़ेंगे। महिला तानों का स्तर इतना गिरा रहता है जिसका उल्लेख यहां करना उचित नहीं है।
यह बातें इसलिए यहां लिख रहा हूं कि इस पर आर्थिक और सामाजिक समाजशास्त्रीय विश्लेषण हो सके। मेरा मानना है कि सबसे पहले तो ऐसी महिलाओं को आगे आकर बोलने के लिए साहस देना पड़ेगा। पुलिस के पास बेखौफ जाएं इसके लिए उन्हें साहसी बनाना पड़ेगा, सरकार को ओपन अप या स्पीक अप का अभियान चलाना पड़ेगा। यह आर्थिक और सामाजिक समस्या का समाधान एक लंबा सामाजिक और कानूनी अभियान मांगता है लेकिन तत्काल में महिलाओं को इसके लिए खुलकर आगे आने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। संचार के इस आधुनिक युग में ऐसे कई माध्यम हैं जहां वो अपनी बातों को रिकॉर्ड कर सकती हैं, बता सकती हैंए शिकायत कर सकती हैं और पुलिस के पास जा सकती हैं। ऐसी महिलाओं को तो सबसे पहले अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करना चाहिए। यह जागरूकता लानी पड़ेगी जो आगे चलकर उनके सुरक्षा सहित कानूनी उपाय के लिए भी काम आ सकता है। ओपन अप या स्पीक अप अभियान के साथ दस्तावेजीकरण के लिए राइट अप अभियान को भी सरकार को बढ़ावा देना पड़ेगा।
सरकार और स्थानीय प्रशासन को इसमें बड़ी पहल लेनी पड़ेगी क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और यह जल्दी से पटल पर नहीं आती हैं। समाज में दहेज प्रथा सदियों पुरानी और गहरी जड़ें जमाए हुए प्रथा है जो आज कालक्रम में बदरंग हो दाग बन गया है। इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें और महत्वपूर्ण कानूनी निहितार्थ हैं। यह प्रणाली सदियों में विकसित हुई और गहन कानूनी आयामों के साथ जटिल सांस्कृतिक पेचीदगियों को भी प्रदर्शित करती है। इस परंपरा की उत्पत्ति ऐतिहासिक सामाजिक-आर्थिक संरचनाओं में देखी जा सकती है, जहां शुरू में दहेज का उद्देश्य दुल्हन के लिए उसके नए वैवाहिक घर में वित्तीय सुरक्षा के रूप में काम करना था।
भारत में इससे निपटने के लिए विभिन्न कानूनी उपाय पेश किए गए। 1961 का दहेज निषेध अधिनियम इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने दहेज देना और लेना दोनों को दंडनीय अपराध बना दिया। हालांकि इस तरह के कानूनी हस्तक्षेप के बावजूद, दहेज प्रथा समाज के कुछ हिस्सों में बनी हुई है। यह प्रथा व्यापक सामाजिक गतिशीलता को प्रभावित करती है और महिला और उसके मायके के परिवार के आत्मसम्मान को चूर-चूर करती है। यह इस धारणा को बल देता है कि एक महिला का मूल्य उसकी क्षमताओं, चरित्र या उपलब्धियों के बजाए उसके भौतिक योगदान से निर्धारित होता है। न्यायपूर्ण उद्देश्य से शुरू की गई यह प्रथा आज महिला के अस्तित्व को नकारने के रूप में उभर कर सामने आ रही है। समय के साथ दहेज़ प्रथा के कई तरह के नकारात्मक परिणाम सामने आये हैं जिसमें हत्या, मानसिक शोषण और यहां तक कि आत्महत्या जैसे अपराध भी शामिल हैं। दहेज प्रथा के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और कानूनी आयाम हैं जो सदियों से विकसित हुए हैं। जो मूल रूप से ‘स्त्रीधन’ जैसी प्रथाओं से उपजा था लेकिन यह दुल्हन के परिवार से पर्याप्त धन हस्तांतरण की अपेक्षा में बदल गया। दहेज निषेध अधिनियम जैसे कानूनी उपायों का उद्देश्य इसके नकारात्मक परिणामों को रोकना है लेकिन इसके प्रभाव को पूरी तरह से खत्म करने में चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।