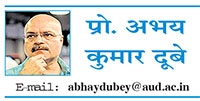जातिगत जनगणना का लाभ किसको होगा ?
जाति के प्याले में एक बार फिर से तूफान आ गया है। इस तूफान से नुकसान किसका होगा? भाजपा का या कांग्रेस और सामाजिक न्याय की पार्टियों का? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं है। क्या इस तूफान से जातिगत समाज तिनके की तरह उड़ जाएगा, या पहले आये कई तरह के तूफानों की तरह यह भी गुज़र जाएगा, और जाति अपनी जगह पहले की ही तरह खड़ी रह जाएगी?
जब से भारत ने खुद को आधुनिक बनाने की ठानी है, तभी से वह जाति को खत्म करने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। विचारधारा कोई भी हो, राजनीति कोई भी हो, जाति को हर कोई ऐसे विकट दुश्मन की तरह देखता है जो पराजित हो कर इतिहास के कूड़ेदान में जाने के लिए तैयार नहीं है। मार्क्सवादी जाति की जगह सामाजिक-आर्थिक वर्ग की स्थापना का आग्रह करते हैं। समाजवादियों का नारा जाति को तोड़ने का था। सावरकर ने ‘जातिबंदी’ की थीसिस दी थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शाखा के भीतर जातिगत दावे को नहीं स्वीकारता। आम्बेडकर ने ‘जाति के वध’ का आह्वान किया था। फुले और पेरियार जैसे सुधारक सारी ज़िंदगी जाति के खिलाफ संघर्ष करते रहे। भारत की वैज्ञानिक और आर्थिक प्रगति पर्याप्त न हो पाने का कारण भी जाति में खोजा जाता है। आरोप है कि जाति के कारण काम करने वाला हाथ और सोचने वाला सिर अलग-अलग हो गया। 19वीं और 20वीं सदी के ज्यादातर हिस्सों में हमारे राष्ट्रनायक जाति की संस्था पर कोड़े बरसाते रहे हैं। जाति को खत्म करने या कमज़ोर करने की सर्वथा नयी विधि ‘जातियों की जनगणना’ के रूप में सामने आयी है। पिछले डेढ़ साल से कांग्रेस इसकी मांग कर रही थी। अब सरकारी पार्टी भाजपा ने भी अपना हीलाहवाला छोड़ कर इसकी घोषणा कर दी है।
खास बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले तक जातिगत जनगणना की मांग करने वालों को भाजपा तालिबानी, जातिवादी हथकंडा, हिंदू समाज का दुश्मन, दलितों का आरक्षण छीनने की यादवी साजिश वगैरह बता रहे थे। पहलगाम के आंतकवादी खूनखराबे के तुरंत बाद भाजपा के छत्तीसगढ़ हैंडिल से एक कार्टून प्रसारित हुआ था जिसमें टिप्पणी की गई थी कि जाति पूछ कर नहीं बल्कि धर्म पूछ कर गोली मारी गई है। ज़ाहिर है कि भाजपा का लक्ष्य हिंदू एकता है, और वह जातिगत जनगणना को अपने इस लक्ष्य के लिए बाधक मानती है। लेकिन, यह एक विरोधाभास ही है कि जो संघ शाखा में जाति को नहीं चलने देता, वह अपने स्वयंसेवकों के शाखा से बाहर के सामाजिक जीवन में जातिगत होने या जातिवादी होने पर आपत्ति नहीं करता। नतीजा यह निकलता है कि हिंदू एकता के पैरोकार गर्व से अपनी जातिगत पहचान सीने पर लगाये घूमते रहते हैं।
बहरहाल, अगर भाजपा के नज़रिये से देखें तो समझा यह जा रहा है कि जब जनगणना के ज़रिये सारे देश में 1300 जातियों (सरकार जातियों की संख्या इसके आगे ले जाने के पक्ष में नहीं है) के रूप में पूरी आबादी का संख्यात्मक नक्शा बन जाएगा, तो वे बड़ी-बड़ी जातिगत पहचानें अपनी जगह से हिल जाएंगी जो आज़ादी के बाद चुनावी राजनीति के हाथों तैयार हुई हैं। यानी, जैसे ही छोटी-बड़ी जातियों को अपनी-अपनी संख्याएं पता चलेंगी, वे बड़ी जातियों से सत्ता-शिक्षा-नौकरी से संबंधित लाभों के लिए संख्या-आधारित प्रतियोगिता करने लगेंगी। भाजपा को उम्मीद है कि इस चक्कर में दक्षिण भारत की सबसे बड़ी द्रविड़ पहचान में दरार पड़ सकती है। शक्तिशाली यादव समुदाय द्वारा ओबीसी एकता की दावेदारियां सांसत में आ जाएंगी। जाटव समुदाय द्वारा अपने नेतृत्व में दलित एकता करने के प्रयास कुंठित हो जाएंगे। भाजपा को शायद यह भी लग रहा है जब मुसलमानों में अजल़ाफ (ओबीसी) और अरज़ाल (दलित) जातियां गिन ली जाएंगी तो उंगलियों पर गिनने लायक भाजपा विरोधी अशराफ (ऊंची जातियां) नेतृत्व को बेअसर किया जा सकेगा। इस तरह पसमांदा मुसलमानों को भाजपा की तरफ खींचे जाने की संभावना खुल जाएगी।
विपक्ष के दृष्टिकोण से देखें तो जातिगत जनगणना ऊंची जातियों को उनकी असली शक्ल दिखा देगी। यह साबित हो जाएगा कि संख्या में मुट्ठी-भर होने के बावजूद वे सत्ता और उत्पादन के बड़े से बड़े हिस्से का उपभोग कर रही हैं। उत्तर, मध्य और पश्चिमी भारत में ऊंची जातियों के मतदाता भाजपा के जेबी वोटर बन चुके हैं, इसलिए जातिगत जनगणना ओबीसी और दलित मतों के सामने एक नया सामाजिक-आर्थिक यथार्थ पेश कर देगी। वह उन्हें ब्राह्मण-ठाकुर-बनिया-भूमिहार-कायस्थ वगैरह से जुड़ कर वोट देने से रोक सकता है। विपक्ष मुसलमानों में पसमांदा और ़गैर-पसमांदा के विभाजन से चिंतित नहीं है। वह मानता है कि मज़हबी एकता इस बंटवारे से खुद निबट लेगी। यानी, विपक्ष को लगता है कि भाजपा के मुकाबले पिछड़े-दलितों और मुसलमानों की एकता को जातिगत जनगणना और मज़बूत करेगी। हिंदू राजनीतिक एकता का स्वप्न भंग हो जाएगा।
इन राजनीतिक प्रत्याशाओं पर ़गौर करें तो स्पष्ट हो जाता है कि जातिगत जनगणना से जिस जाति के कमज़ोर होने की उम्मीद की जा रही है, वह पुराने ढंग की कर्मकांडीय पेशा-आधारित जाति नहीं है। दरअसल, वह पुराने किस्म की जाति अगर कहीं है तो व्यक्तिगत दायरे में सिमटी हुई है। सार्वजनिक जीवन में केवल दलितों पर अत्याचारों के रूप में ही अपनी शक्ल दिखाती है। जातियों की जिस भूमिका और संरचना में यह जनगणना उथलपुथल मचाएगी, वह तो अपने किरदार में आधुनिक और राजनीतिक है। इस बात को शायद सबसे ज्यादा स्पष्ट रूप से कांशीराम समझते थे। इसीलिए अम्बेडकरवादी होते हुए भी वे जाति को कमज़ोर करने या नष्ट करने के चक्कर में नहीं पड़े। उन्होंने तर्क दिया कि जाति जितनी मज़बूत होगी, उनकी राजनीति उतनी ही परवान चढ़ेगी।
इससे यह भी स्पष्ट होता है कि साठ के दशक के आखिर में की गई प्ऱोफेसर रजनी कोठारी की भविष्यवाणी अब रंग ला चुकी है। उन्होंने जाति और राजनीति के संबंधों पर ़गौर करते हुए कहा था कि जातियां आधुनिक राजनीति में भागीदारी करने के दौरान बदल जाती हैं। सार्वजनिक जीवन में उन्हें अपने कर्मकांडीय दायरे का अतिक्रमण करना पड़ता है। उनकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। कोठारी को जातिप्रथा के क्रांतिकारी ध्वंस की कोई ़गलत़फहमी नहीं थी। इसलिए उन्होंने निष्कर्ष यह निकाला कि राजनीति में जातिवाद नहीं है, बल्कि जातियों का राजनीतिकरण हो गया है। इस लिहाज़ से जातिगत जनगणना न तो जातियों को तोड़ेगी, न उनके प्रभाव का क्षय करेगी। वह तो पहले ही राजनीति में जम कर भागीदारी कर रही है, गठजोड़ बना रही है, दलबंदियां कर रही है, गोलबंदी का औज़ार बनी हुई है। जाति अपने कर्मकांडीय स्वरूप में जितनी है, उतनी निजी स्तर पर बनी रहेगी। जनगणना ज्यादा से ज्यादा उसके आधुनिक को ही प्रभावित कर सकती है। पिछड़ी, दलित और मुसलमान जातियों के संदर्भ में वह संख्याबल में कमज़ोर जातियों को संख्याबहुल जातियों से लाभों में वास्तविक साझेदारी की मांग करने की तरफ ले जाएगी। लेकिन ऊंची जातियों को उनकी अधिक स्थायी और सबल मोर्चेबंदी का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला कर जनगणना से वे प्रक्रियाएं और मज़बूत होंगी जो आज़ादी के बाद से ही चल रही हैं।
लेखक अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली में प्ऱोफेसर और भारतीय भाषाओं के अभिलेखागारीय अनुसंधान कार्यक्रम के निदेशक हैं।