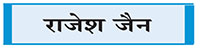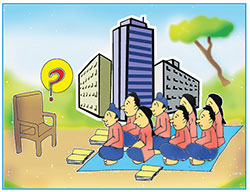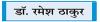देश में शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की ज़रूरत
किसी देश का भविष्य उसके नागरिकों की सोच पर निर्भर करता है और सोच बनती है शिक्षा से। शिक्षा किसी समाज को सिर्फ पढ़ा-लिखा ही नहीं बनाती, बल्कि सोचने, समझने और चुनने की क्षमता भी प्रधान करती है। यही क्षमता व्यक्ति को अंधविश्वास से बाहर लाती है, लोकतंत्र को मज़बूत करती है और अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाती है।
अगर इतिहास पर नज़र डालें तो हर विकसित देश की जड़ में शिक्षा ही रही है। जापान, दक्षिण कोरिया, फिनलैंड, जर्मनी और सिंगापुर जैसे देशों ने युद्धों और संकटों के बाद खुद को शिक्षा के बल पर ही खड़ा किया। भारत में भी जब स्वतंत्रता आंदोलन चला, तब महात्मा गांधी, टैगोर, डा. अम्बेडकर और पंडित नेहरू जैसे नेताओं ने स्पष्ट कहा था कि शिक्षा स्वतंत्र भारत की रीढ़ होगी। उनका मानना था कि जब कोई सरकार या परिवार शिक्षा पर पैसा खर्च करता है, तो वह किताबें नहीं, बल्कि बेहतर भविष्य खरीद रहा होता है। एक शिक्षित व्यक्ति न सिर्फ अपने परिवार की आय बढ़ाता है, बल्कि समाज के लिए नवाचार और नैतिक चेतना लाता है। इसलिए एक शिक्षक को अच्छा वेतन देना, गांव में स्कूल बनाना या डिजिटल लैब खोलना आदि ये सब व्यय नहीं, बल्कि निवेश है, जो आने वाले वर्षों में देश को फल देता है।
यह सही है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था पर सवाल बहुत उठते हैं, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पिछले दशकों में हमने इस क्षेत्र में कई अहम उपलब्धियां हासिल हुई हैं। आज भारत के लगभग हर गांव में प्राथमिक विद्यालय हैं। सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे-मील योजना और शिक्षा का अधिकार जैसे कार्यक्रमों ने लाखों बच्चों को स्कूल तक पहुंचाया है। 1951 में जहां साक्षरता दर केवल 18 प्रतिशत थी, वह आज 77 प्रतिशत से ऊपर है। देश में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी और आईआईएसईआर जैसे संस्थानों ने भारत की शिक्षा को वैश्विक पहचान दी है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उच्च-शिक्षा नेटवर्क रखता है। नई शिक्षा नीति ने अब 10+2 की जगह 5+3+3+4 की संरचना दी है, जो बच्चों की शुरुआती शिक्षा, मातृभाषा और व्यावहारिक ज्ञान पर केंद्रित है। डिजिटल शिक्षा के क्षेत्र में दीक्षा, स्वयम और ई-पाठशाला जैसे सरकारी प्लेटफॉर्म नई दिशा दे रहे हैं।
सफलता की यह कहानी अधूरी है क्योंकि कागज़ी वादों और ज़मीनी हकीकत के बीच अब भी बड़ा अंतर है। सरकारें वायदे अधिक करती हैं, परन्तु निवेश कम करती हैं। 1968 की शिक्षा नीति में कहा गया था कि केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च होना चाहिए जबकि 2020 की नीति में कहा गया कि देश की जीडीपी का 6 प्रतिशत शिक्षा पर निवेश किया जाए।
सुनने में दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन अंतर बड़ा है। केंद्रीय बजट का 6 प्रतिशत मतलब सरकार के वार्षिक खर्च का 6 प्रतिशत तो दूसरी ओर जीडीपी का 6 प्रतिशत मतलब पूरे देश की आर्थिक उत्पादन क्षमता का 6 प्रतिशत। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। आज भारत मुश्किल से जीडीपी का 3 प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च कर पा रहा है।
बच्चे स्कूल तो जा रहे हैं लेकिन क्या वे सीख रहे हैं? एएसइआर रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत के 50 प्रतिशत बच्चे पांचवीं में होकर भी तीसरी की किताब नहीं पढ़ पाते। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा ध्यान बच्चे स्कूल में हैं या नहीं पर है, वे क्या सीख रहे हैं, इस पर नहीं।
देश में लगभग 10 लाख शिक्षकों की कमी है। जो मौजूद हैं, उन्हें अधिकतर को आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण नहीं मिल पा रहा। शहरों के बच्चे ऑनलाइन क्लास में होते हैं, लेकिन गांव के बच्चे मोबाइल सिग्नल ढूंढते फिरते हैं। डिजिटल शिक्षा का फायदा उन्हीं को मिला या मिल रहा है जिनके पास उपकरण और इंटरनेट था, जिससे शिक्षा में असमानता और बढ़ गई। एआई और तकनीक के युग में भी अंकों को ही बुद्धिमत्ता का पैमाना माना जा रहा हैं। हमारे बच्चे सोचते-समझते नहीं, बस रटते हैं। परीक्षा की चिंता ने शिक्षा को जीवन से काट दिया है।
फिनलैंड में बच्चों को 7 साल की उम्र तक औपचारिक पढ़ाई में नहीं डाला जाता। कोई बोर्ड परीक्षा नहीं, कोई रैंकिंग नहीं, है तो बस सीखने की खुशी। शिक्षक वहां समाज का सबसे सम्मानित वर्ग है। सिंगापुर में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को समान दर्जा दिया गया है। वहां शिक्षा रोज़गार की सीढ़ी नहीं, कौशल की यात्रा है। भारत भी अगर कौशल विकास को शिक्षा से जोड़ा जाए तो बेरोज़गारी कम हो सकती है। दक्षिण कोरिया जो 1950 के दशक में लगभग अनपढ़ देश था, आज तकनीकी महाशक्ति है। उसने जीडीपी का बड़ा हिस्सा शिक्षा और अनुसंधान पर लगाया। भारत को भी रक्षा या सब्सिडी जितना खर्च शिक्षा पर करना होगा।
कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने शिक्षा को बहुभाषी और लचीला बनाया। छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता दी। भारत में भी अब समय आ गया है कि आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की दीवारें तोड़ दीं जाएं। अगर सचमुच चाहते हैं कि शिक्षा का उजास देश के हर कोने तक पहुंचे, तो सरकार को अब घोषणाएं नहीं, ठोस कदम उठाने होंगे। शिक्षा पर खर्च बढ़ाया जाए। (युवराज)