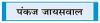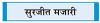अमरीकी ‘टैरिफ’ का सामना करने के लिए भारत की नीति क्या हो ?
जोश ना हो तो जवानी का मतलब क्या है,
होश खो जाए तो दानाई भी खो जाती है।
अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत टैरिफ तथा 25 प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ बढ़ाने की घोषणा पर भारत ने तीव्र प्रतिक्रिया दी है। बेशक यह ट्रम्प की भारत को प्रत्यक्ष रूप में ब्लैकमेल करने की कोशिश भारत को चीन तथा रूस के खेमे की ओर झुकने के लिए मजबूर कर रही है, परन्तु हम नहीं समझते कि भारत का इस प्रकार किसी एक खेमे में जाना भारत के लिए लाभदायक सौदा है। हां, भारत का अमरीकी धौंस के आगे झुकना भी उचित नहीं। ऐसे अवसर जोश के साथ-साथ होश से काम लेने के होते हैं, क्योंकि रूस के साथ दोस्ती के अर्थ अलग हैं और चीन के साथ दोस्ती के अर्थ बिल्कुल ही अलग हैं। चीन पर भरोसा करना, अमरीका पर भरोसा करने से भी खतरनाक है। चीन कभी भी विश्वसनीय दोस्त नहीं रहा। उसकी विस्तारवादी नीति उसके प्रत्येक दोस्त देश को महंगी ही पड़ी है, परन्तु भारत का अनुभव तो बहुत कड़वा है।
1962 में ‘हिन्दी चीनी भाई-भाई’ को हमने देखा है और चीन के प्रमुख शी जिनपिंग के भारत दौरे के बाद की स्थिति भी हमारे सामने ही है। फिर यदि हम चीन आधारित आर्थिकता की ओर बढ़े तो यह हमारे लिए एक आत्मघाती कदम ही सिद्ध होगा, क्योंकि एक तो हमारा चीन के साथ सीधा सीमांत विवाद है। दूसरा, तिब्बत तथा उत्तर-पूर्व के क्षेत्रों पर विवाद है, परन्तु सबसे बड़ी बात है कि हम पाकिस्तानी कब्ज़े वाले कश्मीर को अपना अंग मानते हैं और उसके बहुत-से हिस्से पर पाकिस्तान की मज़र्ी से चीन काबिज़ हो चुका है, परन्तु सीमांत विवाद की बात न भी करें तो व्यापारिक पक्ष से भी चीन अमरीका तथा यूरोप का विकल्प नहीं बन सकता, क्योंकि चीन हमारे सामान का खरीददार नहीं, आपूर्तिकर्ता है। वर्ष 2024-25 में हमने चीन से 113.45 अरब डॉलर का सामान खरीदा और उसे सिर्फ 16.66 अरब डॉलर का सामान बेचा है जबकि इसके विपरीत हमने इसी समय दौरान अमरीका को 87.4 अरब डॉलर का सामान बेचा और उससे 41.8 अरब डॉलर का सामान खरीदा है। हमारा शुद्ध व्यापार लाभ 45.7 अरब डॉलर का है। यदि हमने अपनी आर्थिकता चीन से सहारे खड़ी करने का कोशिश करेंगे तो चीन तो उलटा भारत में अपना बहुतायत वाला सामान भेज कर डम्ंिपग स्टेट ही बना देगा। भारत की ज़रूरत चीन की तरह ही एक विश्व निर्माण हब बनने की है जो चीन के साथ सीधा टकराव है। फिर सैन्य और दोस्ती के मामले में चीन की ‘स्ंिट्रग ऑफ पर्ल्स’ नीति प्रत्यक्ष रूप में भारत विरोधी नीति है। हम इसके मुकाबले ‘नैकलैस ऑफ डायमंड्स’ तथा ‘नेबर फर्स्ट’ नीतियां बनाते हैं और इसी खतरे से बचने के लिए ही ‘क्वाड’ का हिस्सा हैं।
इसलिए यह समय सिर्फ जोश का नहीं, होश से काम लेने का भी है। जल्दबाज़ी में किसी और देश की ओर झुक जाना या अमरीका की आगे आत्म-समर्पण कर देना, दोनों स्थितियां देश हित में नहीं हैं। भारत के लिए यह तलवार की धार पर संतुलन बना कर चलने का समय है। यदि सम्भव हो तो भारत को एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू वाले निर्गुट आन्दोलन (नॉन अलायनमैंट मूवमैंट) को चलाने की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि हमारी ‘सबसे दोस्ती’ की नीति तो स्पष्ट रूप में विफल हो चुकी है।
जहां तक रूस से सस्ता तेल खरीदने की बात है, भारत को भारतीय लोगों के लिए सस्ता तेल खरीदने का अधिकार है, परन्तु सिर्फ अम्बानी, अडानी तथा नायरा जैसे कार्पोरेटरों के लाभ के लिए अमरीका से दुश्मनी करना किसी तरह भी देशहित में नहीं। हमारे सामने है कि गौतम अडानी ने अडानी पोर्ट्स के कार्यकारी अध्यक्ष के पद से इस्तीफा उस समय दिया है जब अमरीका में अडानी की मुद्रा पोर्ट पर ईरान से आए तेल तथा गैस का मामला उभरा है। यहां एक बात और दावे से कहने का साहस कर रहा हूं कि बेशक अमरीका ने अपने मित्र यूरोपियन देशों पर भी टैरिफ लगाया है और उन्हें रक्षा खर्च बढ़ाने के लिए भी मजबूर किया है, परन्तु यह निश्चित है कि इसके बावजूद यूरोपियन तथा पश्चिमी देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अमरीका से ज़्यादा बाहर नहीं जाएंगे और विशेषकर रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वे अमरीका से अधिक रूस विरोधी ही रहेंगे। भारतीय कम्पनी ‘नायरा एनर्जी’ पर सबसे पहला प्रतिबंध यूरोपियन यूनियन ने ही लगाया है। इसलिए यदि भारत पूरी तरह रूसी-चीनी खेमे में चला गया तो निश्चित है कि भारत अमरीका के बाद यूरोपियन देशों से भी अलग-थलग पड़ने लगेगा।
हम समझते हैं कि अभी भी भारत अमरीका के साथ समझौता करने के समर्थ है। हमें उम्मीद है कि आगामी दिनों में यह हो ही जाएगा। भारत तथा अमरीका एक-दूसरे के विरुद्ध दुश्मनी वाली पोस्चरिंग अर्थात झूठी छवि बनाने तथा दिखाने की रणनीति अपने हितों को सुरक्षित रखने की कोशिश है, क्योंकि न तो अमरीका के यह हित में है कि भारत जैसा 144 करोड़ की आबादी वाला देश उसके स्थायी विरोधियों के ग्रुप में जा बैठे, और न ही यह भारत के पक्ष में है कि अमरीका के साथ-साथ उस देश के सहयोगी पश्चिमी देशों तथा आस्ट्रेलिया एवं न्यूज़ीलैंड जैसे देशों तथा जापान से अपने संबंध बिगाड़ ले। भारत तो बीच में फंसा हुआ है।
इस तऱफ बहिर-ए-अज़ल है,
उस तऱफ बहर-ए-रसातल
पुल-सिरातों से गुजरना
आसां भी होता कहां है।
-लाल फिरोज़पुरी
1. बहर-ए-अज़ल = मौत का समुंदर , 2. रसातल = पाताल या निचला स्तर , 3. पुल-सिरात = बाल से बारीक पुल जैसा स्वर्ग का रास्ता
अमरीकी दबाव के आगे झुके तथा अडिग प्रमुख देश
हालांकि ट्रम्प ने 31 जुलाई को लगभग 100 देशों पर टैरिफ लगाया था, परन्तु जिन देशों ने उसके साथ, समझौता या डील कर ली, उन पर 9 प्रतिशत से 20 टैरिफ रह गया है, परन्तु जिन देशों ने समझौता नहीं किया उन पर टैरिफ की दर 21 से 50 प्रतिशत रखी गई है। पाकिस्तान जिस पर पहले 29 प्रतिशत टैरिफ था, अब 19 प्रतिशत कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि अमरीका ने ब्रिटेन पर टैरिफ 41 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया है, परन्तु इस देश के लिए स्टील तथा एल्युमीनियम पर अभी भी 25 प्रतिशत टैरिफ है। बदले में ब्रिटेन ने अमरीकी बीफ तथा एथानोल को टैक्स मुक्त कर दिया है। कई अन्य वस्तुओं पर टैक्स कम करने का वायदा किया है।
जापान का टैरिफ भी 25 प्रतिशत से कम करके 15 प्रतिशत किया गया है। बदले में जापान ने अमरीका में 45 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने तथा 100 बोईंग विमान खरीदने का वादा किया है। उसने अपना रक्षा बजट खर्च बढ़ाने का फैसला भी किया है।
यूरोपीय यूनियन पर अमरीका का टैरिफ 30 प्रतिशत था, जो अब कम होकर 15 प्रतिशत किया गया है। यूरोपीय यूनियन बदले में 64 लाख करोड़ की एनर्जी की खरीद करेगा तथा 51 लाख करोड़ रुपये अमरीका में निवेश करेगा।
इंडोनेशिया का टैरिफ 32 प्रतिशत से कम करके 19 प्रतिशत किया गया है। बदले में इंडोनेशिया 99 प्रतिशत वस्तुओं का प्रवेश मुक्त करने की अनुमति देगा।
दक्षिण कोरिया का टैरिफ 25 से 15 प्रतिशत किया गया है। वह अमरीका में 350 अरब डॉलर का निवेश करेगा, 100 अरब डॉलर की एनर्जी खरीदेगा, परन्तु चावल तथा बीफ बेचने की अनुमति नहीं देगा।
इसके विपरीत भारत कृषि, डेयरी, पोल्ट्री, खुदरा बाज़ार तथा लघु उद्योगों से तैयार की जाने वाली वस्तुओं की अमरीका को भारत में आयात करने की आज्ञा नहीं देगा। जिस कारण अमरीका से समझौता लम्बित है, परन्तु अमरीका बहाना रूस से सस्ता तेल खरीदने को बना रहा है। हैरानी का बात है कि यह सस्ता तेल भारतीय लोगों को नहीं मिलता। इसका प्रत्यक्ष लाभ तो अम्बानी, नायरा तथा अडानी जैसों की निजी कम्पनियों को होता है, परन्तु नुकसान सारे भारतीयों को सहन करना पड़ेगा। यदि अमरीका के साथ कोई समझौता नहीं होता तो भारत को निर्माण हब बनने के लक्ष्य में बहुत बहुत भारी नुकसान हो सकता है। फाक्सकोन जैसी कम्पनियां भारत छोड़ कर किसी कम टैरिफ वाले देश की ओर जा सकती हैं। हमें व्यापार घाटे से अधिक नुकसान रोज़गार के क्षेत्र में हो सकता है। भारत पश्चिमी लॉबी में अलग-थलग पड़ सकता है और अमरीका में नौकरी करते लाखों भारतीयों मे भी बेरोज़गार होने का भय उत्पन्न हो सकता है।
चीन टैरिफ वार में अमरीका के आगे नहीं झुका, परन्तु चीन का अमरीका के बिना काम चलता है। वह जो उत्पादन करता है, उसमें से बहुत कुछ ऐसा है जो अभी अमरीका तथा पश्चिमी देशों द्वारा खरीदना उनकी मजबूरी है जबकि ब्राज़ील, कनाडा तथा दक्षिण अफ्रीका भी अमरीका के आगे अडिग हैं और वे 50, 35 तथा 31 प्रतिशत टैरिफ सहन कर रहे हैं, परन्तु उनकी भौगोलिक तथा आर्थिक स्थिति भारत से बहुत अलग है।
भारत क्या करे?
इस समय भारत को अमरीका के साथ चल रही बातचीत खत्म नहीं करनी चाहिए, अपितु बातचीत ही प्रत्येक समस्या का अंतिम समाधान होती है। भारत को फिर से नान अलायंस (निर्गुट आन्दोलन) की ओर लौटना चाहिए, क्योंकि भारत की ‘सच से दोस्ती’ की नीति बुरी तरह विफल हो चुकी है। भारत को निर्माण इकाइयों विशेषकर लघु उद्योगों को विशेष पैकेज देने चाहिएं। निर्यात सुविधाएं चीन की तरह ही देनी पड़ेंगी। भारत विश्व व्यापार संगठन में मुद्दा उठा सकता है। अमरीका के मित्र देशों जो भारत के भी मित्र हैं, का समर्थन हासिल करना चाहिए। विशेषकर अमरीका में बहुत ही मज़बूत ‘यहूदी लॉबी’ को इज़रायल के माध्यम से भारत के पक्ष में दबाव बनाने के लिए मनाना चाहिए। अमरीका में भारतीय लॉबी जो बहुत अधिक टैक्स अदा करती है, वह यहूदी लॉबी से मिल कर इस दबाव को बढ़ा सकती है। भारत निर्यात लागत कम करने तथा निर्यात सब्सिडी बढ़ाने की ओर ध्यान दे सकता है। सबसे अवश्यक बात आत्म-निर्भरता के लिए विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल सीमित किया जा सकता है और जवाबी टैरिफ लगाए जा सकते हैं।
-मो. 92168-60000