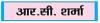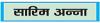प्राकृतिक आपदाएं : आधुनिक तकनीक से कम की जा सकती है क्षति

क्या बादल फटने की आपदा पर किसी का वश नहीं है? प्रकृति के इस कहर के आगे क्या सभी बेबस हैं और बचाव में कुछ किया ही नहीं जा सकता? क्या इसलिए हम केवल आपदा के बाद राहत बांटने तक सीमित रहेंगे? सच यह है कि विज्ञान और नव्यतम तकनीक के पास इसके नुकसान को न्यून करने, भविष्य सुरक्षित करने का रास्ता है और यही एकमात्र मार्ग है।
मानसून में पहाड़ी राज्यों से बादल फटने की खबरें आम हैं। इस आपदा के कई आशंकित क्षेत्र हैं- जैसे पश्चिमी घाट के कुछ हिस्से मसलन केरल, महाराष्ट्र और कभी-कभी झारखंड वगैरह परन्तु उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ये घटनाएं लगभग हर मानसून में नियमित हैं। उत्तर-पूर्वी भारत के अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड भी अकसर इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। दूसरे देश भी इस प्राकृतिक प्रकोप से अछूते नहीं हैं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक दशक में केवल उत्तराखंड और हिमाचल में ही 150 से अधिक बादल फटने की बड़ी विनाशक घटनाएं दर्ज की जा चुकी हैं। इनमें कभी पूरी बिजली परियोजना बह गई तो कभी सैकड़ों घर, समूचे गांव, होटल, सड़कें, पुल-पुलिया, पेड़ और सैकड़ों लोग भी। इस संदर्भ में भविष्य और भयावह दिखता है; क्योंकि एक तो यहां बादल फटने के और फ्लैश फ्लड के बाद नुकसान बढ़ाने वाले कारक अन्य जगहों की तुलना में अधिक हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का निष्कर्ष है कि हर साल इन घटनाओं की आवृत्ति और विनाशक क्षमता बढ़ती जा रही है। एक तो बादल फटनना अत्यंत आकस्मिक और अत्यधिक स्थानीय घटना है, जिस पर किसी का वश नहीं। दूसरे छोटे भौगोलिक क्षेत्र में मौसम का सटीक पूर्वानुमान कठिन है, लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं कि कुदरत के इस कहर के आगे सब बेबस हैं और बचाव में कुछ किया ही नहीं जा सकता। सच तो यह है कि विज्ञान और तकनीक की मदद तथा सरकार और जन-प्रयासों से, भले इसे पूरी तरह रोका न जा सके, लेकिन क्षति को अत्यधिक न्यून तो अवश्य किया जा सकता है।
नि:संदेह भविष्य में बादल फटने जैसी आपदा से निपटने का एकमात्र भरोसेमंद उपाय नई तकनीक का विकास और उसका सही उपयोग ही हो सकता है। रडार प्रणाली, सूचना-संचार प्रौद्योगिकी, उपग्रह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विभिन्न प्रकार के सेंसर, सैटेलाइट इमेजिंग और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी तकनीक इस क्षेत्र में तबाही से बचाव की मजबूत ढाल बन सकती हैं। जब जुलाई से सितम्बर के बीच हिमालयी क्षेत्रों में ऐसी घटनाओं की आशंका तयशुदा मानी जाती है। जब यह तथ्य स्थापित है कि इस दौरान लगभग 70 प्रतिशत बादल फटने की घटनाएं समुद्र तल से 1000-2000 मीटर ऊंचाई वाले इलाकों में होती हैं। जब यह भी स्पष्ट है कि कम मानसूनी वर्षा वाले क्षेत्रों में भीषण बारिश और बादल फटने की घटनाएं अधिक होती हैं, साथ ही नमी, ताप और वर्षा के समीकरणों का संबंध भी हम पहचान ही चुके हैं, तो फिर इन सबके पैटर्न और प्रभावित इलाकों का विश्लेषण कर आशंकित स्थानों को पहले से चिन्हित करना बहुत कठिन नहीं है। यदि ऐसे आशंकाग्रस्त स्थानों को पहचान कर वहां पहले से सचेत रहा जा सके तो आपदा से पहले और बाद में होने वाले नुकसान को न्यूनतम किया जा सकता है।
बेशक बादल फटने की घटना का घंटों पहले पूर्वानुमान और लम्बी अवधि की चेतावनी संभव नहीं है। फिर भी, आधुनिक रडार और सैटेलाइट तकनीक की मदद से एक-दो घंटे पहले इसकी आशंका का भान हो सकता है। हमारे पास उन्नत डॉप्लर वेदर रडार और इसरो के कई मौसम उपग्रह मौजूद हैं, जो भारी वर्षा और बादल बनने की स्थिति का पता लगाने में सक्षम हैं। इनके उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी से छोटे पैमाने पर बादलों की गतिविधि पर नज़र रखते हैं। किस क्षेत्र में बादल फटने की आशंका है, इसका अनुमान लगाते हैं और इन सबके विवेचन से कुछ घंटे पहले ही खतरे की चेतावनी देकर लोगों को आपदा स्थल से सुरक्षित निकाला जा सकता है। भारी वर्षा के पैटर्न, नमी और तापमान के रीयल-टाइम डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई )आधारित मॉडल अधिक सटीकता से मिनट-दर-मिनट दर्ज कर सकते हैं। इन आंकड़ों के विश्लेषण से संभावित खतरे का तत्काल पता लगाया जा सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग आधारित डेटा प्रोसेसिंग से तुरंत निर्णय लेने में बड़ी मदद मिलती है। अगर आशंकाग्रस्त हिमालयी क्षेत्रों के गांव-गांव में स्वचालित रेन-गेज नेटवर्क स्थापित किए जाएं, जिनमें ऐसे सेंसर हों, जो वर्षा का डेटा तुरंत केंद्रीय सर्वर को भेजें, तो स्थानीय स्तर पर चेतावनी जारी करने की क्षमता बढ़ेगी।
ड्रोन के ज़रिये जीआईएस मैपिंग करवा करके मानसून से पहले ही खतरे वाले गांवों को चिन्हित किया जा सकता है। इन्हीं से संवेदनशील ढलानों और नदियों के किनारों की बसाहट, मोड़ और अवरोध का नक्शा तैयार किया जा सकता है, जिससे फ्लैश फ्लड आने से पहले आगत समस्या का समाधान तलाशा जा सके। एआई और संचार तकनीक के इस युग में आसान है कि आशंकाग्रस्त क्षेत्रों में साइरन सिस्टम के अलावा ऐसे सामुदायिक रेडियो और मोबाइल एप विकसित किए जाएं, जो स्थानीय बोली-भाषा में चेतावनी प्रसारित करें। भारत के पास मौसम विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत ढांचा और तकनीक है। 37 डॉप्लर रडार हैं, बादलों की गति और नमी का रीयल-टाइम डेटा देने के लिए इसरो के उपग्रह हैं। 2 से 6 घंटे पहले ‘नाउकास्टिंग’ के जरिये अप्रत्याशित भारी वर्षा की चेतावनी दी जा सकती है। मोबाइल, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए सूचना प्रसारण की व्यवस्था भी है। फिर भी, 2021 में उत्तराखंड के रैनी हादसे के दौरान तकनीकी निगरानी के बावजूद विद्युत आपूर्ति बाधा के चलते अलर्ट गांवों तक नहीं पहुंचा। साल 2023 में हिमाचल के किन्नौर में बादल फटा तो वहां डॉप्लर रडार ही मौजूद नहीं था। जम्मू के किश्तवाड़ और कठुआ में मोबाइल नेटवर्क बाधित होने से अलर्ट का लाभ नहीं मिल पाया।
ये घटनाएं बताती हैं कि तकनीकी साधनों का होना और उनका कुशलता के साथ उचित प्रयोग दो अलग बातें हैं। हिमालयी राज्यों में डॉप्लर रडार लगाने की सरकारी योजना के बावजूद यहां कवरेज अत्यंत कम है। छोटे-छोटे अंतराल पर डॉप्लर रडार लगाने की आवश्यकता है। मिनी-रडार और पोर्टेबल रडार तकनीक से दूरदराज़ क्षेत्रों को भी कवर किया जा सकता है। वैसे भी केवल पारम्परिक रडार और उपग्रह पर्याप्त नहीं। उन्नत तकनीक की ओर बढ़ना होगा—जैसे आपदा में बिजली गुल होने पर मोबाइल अलर्ट न रुके, इसके लिए सैटेलाइट-आधारित संचार का विकल्प देना होगा। एनडीएमए की गाइडलाइंस हैं ज़रूर, लेकिन आमजन को इनकी जानकारी नहीं। ग्राम समितियों और स्कूलों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण सुस्त है, तो जल-निकासी योजनाएं और सुरक्षित आश्रय स्थल नगण्य।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर