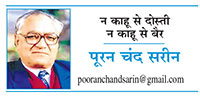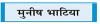भारतीय अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं लघु उद्योग
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस पर विशेष
प्रति वर्ष 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाने की याद 25 साल पहले आई थी। तब से इसकी लकीर पीटने के कार्यक्रम होते हैं जिनका कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलता, परिणामस्वरूप छोटे उद्योग घट रहे हैं। लोग बेरोज़गार होने के कारण बड़े उद्योगों में नौकरी, चाहे कैसी भी हो, करने के लिए विवश हैं, ताकि गुज़ारे के योग्य वेतन मिल जाए। इसके लिए क्या कोई व्यक्ति, दल, संस्था, सरकार या बिचौलिये जिम्मेदार हैं, इसकी पड़ताल करनी आवश्यक है जिससे इस मज़र् की दवा खोजी जा सके।
अमीरी और गरीबी का बढ़ते रहना : इसे समझने के लिये लिए महात्मा गांधी की ओर लौटना होगा। जब वह विदेश से भारत आये और पूरे देश का चक्कर लगाने निकल पड़े तो उनको समझ में आ गया कि भारत की समस्या और उसका मूल कारण यह है कि अधिकतर लोगों के पास रोटी, कपड़ा और मकान नहीं है जबकि मुट्ठी भर साहूकारों, ज़मींदारों और व्यापारियों के पास उनकी सात पुश्तों तक के लिए पर्याप्त धन है। उन्होंने इस बात को समझते हुए चरखे को घर-घर पहुंचाने का रास्ता चुना। इससे तन ढंकने को कपड़ा, अतिरिक्त सूत बेचकर भोजन का जुगाड़ और घास फूस की झोंपड़ी खड़ी करने की व्यवस्था की जा सकती है। इसके बाद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय उत्पादों से कोई लघु उद्योग शुरू करने की योजना बनाई और उन्हें सशक्त बनाकर आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाई। उनकी बात का असर हुआ और देशवासियों में हीनता की भावना समाप्त होने लगी और इसके साथ ही अनगिनत स्वतंत्रता सेनानी मिलने लगे जिन्हें पेट भरने की चिंता नहीं थी।
भारत आज़ाद हुआ और पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने। गांधी जी की हत्या हो चुकी थी। पंडित नेहरू जिन पर विदेशी संस्कृति और पश्चिमी देशों की औद्योगिक प्रगति का ज़बरदस्त प्रभाव था, उन्होंने तय किया कि देश में बड़े उद्योग खोले जाएं, इसके लिए देश का अमीर वर्ग बहुत प्रसन्न हुआ, उसकी तो जैसे मन की मुराद पूरी हुई। देश के संसाधनों, प्राकृतिक संपदा मुंह मांगे दामों पर सुलभ करा दी गई। धन्ना सेठों की पीढ़ी तैयार हुई जिनके नाम की चर्चा न कर इस बात को ध्यान में रखते हुए यह विचार करना है कि इस व्यवस्था से गांधी जी द्वारा तैयार की गई लघु उद्योगों की जड़ को ही काट दिया गया। आज जो हम ‘एक ज़िला-एक उत्पाद’ या ऐसी ही योजनाओं के असफल होने और स्टार्ट अप की विफलताओं का रोना रोते हैं, इसका मूल कारण यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों के उद्योग धंधों को बड़े उद्योगपतियों ने सरकार के सहयोग से इस हालत में पहुंचा दिया कि चाहे हम कागज़ों में कितनी ही डींगें हांक लें, यह मानने से कोई भी अर्थशास्त्री इंकार नहीं कर सकता कि यह वर्ग ही अर्थव्यवस्था की रीढ़ है जबकि हमने लघु उद्योगों को मरणासन्न अवस्था में छोड़ दिया है।
इतिहास गवाह है कि सन् 1948 और सन् 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्तावों में, उदाहरण के लिए इस्पात, कोयला, ऊर्जा जैसे क्षेत्र, भारी उद्योगों की स्थापना को प्राथमिकता देते हुए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग स्थापित किए और 60 और 70 के दशक तक पूरे देश में इनका जाल बिछ गया और देश का अधिकांश धन इसमें लग गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि इनसे देश की जीडीपी बढ़ी और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि कुछ संस्थानों को छोड़कर अधिकतर घाटे की भेंट चढ़ गए और देश के सीमित संसाधनों पर बोझ बन गए। इसी के साथ लघु उद्योगों की इस तरह उपेक्षा हुई कि वे या तो बंद हो गए या बड़े उद्योगों के अधीन हो गए। सरकार यह भूल गई कि लघु उद्योगों की बदौलत ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा होते हैं। बड़े उद्योगों में नौकरी मिलना आसान नहीं है, इसलिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में छोटे उद्योगों का विकास थमा नहीं और वे 1973-74 में 4 लाख से बढ़कर सन् 2000 तक 6 करोड़ से अधिक हो गए जिन्हें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम (एसएमएसई) कहा जाने लगा।
इनकी नियति यह है कि ये खुलते हैं, बंद होते हैं, उद्यमी बनने की कोशिश करते लोग गांठ का पैसा लुटाकर और बैंक या वित्तीय संस्थानों के कज़र्दार बनकर अपना घर-द्वार बेच कर जैसे तैसे गुज़र बसर करते हैं। इसका कारण यह है कि सरकार बड़े पूंजीपतियों का संरक्षण करती है, उन्हें सभी तरह की छूट देती है और लघु उद्योगों का गला घोटने के लिए ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने देती हैं जो लघु उद्योगों का सहारा है। ये छोटे उद्यमी उनके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते क्योंकि उनकी लागत ही नहीं पूरी होती। न वे अपना ब्रांड बना पाते हैं और न ही ग्राहक को अपनी गुणवत्ता के बारे में भरोसा दिला पाते हैं क्योंकि प्रचार और विज्ञापनों की दुनिया इतनी महंगी है कि वे कहीं टिक नहीं पाते।
कागज़ी योजनाएं और भ्रम : ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ सोचती या करती नहीं, बहुत सारी योजनाएं बनती है। उदाहरण के लिए सन् 2001 से 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाने की घोषणा। एक पालिसी पैकेज भी बना कर दिया गया जिसमें ढांचागत सुविधाओं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उत्पादन और कोई भुगतान न करे तो कानूनी कार्रवाई जैसी व्यवस्था की। इससे सहूलियत से ज़्यादा उद्यमियों की दु:खभरी दास्तान सुनने को मिली और यह उनके जले पर नमक छिड़कने जैसी बात हुई—जैसे सरकार से कोई भी सुविधा लेने के लिए अफसरों का सुविधा शुल्क (कथित रिश्वत) लिए बिना कोई काम न होने देना, कच्चा माल जुटाने में पसीना निकल जाना, ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम करने और माल ढुलाई में इतनी परेशानी होना कि जल्दी खराब हो जाने वाली वस्तुओं का समय पर न पहुंच पाने के कारण रास्ते में ही किसी खाई खंदक में फेंक देना।
सबसे बड़ी समस्या यह कि लघु उद्योगों पर भी कर्मचारियों के वेतन, हाज़िरी, ई.एस.आईच, प्रोविडेंट फंड और श्रम कानून वैसे ही जो बड़े औद्योगिक संस्थानों पर लगते हैं। अब इससे लघु उद्यमी की कमर तो टूटनी ही है। उद्यमी और उसकी ईकाई दोनों तबाह होने लगते हैं और सरकार इस पर टैक्स लगाने से नहीं चूकती क्योंकि उसकी नज़र में सभी छोटे-बड़े उद्यमी एक समान हैं।
ऐसा नहीं है कि यह अंतर मिट या कम नहीं हो सकता, लेकिन इसके लिए नीयत और नीति तथा उसके लागू करने की भ्रष्टाचारविहीन व्यवस्था की ज़रूरत है। आप आधुनिक संसाधन जैसे डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन के साधन लघु उद्योगों के लिए सुगमता से उपलब्ध करा दीजिए, उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था कर दीजिए, आसानी से बिना गारंटी जितनी ज़रूरत, उतना ऋण और कम से कम तीन साल न ब्याज, न मूल रकम चुकाने की सुविधा और 5 वर्ष तक आयकर देने से मुक्ति दे दीजिए, फिर देखिए हम चीन को भी कैसे उत्पादन और दाम में चुनौती दे सकते हैं।
राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस एक अवसर है जो सरकार को अपनी नीतियों पर फिर से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकता है। लघु व मध्यम उद्योग को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ समझा जाए। उनके लिए सहायता और वित्तीय संरक्षण प्रदान करने की नीति बनाकर उस पर क्रियान्वयन करने की ज़रूरत है।