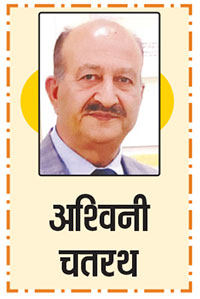मॉनसून का हमारे महाद्वीप के लिए महत्व
विश्व के अलग-अलग हिस्सों में अनेक ऐसी वर्षा प्रणालियां हैं जो विभिन्न देशों की कृषि, वातावरण तथा वहां की अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। ये हैं पूर्वी एशियाई मॉनसून हवाएं जो चीन, वीयतनाम, ताइवान, जापान, कोरिया तथा फिलिपीन्स आदि देशों में बारिश करती हैं। इसी प्रकार उत्तरी अमरीकी मॉनसून हवाएं जो अमरीका तथा मैक्सिको देशों में बारिश के लिए ज़िम्मेदार है। इसी प्रकार विश्व के अन्य हिस्सों में ऐसी अन्य कई मॉनसून प्रणालियां हैं जो संबंधित देशों में बारिश करके उन क्षेत्रों की संस्कृति और अर्थ-व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। दरअसल मॉनसून शब्द अरबी भाषा के शब्द ‘मौसिम’ से लिया गया है जिसका अर्थ है ‘ऋतु’।
यदि भारत सहित समूचे दक्षिण एशिया में चलती मॉनसून हवाओं की बात करें तो यह इस क्षेत्र में लगभग चार महीने चलने वाली ऐसी प्रमुख वातावरणीय प्रणाली है जो भारतीय उप-महाद्वीप के मौमस, कृषि, अर्थ-व्यवस्था तथा दैनिक जीवन को बड़ी गहराई से प्रभावित करती है। इन हवाओं के इस क्षेत्र के बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान तथा श्रीलंका आदि देशों पर पड़ते प्रभावशाली असर के कारण ही इन क्षेत्रों के लोगों द्वारा मॉनसून ऋतु का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है। जून से सितम्बर तक चलने वाला यह सीज़न इस क्षेत्र की कृषि को सहारा देता है और यहां के कम हो रहे जल भंडारों को भरने का काम करता है। इसे दक्षिण-पश्चिम मॉनसून का नाम दिया जाता है। ये हवाएं हिन्द महासागर के अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी से चल कर दक्षिण एशिया के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचती हैं। इन मॉनसून हवाओं के पैदा होने की शुरुआत मई तथा जून के महीने में भारतीय उप-महाद्वीप के केन्द्रीय तथा उत्तरी क्षेत्रों में पड़ती भीषण गर्मी से होती है जिससे क्षेत्र का समूचा वातावरण बहुत अधिक गर्म हो जाता है। इसके साथ इस क्षेत्र की हवा गर्म होकर फैलने लगती है और इसका दबाव काफी सीमा तक कम हो जाता है। कम दबाव के कारण पैदा हुए खाली स्थान को पूरा करने के लिए हिन्द महासागर से चलने वाली नमी वाली हवाएं इस क्षेत्र की ओर चल पड़ती हैं। इन हवाओं की एक विशेषता यह है कि ये समुद्र के पानी से भरपूर होती हैं। जहां-जहां से भी ये हवाएं गुज़रती हैं, वहां-वहां बारिश करती हैं। इन हवाओं से कुछेक क्षेत्रों में अधिक बारिश होती है और कुछ दूसरे क्षेत्रों में कम बारिश होती है। भारत के पश्चिमी तथा केन्द्रीय हिस्सों में होती कुल बारिश की लगभग 90 प्रतिशत बारिश मॉनसून हवाओं के कारण होती है और उत्तर भारत में होती बारिश का 50 से 75 प्रतिशत हिस्सा मॉनसून हवाओं द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है।
कृषि : दक्षिण-पश्चिम मॉनसून हवाओं का भारतीय कृषि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, विशेषकर उन क्षेत्रों में जिनमें कृषि व्यवसाय सिर्फ और सिर्फ बारिश पर ही निर्भर है। उचित तथा समय पर हुई बारिश से भरपूर कृषि उपज पैदा होती है। धान की फसल को बहुत अधिक मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है। इसलिए यह फसल बड़ी सीमा तक मॉनसून की बारिश पर ही निर्भर करती है। कपास तथा गन्ने की फसलें भी अधिकतर बरसाती पानी पर ही निर्भर करती हैं।
पानी की पूर्ति : भारतीय उप-महाद्वीप के अधिकतर हिस्सों के भू-जल की कमी को पूरा करने के लिए मॉनसून की बारिश ही एक सबसे बड़ा स्रोत है। विगत कुछ वर्षों से भू-जल का कम होता पानी वैज्ञानिकों, सरकारों तथा विशेष तौर पर आम लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
बिजली का उत्पादन : भारत में कुल बिजली के उत्पादन का 10 प्रतिशत हिस्सा हाईड्रो पावर यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली ही होती है। इसलिए डैमों में पानी का उचित मात्रा में होना ज़रूरी हो जाता है। इसे पूरा करने में मॉनसून की बारिश की बड़ी भूमिका होती है और यह पन-बिजली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा स्रोत होती है।
बीमारियां लगने की सम्भावना : मॉनसून हवाओं के भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर बहुत-से सकारात्मक प्रभावों के अतिरिक्त कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। उनमें से एक है मौसमी बीमारियों के फैलने का रूझान। इस सीज़न में मौसमी ज़ुकाम, खांसी, हैज़ा, आंखों का खराब होना तथा त्वचा रोग के अतिरिक्त कुछेक और चिन्ताजनक बीमारियां भी लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ये हैं मलेरिया, डेंगू तथा चिकनगुनिया आदि। इन दिनों में अस्पताल डेंगू के मरीज़ों से भर जाते हैं।
-मो. 62842-20595