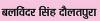‘एक देश, एक चुनाव’ के साथ ज़रूरी हैं चुनाव सुधार
यह विडम्बना है कि हमारे देश में लगभग हर साल चुनाव होते रहते हैं। आचार संहिता लागू हो जाती है। राजनेता व जिम्मेदार लोग अपना काम-ध्ाधा छोड़ कर चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। इससे ना केवल सरकारी व्यय बढ़ता है, बल्कि प्रशासनिक मशीनरी, राजनीतिक तंत्र भी अपने मूल उद्देश्य से लम्बे समय तक विमुख रहता है। लेकिन यदि चुनाव साथ ही करवाने हैं तो अन्य चुनाव सुधार भी साथ ही लागू करना अनिवार्य है। इनमें सबसे प्राथमिक है मतदाता का बेहतर प्रशिक्षण । यह अब आम हो गया है कि चुनावों में जनता के मुद्दे नदारद रहते हैं। सांसद का चुनाव लड़ने वाले नालियां साफ करवाने या बगीचा या सड़क बनवाने के वायदे करते दिखते हैं। असल में ये काम तो स्थानीय निकाय के पार्षद या सरपंच के होते हैं। न तो उम्मीदवार और न ही जनता समझ पा रही है कि उन्हें सरपंच के साथ-साथ सांसद की ज़रूरत क्यों है। सांसद और विधायक के काम क्या हैं? उन्हें हम चुन कर किस काम से भेजते हैं? वे जिस सदन में बैठते हैं, वहां वे क्या काम करते हैं? पंचायत से ले कर संसद तक के चुनाव प्रचार में निजी आरोप-प्रत्यारोप गाली-गलौज की जो भरमार हो चुकी है, उससे साफ हो जाता है कि सियासत का जन सरोकार से कोई वास्ता रह नहीं गया है। यह केवल राजनेताओं का दोष नहीं है। जन प्रतिनिधि कोई दूसरे ग्रह से नही आता, वह भी हमारे समाज का हिस्सा होता है और हम जैसा ही होता है। ‘एक देश एक चुनाव’ के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी यही है। हालांकि हमारे देश में कोई चार बार एक साथ चुनाव भी हैं। लेकिन राज्यों में अलग से चुनाव होने का असल कारण आयाराम-गयाराम की राजनीति रहा। दलबदल विरोधी कानून आज के हालात में अप्रासंगिक है। कोई कभी भी दल बदल कर नए दल से चुनाव लड़ कर तस्वीर बदल देता है। कई जगह तो दल बदल विरोधी नियमों को सदन के अध्यक्ष ही धता बताते रहते हैं। इसका मूल तो दलों के चुनाव के प्रचार अभियान से साबित हो जाता कि लाख पाबंदी के बावजूद चुनाव न केवल महंगे हो रहे हैं, बल्कि सियासी दल जिस तरह एक दूसरे पर शुचिता के उलाहने देते दिखते हैं, खुद को पाक-साफ व दूसरे को चोर साबित करते रहते हैं, असल में समूचे कुएं में ही भांग घुली हुई है। लोकतंत्र के मूल आधार निर्वाचन की समूची प्रणाली ही अर्थ-प्रधान हो गई है और विडम्बना है कि सभी राजनीतिक दल चुनाव सुधार के किसी भी कदम से बचते रहे हैं। वास्तव में यह लोकतंत्र के समक्ष नई चुनौतियों की बानगी मात्र है। यह चरम बिंदू है जब चुनाव सुधार की बात आर्थिक-सुधार के बनिस्पत अधिक प्राथमिकता से करना ज़रूरी है। आधी-अधूरी मतदाता सूची, कम मतदान, पढ़े-लिखे मध्य वर्ग की मतदान में कम रुचि, महंगी निर्वाचन प्रक्रिया, बाहुबलियों और धन्ना सेठों की पैठ, उम्मीदवारों की बढ़ती संख्या, जाति-धर्म की सियासत, चुनाव करवाने के बढ़ते खर्च, आचार संहिता की अवहेलना—ये कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो स्वस्थ्य लोकतंत्र के लिए जानलेवा वायरस हैं और इस बार ये सभी ताकतवर हो कर उभरी हैं। कहीं पर हजारों मतदाताओं के नाम गायब होते हैं तो कहीं एक राजनेता कैमरे के सामने 11 वोट डाल लेता है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त या कर्नाटक निर्वाचन आयोग के ब्रांड एंबेसेडर का नाम ही मतदाता सूची में नहीं होता परन्तु किसी भी जिम्मेदार पर कोई कार्यवाही होती नहीं। कई बार निर्वाचन आयोग असहाय सा दिखा है। फिर आयोग ने ही अपने खर्चे इतने बढ़ा लिए हैं कि वह आम आदमी के विकास के लिए जरूरी बजट पर डाका डालता प्रतीत होता है।यह एक विडम्बना है कि कई राजनीतिक कार्यकर्ता ज़िन्दगी भर मेहनत करते हैं और चुनाव के समय उनके इलाके में कहीं दूर का उम्मीदवार आ कर चुनाव लड़ जाता है और ग्लेमर या पैसे या फिर जातीय समीकरणों के चलते जीत भी जाता है। ऐसे में सियासत को दलाली या धंधा समझने वालों की कतार बढ़ती जा रही है। संसद का चुनाव लड़ने के लिए निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम पांच साल तक सामाजिक काम करने के प्रमाण प्रस्तुत करना, उस इलाके या राज्य में संगठन में निर्वाचित पदाधिकारी की अनिवार्यता ‘जमीन से जुड़े’ कार्यकर्ताओं को संसद तक पहुंचाने में कारगर कदम हो सकता है। एक बात हमें पाकिस्तान से सीख लेनी चाहिए कि चुनाव से पहले सरकार भ्ांग हो और किसी वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक सरकार का जिम्मा दिया जाए। इससे चुनाव में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल की कुरीति से बचा जा सकता है। आज प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सरकारी जहाज़ की सुविधा पर प्रचार करते हैं। कई जगह चुनाव निष्पक्षता से करवाने की ड्यूटी में लगे अफसरों को प्रभावित करने की खबरें भी आती हैं।