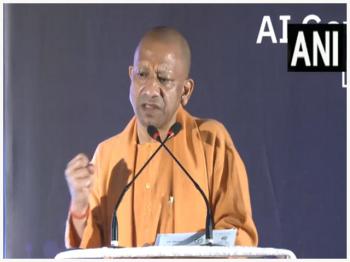टी-20 वर्ल्ड कप - भारत को एक और झटका, अभिषेक कैच आउट
टी-20 वर्ल्ड कप - भारत को एक और झटका, तिलक भी आउट
-
टी-20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका ने भारत को 188 रन का दिया टारगेट
-
 दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लगी आ.ग
दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लगी आ.ग
-
 टी20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका को एक और झटका, स्टब्स कैच आउट, 158/6
टी20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका को एक और झटका, स्टब्स कैच आउट, 158/6
-
 मोदी का मेरठ भाषण विपक्ष पर केंद्रित था, जनता की चिंताओं के बारे में कुछ नहीं : कांग्रेस
मोदी का मेरठ भाषण विपक्ष पर केंद्रित था, जनता की चिंताओं के बारे में कुछ नहीं : कांग्रेस
-
टी20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका को एक और झटका, ब्रेविस कैच आउट
-
 टी20 वर्ल्ड कप - 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 78/3
टी20 वर्ल्ड कप - 10 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 78/3
दिलकश अंदाज़ में नज़र आईं Sonam Bajwa, फैंस के साथ लीं Selfie
टी20 वर्ल्ड कप - 5 ओवर के बाद साउथ अफ्रीका 31/5
-
टी20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका को एक और झटका, रिकलेटन कैच आउट
-
 कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का ब्यान
कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का ब्यान
-
 पंजाब में कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब - सुखबीर सिंह बादल
पंजाब में कानून-व्यवस्था की हालत बहुत खराब - सुखबीर सिंह बादल
-
 T20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का किया फैसला
T20 वर्ल्ड कप - साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का किया फैसला
-
 उत्तराखंड: मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के लिए राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी
उत्तराखंड: मौसम विभाग द्वारा अगले 24 घंटों के लिए राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी
-
 उत्तराखंड: सीएम धामी ने संस्कृत स्टूडेंट टैलेंट सम्मान कार्यक्रम में लिया हिस्सा
उत्तराखंड: सीएम धामी ने संस्कृत स्टूडेंट टैलेंट सम्मान कार्यक्रम में लिया हिस्सा
अटारी, 22 फरवरी (गुरदीप सिंह अटारी/राजिंदर सिंह रूबी) - BSF द्वारा आयोजित मैराथन...
लखनऊ, 22 फरवरी - उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने IBM सेंटर के...
-
 इस बार का चुनाव बंगाल में बदलाव लेकर आएगा - दिल्ली CM रेखा गुप्ता
इस बार का चुनाव बंगाल में बदलाव लेकर आएगा - दिल्ली CM रेखा गुप्ता
-
 उत्तर प्रदेश फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट ने खजूर के गोदाम पर की छापेमारी
उत्तर प्रदेश फ़ूड सेफ़्टी डिपार्टमेंट ने खजूर के गोदाम पर की छापेमारी
-
 AI समिट मुद्दा - कांग्रेस ने हद दर्जे की गंदी राजनीति की: PM मोदी
AI समिट मुद्दा - कांग्रेस ने हद दर्जे की गंदी राजनीति की: PM मोदी
-
 डिजिटल गिरफ्तारी: देहरादून में बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी
डिजिटल गिरफ्तारी: देहरादून में बुजुर्ग महिला से 3 करोड़ से ज्यादा की ठगी
-
 दोनों मृत पुलिसकर्मियों के परिजन आए सामने, एक-दूसरे पर हमले की बात को सिरे से नकारा
दोनों मृत पुलिसकर्मियों के परिजन आए सामने, एक-दूसरे पर हमले की बात को सिरे से नकारा
-
 देश की पहली RRTS का रूट हुआ तय - केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर
देश की पहली RRTS का रूट हुआ तय - केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर
गोवा, 22 फरवरी - केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि गोवा लंबे समय से देश...
मेरठ, उत्तर प्रदेश, 22 फरवरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "कांग्रेस ने नेताओं.....
-
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का किया उद्घाटन
-
 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
-
 CM योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ पहुंचने पर किया स्वागत
CM योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेरठ पहुंचने पर किया स्वागत
-
 AALP के लिए चुने गए IIM लखनऊ के आयुष, 500 से अधिक इंजीनियरों को ऑयल और गैस सिस्टम में दिया प्रशिक्षण
AALP के लिए चुने गए IIM लखनऊ के आयुष, 500 से अधिक इंजीनियरों को ऑयल और गैस सिस्टम में दिया प्रशिक्षण
-
 हिमाचल: CBSE में बदले स्कूलों में जाने के लिए कम रुचि दिखा रहे टीचर
हिमाचल: CBSE में बदले स्कूलों में जाने के लिए कम रुचि दिखा रहे टीचर
-
 किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़
कानपुर, 22 फरवरी - बिल्हौर और चौबेपुर में झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा बुखार के मरीजों....
चेनारी, 22 फरवरी - गुप्ता धाम विश्व के प्राचीनतम पूजा स्थलों में से एक.....
-
 बरेली जोगेंद्र हत्या.कांड: वारदात की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस
बरेली जोगेंद्र हत्या.कांड: वारदात की वजह पता लगाने में जुटी पुलिस
-
 सैन्यकर्मी हत्या/कांड: मुठभेड़ में दबोचा 25 हजार का इनामी हत्या/रोपी, पैर में लगी गो.ली
सैन्यकर्मी हत्या/कांड: मुठभेड़ में दबोचा 25 हजार का इनामी हत्या/रोपी, पैर में लगी गो.ली
-
 इस समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भूत क्षमताएं देखने को मिली है: प्रधानमंत्री मोदी
इस समिट में दुनिया को AI के क्षेत्र में भारत की अद्भूत क्षमताएं देखने को मिली है: प्रधानमंत्री मोदी
-
 प्रधानमंत्री मोदी 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
प्रधानमंत्री मोदी 12,930 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन
-
 अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा-अर्चना
अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में की पूजा-अर्चना
-
 ओडिशा सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में 5 पुलिस कर्मियों की मौत
ओडिशा सड़क हादसा: ट्रक और कार की टक्कर में 5 पुलिस कर्मियों की मौत
नई दिल्ली, 22 फरवरी - दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली.....
नई दिल्ली, 22 फरवरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत....
-
 मेरठ को आज मिलेगी ‘नमो भारत’ और मेट्रो की सौगात, PM मोदी और CM योगी करेंगे उद्घाटन
मेरठ को आज मिलेगी ‘नमो भारत’ और मेट्रो की सौगात, PM मोदी और CM योगी करेंगे उद्घाटन
-
 CM मोहन चरण माझी ने 44वीं हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी बैठक की अध्यक्षता की
CM मोहन चरण माझी ने 44वीं हाई लेवल क्लीयरेंस अथॉरिटी बैठक की अध्यक्षता की
-
 पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किया हवाई हमला
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में किया हवाई हमला
-
 AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा चुनाव 2026 पर दिया बयान
AIUDF अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने असम विधानसभा चुनाव 2026 पर दिया बयान
-
 नितिन नवीन और सीएम भूपेंद्र पटेल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल
नितिन नवीन और सीएम भूपेंद्र पटेल बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हुए शामिल
-
 माणिक मोती
माणिक मोती
चेन्नई, 21 फरवरी - नाम तमिलर काची (NTK) ने त्रिची के आलमपट्टी पुदुर में आयोजित...
देहरादून (उत्तराखंड), 21 फरवरी - देहरादून में, रायपुर थाने की पुलिस ने उत्तराखंड...
-
 लोकप्रिय पहलवान और गायक के.एस. मक्खन की शिरोमणि अकाली दल में घर वापसी
लोकप्रिय पहलवान और गायक के.एस. मक्खन की शिरोमणि अकाली दल में घर वापसी
-
 कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है - सम्राट चौधरी
कांग्रेस पार्टी भारत विरोधी है - सम्राट चौधरी
-
 देश और गुजरात का बजट एक जैसा है - मुख्यमंत्री भगवंत मान
देश और गुजरात का बजट एक जैसा है - मुख्यमंत्री भगवंत मान
-
 T20 वर्ल्ड कप सुपर-8: बारिश की वजह से न्यूज़ीलैंड-पाकिस्तान का मैच रद्द
T20 वर्ल्ड कप सुपर-8: बारिश की वजह से न्यूज़ीलैंड-पाकिस्तान का मैच रद्द
-
 भाजपा के लोग हर जगह अत्या.चार कर रहे हैं - अजय राय
भाजपा के लोग हर जगह अत्या.चार कर रहे हैं - अजय राय
-
दिनदहाड़े नवविवाहिता को मारी गोली, हालत गंभीर
टी20 वर्ल्ड कप सुपर 8: बारिश के कारण न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मैच की शुरुआत में देरी
अहमदाबाद, 21 फरवरी - मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुजरात में घोषणा की कि पंजाब में...
-
 प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के समारोह में हुए शामिल
प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली इंडिया चिप प्राइवेट लिमिटेड के समारोह में हुए शामिल
-
 मध्य प्रदेश: BJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प
मध्य प्रदेश: BJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस और BJP कार्यकर्ताओं के बीच झड़प
-
 नड्डा ने देश में बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (Td) वैक्सीन की लॉन्च
नड्डा ने देश में बनी टेटनस और एडल्ट डिप्थीरिया (Td) वैक्सीन की लॉन्च
-
 कांग्रेस इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को बदनाम कर रही है - अनुराग ठाकुर
कांग्रेस इंटरनेशनल स्टेज पर भारत को बदनाम कर रही है - अनुराग ठाकुर
-
 कांग्रेस पूरी तरह से निराश, हताश हो चुकी है: चिराग पासवान
कांग्रेस पूरी तरह से निराश, हताश हो चुकी है: चिराग पासवान
-
 हमारी सरकार सदन में बहस करने के लिए तैयार है - जवाहर सिंह बेढम
हमारी सरकार सदन में बहस करने के लिए तैयार है - जवाहर सिंह बेढम
अहमदाबाद (गुजरात), 21 फरवरी - इंडियन क्रिकेट टीम के T20 कैप्टन...
नई दिल्ली, 21 फरवरी- भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित 'इंडिया एआई इम्पैक्ट....
-
 जम्मू-कश्मीर: संदिग्ध चीज़ मिलने के बाद बांदीपुरा-श्रीनगर वैकल्पिक किया रास्ता बंद
जम्मू-कश्मीर: संदिग्ध चीज़ मिलने के बाद बांदीपुरा-श्रीनगर वैकल्पिक किया रास्ता बंद
-
प्रेग्नेंसी की खबर फैलाने वालों को सरगुन मेहता ने लगाई फटकार
-
 महाराष्ट्र के मंत्री ने राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया
महाराष्ट्र के मंत्री ने राउत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया
-
 अ'सम को मुक्त कराने का काम भाजपा करने वाली - अमित शाह
अ'सम को मुक्त कराने का काम भाजपा करने वाली - अमित शाह
-
 भारत मंडप में कांग्रेस का हंगामा: कोर्ट ने पांच आरोपियों की दी पुलिस हिरासत
भारत मंडप में कांग्रेस का हंगामा: कोर्ट ने पांच आरोपियों की दी पुलिस हिरासत
-
 सिख गुरुओं के मामले पर टिप्पणियाँ: पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा दिल्ली विधानसभा सचिवालय को लिखा पत्र
सिख गुरुओं के मामले पर टिप्पणियाँ: पंजाब सरकार के गृह विभाग द्वारा दिल्ली विधानसभा सचिवालय को लिखा पत्र
नई दिल्ली, 21 फरवरी - स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री...
वॉशिंगटन, डी.सी, 21 फरवरी - अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप.....
-
 अमृतसर में रईया पुलिस पोस्ट के पास एक IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद
अमृतसर में रईया पुलिस पोस्ट के पास एक IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) बरामद
-
 एआई समिट में बवाल के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा, चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
एआई समिट में बवाल के खिलाफ सड़क पर उतरी भाजपा, चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
-
 कर्नाटक के बागलकोट में ट्रैक्टर खाई में गिरा ,चार लोगों की मौत
कर्नाटक के बागलकोट में ट्रैक्टर खाई में गिरा ,चार लोगों की मौत
-
 मान सरकार ने पंजाब की बेटियों, बहनों और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा- मजीठिया
मान सरकार ने पंजाब की बेटियों, बहनों और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा- मजीठिया
-
 UP: अब अपराधियों की भी होगी यूनिक आई-डी, पुलिस के पास रहेगा फोटो
UP: अब अपराधियों की भी होगी यूनिक आई-डी, पुलिस के पास रहेगा फोटो
-
 शिरोमणि अकाली दल की पंजाब बचाओ रैली गांव भकना से शुरू
शिरोमणि अकाली दल की पंजाब बचाओ रैली गांव भकना से शुरू
दिल्ली, 21 फरवरी - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो.....
अयोध्या, 21 फरवरी - गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉ. भरत जगदेव अयोध्या पहुंचे.....
-
 दिल्ली सरकार की ओर से CM जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप की हुई शुरूआत
दिल्ली सरकार की ओर से CM जनसुनवाई पोर्टल और मोबाइल ऐप की हुई शुरूआत
-
 अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटके बाद बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें, अब 133 अरब डॉलर लौटाने की चुनौती
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटके बाद बढ़ी ट्रंप की मुश्किलें, अब 133 अरब डॉलर लौटाने की चुनौती
-
 पंजाब बचाओ रैली में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल
पंजाब बचाओ रैली में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल
-
 जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण को मिली मजबूती
जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार से जल संरक्षण को मिली मजबूती
-
 जागरूक जनता नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी, जो भारत की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करे: अन्नपूर्णा देवी
जागरूक जनता नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी, जो भारत की प्रगति में बाधा डालने का प्रयास करे: अन्नपूर्णा देवी
-
 रणवीर सिंह को धमकी देने वाले हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
रणवीर सिंह को धमकी देने वाले हैरी बॉक्सर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी
गुवाहाटी (असम), 21 फरवरी - केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 87वें CRPF दिवस परेड....