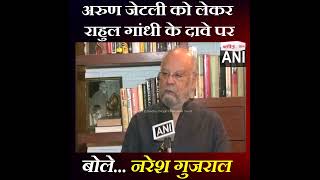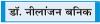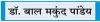परमाणु बम की छाया में कांपती दुनिया
6 अगस्त हिरोशिमा दिवस पर विशेष
हर साल 6 अगस्त को ‘हिरोशिमा दिवस’ मनाया जाता है। यह 6 अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम हमले की वर्षगांठ का प्रतीक है, जोकि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान एक अत्यंत भयावह और विनाशकारी घटना थी। परमाणु बम के पीड़ितों को याद करते हुए यह दिन परमाणु युद्ध के खतरों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाता है। 6 अगस्त 1945 मानव इतिहास का एक ऐसा दिन बन गया, जो विज्ञान की उपलब्धियों की चरम सीमा के साथ-साथ उसके विनाशकारी प्रयोग की भयावहता को भी दर्शाता है। अमरीका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर इसी दिन ‘लिटिल बॉय’ नामक परमाणु बम गिराया था, जिससे हजारों लोगों की तत्काल मृत्यु हुई और अगले कई वर्षों तक लाखों लोग पीड़ा, कैंसर, अपंगता और सामाजिक बहिष्करण का शिकार बने। यह हमला न केवल जापान के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक ऐसा स्थायी घाव बन गया है, जो आज भी न केवल उस देश के जनमानस में बल्कि विश्व राजनीति और शांति विमर्श में जीवित है। हिरोशिमा दिवस केवल एक ऐतिहासिक घटना की स्मृति नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतावनी भी है कि जब विज्ञान की शक्ति नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो वह मानव अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाती है। हिरोशिमा दिवस की प्रासंगिकता आज के समय में बहुत बढ़ गई है। रूस-यूक्रेन तथा इज़रायल-फलस्तीन युद्ध, उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और भारत-पाक जैसे परमाणु संपन्न देशों के बीच तनाव, ये सभी घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि परमाणु हथियार केवल संग्रहालय की वस्तु नहीं बल्कि आज भी राजनीतिक समीकरणों और सैन्य रणनीतियों का हिस्सा बने हुए हैं। ऐसे में हिरोशिमा दिवस वह आईना है, जिसमें हम आने वाले संभावित भविष्य की झलक देख सकते हैं। हिरोशिमा पर गिराए गए बम की शक्ति लगभग 15 किलोटन थी यानी 15000 टन टीएनटी विस्फोटक के बराबर। वह एक अकेला बम था लेकिन उसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्काल करीब 80 हजार लोगों की मृत्यु हो गई थी और वर्ष के अंत तक संख्या बढ़कर 1.4 लाख हो गई थी। एक शांत शहर, जिसकी आबादी करीब 3.5 लाख थी, क्षण भर में ही राख में बदल गया था। वहां की मिट्टी, जल, वायु और मानव शरीर, सबकुछ रेडियोधर्मी विकिरण से प्रभावित हो गए। बमबारी के बाद कई दशकों तक बच्चों में जन्म दोष, कैंसर, मानसिक बीमारियां और सामाजिक कलंक देखने को मिला।
परमाणु हमले के मात्र तीन दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर भी ‘फैट मैन’ नामक बम गिराया गया। वह और भी घातक था, जिसने करीब 70 हजार लोगों की जान ली। दो शहरों पर बम गिराकर अमरीका ने एक तरह से विश्व को संदेश दिया था कि युद्ध के नियम बदल चुके हैं और विनाश का नया युग शुरू हो गया है। हालांकि तर्क दिया गया कि इससे द्वितीय विश्वयुद्ध का अंत हुआ परंतु इस तर्क पर नैतिक बहस आज भी जारी है कि क्या युद्ध समाप्त करने के लिए एक पूरे शहर को नष्ट करना और लाखों निर्दोष नागरिकों को मारना उचित था? क्या कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता था? इन हमलों ने केवल जापान को ही नहीं, समूचे विश्व को झकझोर दिया। उसके बाद एक नई दौड़ शुरू हुई, परमाणु हथियारों की होड़। 1945 के बाद अमरीका, सोवियत संघ (अब रूस), ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इज़राइल जैसे देशों ने परमाणु हथियार बनाए। संयुक्त राष्ट्र के तहत परमाणु अप्रसार संधि (एनपीटी) और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (सीटीबीटी) जैसी पहल की गई पर ये समझौते वैश्विक स्तर पर पर्याप्त प्रभाव नहीं छोड़ पाए। कुछ देश इन संधियों का हिस्सा नहीं बने, कुछ ने नाममात्र का पालन किया और कुछ ने गुपचुप हथियारों का विस्तार जारी रखा। भारत के संदर्भ में देखें तो 1974 में ‘स्माइलिंग बुद्धा’ नामक पहला परमाणु परीक्षण और फिर 1998 में पोखरण-2 के सफल परीक्षणों ने भारत को आधिकारिक तौर पर परमाणु शक्ति सम्पन्न राष्ट्र बना दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि उसकी नीति ‘नो फर्स्ट यूज’ यानी पहले इस्तेमाल नहीं करने की है पर पाकिस्तान, जिसने 1998 में परमाणु परीक्षणों के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन किया, अक्सर इस नीति के विरुद्ध बयान देता रहा है। भारत-पाक के बीच जब-जब सैन्य तनाव बड़ा है, तब-तब परमाणु युद्ध की आशंका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं भी उभरी हैं। कारगिल युद्ध, पठानकोट, बालाकोट स्ट्राइक, पुलवामा और पहलगाम जैसे घटनाक्रमों ने परमाणु हथियारों के खतरनाक उपयोग की संभावना को और अधिक गंभीर बना दिया है। वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध ने भी परमाणु संकट को जगा दिया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा खुले तौर पर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी देना इस बात का संकेत है कि आज भी शक्तिशाली राष्ट्र परमाणु ताकत को केवल सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के हथियार के रूप में देख रहे हैं। उत्तर कोरिया द्वारा बार-बार मिसाइल परीक्षण करना और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अवहेलना करना, चीन द्वारा परमाणु शस्त्रागार बढ़ाने की हो? तथा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जारी तनाव, ये सब आज के ‘हिरोशिमा’ के खतरे की पुनरावृत्ति के स्पष्ट संकेत हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक महामारी, जैविक हथियार और साइबर युद्ध जैसे आधुनिक संकटों के बीच परमाणु हथियारों का अस्तित्व मानवता के लिए एक छुपा हुआ विस्फोटक है, जो कभी भी सक्रिय हो सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अब हम पारंपरिक युद्धों की बजाय ‘साइबर स्पेस’ और ‘परमाणु धमकी’ जैसे असयंमित युद्ध के युग में प्रवेश कर चुके हैं। छोटी सी चूक, गलतफहमी या तकनीकी असफलता भी मानवता को एक बार फिर हिरोशिमा जैसे विनाश की ओर ले जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और शांति कार्यकर्ता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि पृथ्वी पर परमाणु हथियारों का अस्तित्व ही सबसे बड़ा खतरा है।
बहरहाल, हिरोशिमा दिवस का महत्व केवल अतीत की पीड़ा को याद करना नहीं है बल्कि वर्तमान और भविष्य की रक्षा हेतु चेतना विकसित करना है। यह दिवस हमें यह सोचने पर मज़बूर करता है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग किस दिशा में होना चाहिए? क्या विकास का अर्थ विनाश की तैयारी करना है? क्या शक्ति का प्रदर्शन ही राष्ट्रीय सुरक्षा की गारंटी है या शांति का विस्तार? जब तक दुनिया में एक भी परमाणु हथियार अस्तित्व में है, हिरोशिमा दिवस की आवश्यकता बनी रहेगी। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं बल्कि निर्माण में होती है और यही संदेश मानवता के सबसे कठिन समय में सबसे अधिक प्रासंगिक बन जाता है।