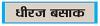हर मौसम का साथी है छाता
आज भी नहीं पता कि छाते का आविष्कार कब हुआ, किन्तु इतना मालूम हुआ है कि छाते का आविष्कार, सूर्य की तेज़ गर्मी से बचाव के लिए हुआ था। बाद में छाते-छतरियां बरसात में भी भीगने से बचने के लिए प्रयोग आने लगीं। पुराणों में कथा आती है कि परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि की कड़ी तपस्या से पसीज कर भगवान सूर्यदेव ने उन्हें जूते (पदत्राण) तथा छाता दिया था, तेज़ किरणों से तथा जूते जलती धरती से महर्षि के पैरों की रक्षा करते थे। कहते हैं छाता, जिसने भी बनाया होगा, उसने वृक्ष को देखकर ही बनाया होगा। आदिवासी लोग आज भी ढाक के पत्तों, केलों के पत्तों को छतरीनुमा बनाकर बांस की एक लकड़ी में टांग लेते हैं और धूप-पानी से बचाव के लिए इसे प्रयोग करते हैं।
यदि इतिहास की मानें तो सबसे पहले छाते का आविष्कार चीन में हुआ। इसके बाद यूनान में छाते बनाए गए। बाद में भारत में भी बनने लगे। आज से चार हजार वर्ष पूर्व चीन, यूनान व भारत में छाते के प्रयोग के बारे में प्रमाण मिलते हैं। 18वीं शताब्दी से छाता स्पेन, ब्रिटेन से होता हुआ सारी दुनिया में छा गया। आज अमरीका में निर्मित छातों की दुनिया भर में मांग है। अमरीकी रेशमी छाते सुगंध छोड़ते हैं तथा एक छाते की कीमत 10 हजार डॉलर तक है। मैक्सिको का छाता टोप के आकार का होने के कारण दूर से पहचान देता है। छाते को अंग्रेजी में ‘अंब्रेला’ कहा जाता है। यह लैटिन भाषा के ‘आम्ब्रा’ शब्द से बना है, जिसका अर्थ ‘छाया देने वाला’ होता है। यूनानी भाषा में छाते को ‘अंबरा’ तथा ‘पेरासोल’ कहा जाता है, जबकि संस्कृत में छाते को ‘आत्रपात्र’ कहते हैं। इन सबका अर्थ छाया देने वाला होता है। भारत में करीब 1000 से अधिक छोटी-बड़ी कंपनियां छाते/छतरियां बनाती हैं। करीब 2 करोड़ छाते भारत में हर साल बिक जाते हैं। आज 300 तरह के छाते दुनिया में प्रचलन में हैं।