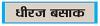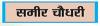क्या रोका जा सकता है बादलों का फटना?
हिमाचल प्रदेश में उत्तरकाशी जैसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला है। भारी बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बीच 13 अगस्त को पांच जगहों पर बादल फटे। बादल फटने से श्रीखंड के भीमडवारी एवं नंती, किन्नौर के पूह, लाहौल के मयाड़ और कुल्लू की तीर्थन घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई। भीमडवारी और नंती में बादल फटने से आई बाढ़ में दो शेड बह गए, छह पानी में डूब गए, एक पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तीर्थन घाटी के बंजार में टिल्ला और दोगड़ा पुल क्षतिग्रस्त हो गए, कुल्लू की तीर्थन घाटी में कई गाड़ियां और कॉटेज बह गए। पूह में बादल फटने से होजो नाले में आई बाढ़ में आईटीबीपी कैंप के लिए ऋषि डोगरी सड़क निर्माण में लगी कंपनी की मशीनरी बह गई और कुछ कर्मचारी फंस गए। इस मानसून सीजन में राज्य में 20 जून से 12 अगस्त तक 241 लोगों की मौत हो चुकी है, 326 लोग घायल हुए हैं, 36 अभी लापता हैं। इस दौरान सड़क हादसों में 115 लोगों की मौत हुई है। बादल फटने, भूस्खलन एवं बाढ़ से अब तक 2507 कच्चे-पक्के घरों, दुकानों को क्षति हुई है, 2043 गोशालाएं भी क्षतिग्रस्त हुई हैं और नुकसान का कुल आंकड़ा 2031 करोड़ रुपये पहुंच गया है।
हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की घटनाएं बार-बार सामने आ रही हैं। उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों में यह स्थिति ज्यादा गंभीर इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां की भौगोलिक बनावट नदियों और घाटियों को सीमित दिशा में प्रवाहित करती है, जिससे अचानक आई बाढ़ का दबाव कई गुना बढञ जाता है। उत्तरकाशी के धराली में हुई घटना भी इसका ज्वलंत उदाहरण है, जहां भारी जलप्रवाह के कारण फ्लैश फ्लड ने घरों, होटलों और बुनियादी ढ़ांचे को नष्ट कर दिया था। उस घटना में कुछ लोगों की जान गई, कई लापता हो गए और बची-खुची संपत्ति भी पानी के साथ बह गई। पहाड़ी इलाकों की संकरी घाटियां, अस्थिर मिट्टी, लगातार हो रहे निर्माण कार्य और वनों की अंधाधुंध कटाई स्थिति को और गंभीर बना देती हैं। जब नदियों का प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है तो पानी का दबाव बढ़ता है और एक बिंदु पर पहुंचकर वह विनाशकारी रूप में टूट पड़ता है। यही कारण है कि यहां छोटी-सी वर्षा भी कभी-कभी भीषण तबाही मचा जाती है।
मनुष्य और प्रतृति के बीच का रिश्ता जितना गहरा और सहजीवी है, उतना ही संवेदनशील भी है। जब प्रकृति अपनी सहज लय में बहती है तो यह संबंध जीवनदायी और संतुलित रहता है लेकिन जैसे ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है या वह अपने अप्रत्याशित और भीषण रूप में सामने आती है, तब यह संबंध भयए विनाश और अस्तित्व के संकट में बदल जाता है। भारत के पर्वतीय इलाकों में मानसून के दौरान घटने वाली बादल फटने’ की घटनाएं इसी असंतुलन और प्राकृतिक तीव्रता की प्रतीक हैं। हाल के वर्षों में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ऐसे कई हादसों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जलवायु और स्थलाकृति के बदलते स्वरूप के साथ-साथ मानवीय हस्तक्षेप इस आपदा की गंभीरता को और बढ़ा रहा है। बादल फटना सुनने में किसी विस्फोट की तरह लगता है लेकिन यह असल में वायुमंडलीय परिस्थितियों का परिणाम है, जिसमें बहुत कम समय में किसी बेहद सीमित क्षेत्र पर अत्यधिक वर्षा होती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार यदि 10 वर्ग किलोमीटर से कम क्षेत्र में एक घंटे से भी कम समय में 100 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश होती है तो इसे बादल फटना माना जाता है। यह घटना तब होती है, जब वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवाष्प वाले बादल किसी कारणवश ठहर जाते हैं और अचानक नीचे गिर पढ़ते हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर मूसलाधार बारिश होती है, जो बाढ़ और भूस्खलन का कारण बनती है।
जलवायु परिवर्तन भी इस आपदा के पीछे एक बड़ा कारक बनकर उभर रहा है। बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ रही है, जिससे बादलों में नमी का स्तर अधिक हो जाता है और भारी वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। साथ ही, तापमान बढ़ने से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे ग्लेशियल झीलों का आकार बढ़ रहा है और उनका टूटना और बहना आसान हो गया है। जब ऐसी झीलें फटती हैं तो नीचे बसे क्षेत्रों में अचानक आई बाढ़ का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है और आने वाले वर्षों में यदि कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसी आपदाएं और अधिक बार और अधिक तीव्रता से घट सकती हैं।
बादल फटने की इतनी तीव्रता से उत्पन्न आपदाओं के कारण ऐसी घटनाओं की पूर्व सूचना देना वैज्ञानिक दृष्टि से अभी भी चुनौतीपूर्ण है। भारतीय मौसम विभाग, इसरो और अन्य वैज्ञानिक संस्थान आधुनिक डॉप्लर रडार और उपग्रह तकनीक का उपयोग करते हुए मौसम के पूर्वानुमान में सुधार कर रहे हैं लेकिन बादल फटने जैसी घटनाएं अतिसूक्ष्म और सीमित क्षेत्र में अचानक होती हैं, जिनका सटीक पूर्वानुमान काफी कठिन होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या बादल फटने की घटनाओं को रोका जा सकता है और किन वैज्ञानिक एवं सामाजिक उपायों से इस संकट को कम किया जा सकता है? सीधे तौर पर बादल फटना रोकना फिलहाल संभव नहीं है क्योंकि यह प्राकृतिक और जलवायु आधारित प्रक्रिया है लेकिन इसके प्रभाव को कम करने के लिए व्यापक कदम उठाए जा सकते हैं।
इसके लिए सबसे पहले, पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी प्रणाली को मज़बूत बनाना होगा। वर्तमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग और इसरो मिलकर रडार, उपग्रह चित्र और अन्य तकनीकों से अल्पकालिक मौसम पूर्वानुमान तैयार करते हैं लेकिन इनकी सटीकता और त्वरित प्रसार में सुधार की आवश्यकता है। स्थानीय प्रशासन और ग्रामीण समुदायों तक सही समय पर चेतावनी पहुंचाना अनिवार्य है, जिससे लोग सुरक्षित स्थानों पर जा सकें और हताहतों की संख्या घट सके। दूसरा, इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य के लिए सख्त भू-वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मानदंड तय करने होंगे। अवैज्ञानिक ढ़ंग से हो रहे सड़क चौड़ीकरण, नदी किनारे होटल निर्माण, खनन और पेड़ों की कटाई को रोकना ज़रूरी है। तीसरा, स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण और संसाधन उपलब्ध कराने होंगे। जब लोग यह जानेंगे कि आपदा के समय कैसे प्रतिक्रिया करनी है तो जान-माल का नुकसान कम होगा। पर्वतीय गांवों में सामुदायिक शेल्टर, आपातकालीन किट, सुरक्षित निकासी मार्ग और नियमित अभ्यास (ड्रिल) से तैयारी के स्तर को बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर बादल फटने की घटनाओं को रोकना तो संभव नहीं लेकिन उनके प्रकोप को कम से कम जनहानि और संपत्ति क्षति तक सीमित करना संभव है। बादल फटना केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि हमारे समय का एक चेतावनी संकेत है, जो हमें याद दिलाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों की नाजुक पारिस्थितिकी और जलवायु संतुलन से छेड़छाड़ के परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं।