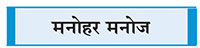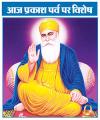बेहतर होने के बावजूद ‘बदनाम’ क्यों है बिहार ?
बिहार विधानसभा चुनाव-2025
इन विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दलों और मीडिया दोनों के द्वारा बिहार की जो आर्थिक तस्वीर पेश की जा रही है, वह वास्तव में विभ्रम पैदा करने वाली है। पेश किये जा रहे आंकड़ों में प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद, प्रतिव्यक्ति आय, शहरी आबादी का प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्र का योगदान और कमोबेश मानव विकास की साधारण हासिल दर— इन सभी के जरिये बिहार को देश का सबसे निचले पायदान का प्रदेश दिखाया जा रहा है। लेकिन यह तस्वीर आकड़ों के लिहाज से एक मिथक ही लगती है। इसलिए नहीं कि ये आंकड़े गलत हैं बल्कि इसलिए कि अगर वास्तविकता में देखें तो बिहार का सामाजिक आर्थिक परिदृश्य कई मामले में काफी आशाजनक भी है। क्योंकि उपरोक्त स्टीरियोटाइप आकड़ों के अलावा बिहार में ऐसे कई और सामाजिक आर्थिक निर्देशांक हैं, जिनके सही आंकड़े सामने लाये जाएं तो बिहार देश के तमाम प्रदेशों के बीच एक सम्मानित स्थान का भी हकदार बनता है।
मिसाल के तौर पर बिहार के करीब 45 हज़ार गांवों में ग्रामीण आधारभूत संरचना की स्थिति काफी अच्छी है, जहां ग्रामीण सड़क निर्माण की एक बड़ी क्रांति हुई है। देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के गांवों में सड़कों का बेहतरीन नेटवर्क दिखाई देता है। ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य था, जहां आधी आबादी अभी कुछ सालों पहले तक बिजली से वंचित थी। वहां अब शत-प्रतिशत घरों में 24 गुणा 7 बिजली का उपलब्ध होना और वह भी बिना किसी अपने बड़े बिजली प्लांट के, अपने आपमें एक बड़ी बात है। दूसरी बात करें तो ग्रामीण पेय जल और प्राथमिक विद्यालयों की आधारभूत संरचना के मामले में भी बिहार देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। तीसरी बात, बिहार में आधी आबादी का सशक्तिकरण भी खूब हुआ है, चाहे इनके शैक्षिक उत्थान की स्थिति हो, पंचायत के जरिये इनकी 50 प्रतिशत राजनीतिक भागीदारी की बात हो और फिर इनकी स्व-सहायता समूहों के जरिये आजीविका मिशन में मिली बड़ी कामयाबी बात हो।
बिहार की तस्वीर देश के कई प्रदेशों से ज्यादा बेहतर है। दरअसल बिहार के आर्थिक विकास के आंकड़ों का मिथक इसीलिए सुनहरी तस्वीर नहीं दिखा पाता; क्योंकि बिहार में देश के अन्य राज्यों की तरह बड़े पूंजीपति और कारपोरेट समूह नहीं हैं। यहां देश के तीन बड़े राष्ट्रस्तर के व्यवसायियों का कोई भी निवेश नहीं है। यही नहीं, बिहार में पटना के अलावा इसके समक्ष समकक्ष का कोई दूसरा शहर नहीं है, क्योंकि झारखंड के अलग होने के बाद दस लाख की आबादी के करीब के तीन बड़े शहर इस प्रदेश से निकल गये हैं। अभी करीब 25 लाख आबादी वाला पटना प्रदेश का एकमात्र बड़ा शहर है, जबकि इसके बाद राज्य के दूसरे बड़े शहर 5-5 लाख की आबादी तक भी नहीं पहुंचे हैं। तीसरी बात यह भी है कि बिहार में देश के अन्य राज्यों की तरह कोई भी विशेष औद्योगिक शहर भी नहीं है। साथ ही बिहार के कृषि प्रधान प्रदेश होने की वजह से औद्योगिक विस्तार के लिए ज्यादा भूमि भी उपलब्ध नहीं है। वास्तव में ये चार ऐसे फैक्टर हैं, जिससे किसी भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर बड़ा प्रभावी असर पड़ता है लेकिन अगर बिहार के समकक्ष देश के अन्य राज्यों मसलन यूपी, एमपी और राजस्थान से इसकी तुलना की जाए तो इन राज्यों की जैसी परिस्थितियां भी बिहार में नहीं हैं। उदाहरण के लिए पड़ोसी राज्य यूपी को ही लें यहां राजधानी लखनऊ के समकक्ष करीब आधे दज़र्न शहर हैं।
उत्तर प्रदेश में राजधानी दिल्ली की सीमा से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के रूप में बड़े औद्योगिक शहर मौजूद हैं। यूपी के सकल घरेलू उत्पाद में इन तीन शहरों का अकेले उत्पादन 15 प्रतिशत के बराबर है। इसी तरह एमपी को खनिज और पर्यटन तथा राजस्थान को खनन और पर्यटन का लाभ है। इस तरह का लाभ बिहार के पास नहीं है। अभी बिहार में मुश्किल से 12 प्रतिशत आबादी ही शहर निवासी है, जबकि यूपी की करीब 28 प्रतिशत और करीब-करीब इतनी ही मध्य प्रदेश व राजस्थान की आबादी शहरवासी है। बिहार के विकास के पैरोकार शुरू से ही इस बात की बड़ी दुहाई देते रहे हैं कि आज़ादी के बाद भाड़ा समानीकरण की नीति की वजह से अविभाजित बिहार को अपने स्थानीय खनिज सम्पदा का कोई विशेष फायदा नहीं मिला।
वर्ष 2005 के बाद बिहार में चौतरफा टर्नअराउंड हुआ। इस बात की स्वीकारोक्ति नितीश कुमार के विरोधी भी करते हैं, मगर सवाल यही है कि बिजली, सड़क, पानी, कानून व्यवस्था और आपदा राहत के कार्यों के इतर बिहार में औद्योगिक प्लांट, शहरी विस्तार और शिक्षा व रोज़गार के व्यापक नेटवर्क क्यों नहीं विकसित नहीं हो पाए? कुछ पुरानी चीनी मिलें, सीमेंट और उर्वरक के कारखाने पुन: शुरू होने के अलावा यहां बड़े उद्योग बड़े पैमाने पर नहीं आये। शायद इसका कारण यह भी है कि राज्य सरकार का सदैव मानना रहा है कि कृषि प्रधान राज्य में भूमि अधिग्रहण के जरिये सामाजिक अशांति लाना उचित नहीं है। ये बात सही है कि इस वजह से बिहार में किसानों की आत्महत्या, जमीनों का ऊसर बंजर होना तथा औद्योगिक अशांति जैसी स्थिति कभी उत्पन्न नहीं होती।
बिहार की अर्थव्यवस्था में श्रमिकों द्वारा बाहर से भेजी गई आय की एक बड़ी भूमिका रहती है। साथ ही वहां के ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को बढ़ाने में इसका योगदान उल्लेखनीय है। यह ठीक वैसे ही है जैसे केरल की अर्थव्यवस्था में पेट्रो डॉलर का योगदान है। इसके अलावा पेशेवर शिक्षा का व्यापक नेटवर्क, शहरीकरण और औद्योगिकीकरण बिहार के विकास के भावी एजेंडे हैं। इससे कोई भी सत्तारूढ़ दल अपने को विलग नहीं रख पायेगा।
-इमेज रिफ्लेक्शन सेंटर