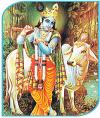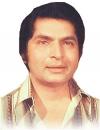मंदिरों में बजने वाले वाद्य यंत्रों का महत्त्व
मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाएं होती हैं। उनकी आरती और अर्चनाएं होती हैं। इन्हीं प्रतिमाओं के समक्ष नाद ब्रह्मा की उपासना की जाती है जिसके लिए मंदिरों में विविध प्रकार के वाद्य बजाए जाते हैं। वादन की यह सनातन परंपरा रही है।
वाद्य तीन प्रकार के होते है - (1) आनद्ध (मृदंग, प्रणव, दुंदुभि) (2) सुषिर (बंशी, शंख, सूर्य, श्रृंगी) और (3) तंतु (वीणा, सारंगी, बेला)। कांस्य वाद्य भी हैं - झांझ, मंजीरा, चिमटा आदि। सभी वाद्यों की अपनी-अपनी विशेषताएं हैं। कांस्यनाद गति को स्तंभित करता है। श्रृंगी नाद आसुरी शक्तियों के मन में भय उत्पन्न करता है। घंटानाद सत्यम्, शिवम्, सुंदरम् का घोष करते हैं। इस नाद को सुनने के लिए देव, यक्ष किन्नर, विद्याधर आदि परोक्ष रूप से मंदिरों में चले आते हैं।
वीणा नाद से योगियों का ब्रह्मा से साक्षात्कार होने लगता है। बंशी वादन से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। शंखनाद युद्ध का उद्धोष करते हैं। महाभारत काल में कुरूक्षेत्र में योगीराज कृष्ण ने ‘पांचजन्य’, युधिष्ठिर ने ‘अनंत विजय’, भीमसेन ने ‘पौण्डू’, नकुल ने ‘सुघोष’, सहदेव ने ‘मणिपुष्प’ और अर्जुन ने ‘देवदत्त’ नामक शंख से युद्ध के लिए नाद किया था। शंखनाद से विजय की संभावना की जाती है। सूर्यनाद सैनिकों में उत्साह पैदा करता है। नारद और सरस्वती की वीणा, नाथ संप्रदायों की सारंगी, कृष्ण की मुरली, शंकर का डमरू, उर्वशी के नूपुर आदि अपने नादों के लिए जाने जाते हैं। यूनानी देवता भी बंशी वादन करते थे जिससे ब्रह्मांड हिल जाता था। प्राचीन रोम के चर्च में घंटानाद होते थे। ’ताण्डव’ नृत्य के समय शिव के पद घुंघरू बोल उठे थे और ’लास्य’ नृत्य के समय पार्वती के नूपपुर रासलीला के समय कृष्ण की पैंजनी नाद ब्रह्मा की उपासना करती थी। शिव बारात में गणों ने तुरही बजा-बजा कर नाद पर नृत्य किया था। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों के नूपुर बजते ही पूजा की घंटियां बजने लगती थी।
भरत नाटयम, कत्थक नृत्य आदि के माध्यम से घंटिका नाद होता रहा है। कीर्तन में सभी राग और नाद मुखरित होने लगते है। संगीत की उपासना नाद ब्रह्मा की उपासना रही है। यूनान की संगीत और नाद शास्त्र की अधिष्ठात्री म्यूज को सारा यूरोप जानता है। सामवेद की संस्कृति नाद उपासना रही है। वीणा वादिनी भारती, स्वयं नाद ब्रह्मा की देवी हैं। वाद्य से मंदिर के देवता प्रसन्न रहते हैं।
भगवान शिव द्वारा मन को लय करने के सवा लाख साधनों में नादश्रवण को वरीयता देते हुए कहा गया है कि इंद्रियाें का स्वामी मन है। मन का स्वामी वायु है, वायु का स्वामी लय है और लय नाद के आश्रित है। शिवसंहिता के अनुसार नाद के समान दूसरा लय कारक नहीं है, अत:योग साम्राज्य की इच्छा रखने वाले को चिंता छोड़कर सावधान हो एकाग्र मन से नाद को सुनना चाहिए। नाद अर्थात् ध्वनि लय अर्थात् एक का दूसरे में मिल जाना।
नाद और लय के अनेक प्रकार हैं। नाद के प्रमुख दो प्रकारों में प्रथम अनाहत और दूसरा आहत नाद है। अनाहत नाद बिना टकराहट के उत्पन्न होता है। आहत नाद उसे कहा गया है जो वायु अथवा दो वस्तुओं के टकराने या घिसने आदि से उत्पन्न होता है। आहत नाद के भी दो वर्ग हैं प्रिय और अप्रिय। संगीत मनीषियों ने केवल सुनने में सुख देने वाली ध्वनि को ही नाद संज्ञा से विभूषित किया है। कारण स्पष्ट है। कर्णकटु ध्वनि मन को तत्काल उद्विग्न करती है। सुनने में अप्रिय लगने वाली ध्वनियों द्वारा शांति प्रापति का हमारा लक्ष्य कभी नहीं प्राप्त होगा। संगीत में उपयोगी नाद की स्थिति इस प्रकार हैं बाइस ‘रुतियां, पांच विकृत और सात शुद्ध स्वर। स्वरों की गरिमा के बोध हेतु विद्वान साधकों ने इनके कुरू, जाति वर्ण का निर्णय किया है। इसके अनुसार षड्ज, गांधार एवं मध्यम देवकुल, पंचम पितर कुल, श्रषभ और धैवत मुकुल तथा निषाद स्वर दैत्यकुल में उत्पन्न हुआ है।
वैदिक पद्धति के अनुसार सात स्वरों के ऋषि देवता तथा छंद संगीत पारिजात नामक गं्रथ में कहे गए हैं। इसके अनुसार षड्ज से निषाद तक सात स्वरों के द्रष्टा ऋषि क्रमश: अग्नि, ब्रह्मा, चंद्रमा, भगवना विष्णु, नारद, तुम्बुरू और कुबेर हैं। सात स्वरों के देवता क्र मश: अग्नि, ब्रह्मा, सरस्वती, भगवान शिव, विष्णु, गणेश और सूर्य हैं। अनुष्टप, गायत्री, त्रिषटिप, बृहती, पंक्ति, उष्णिक तथा जगती, ये सात स्वरों के छंद कहे गए हैं।
समाधि अथवा ध्यान की अवस्था में सुनी गई ध्वनियों के आधार पर वैसी ध्वनि उत्पन्न करने के प्रयत्न ने घंटा, शंख, बंशी, वीणा और मृदंग जैसे वाद्यों को जन्म दिया। समाधि के सहायक होने के कारण इन वाद्यों का देव मंदिरों में पूजन के समय प्रयोग आरंभ हुआ। महर्षि पाणिनि को ध्यान की अवस्था में डमरू ध्वनि द्वारा व्याकरण-सूत्रों की उपलब्धि होने की कथा प्रसिद्ध है। (उर्वशी)